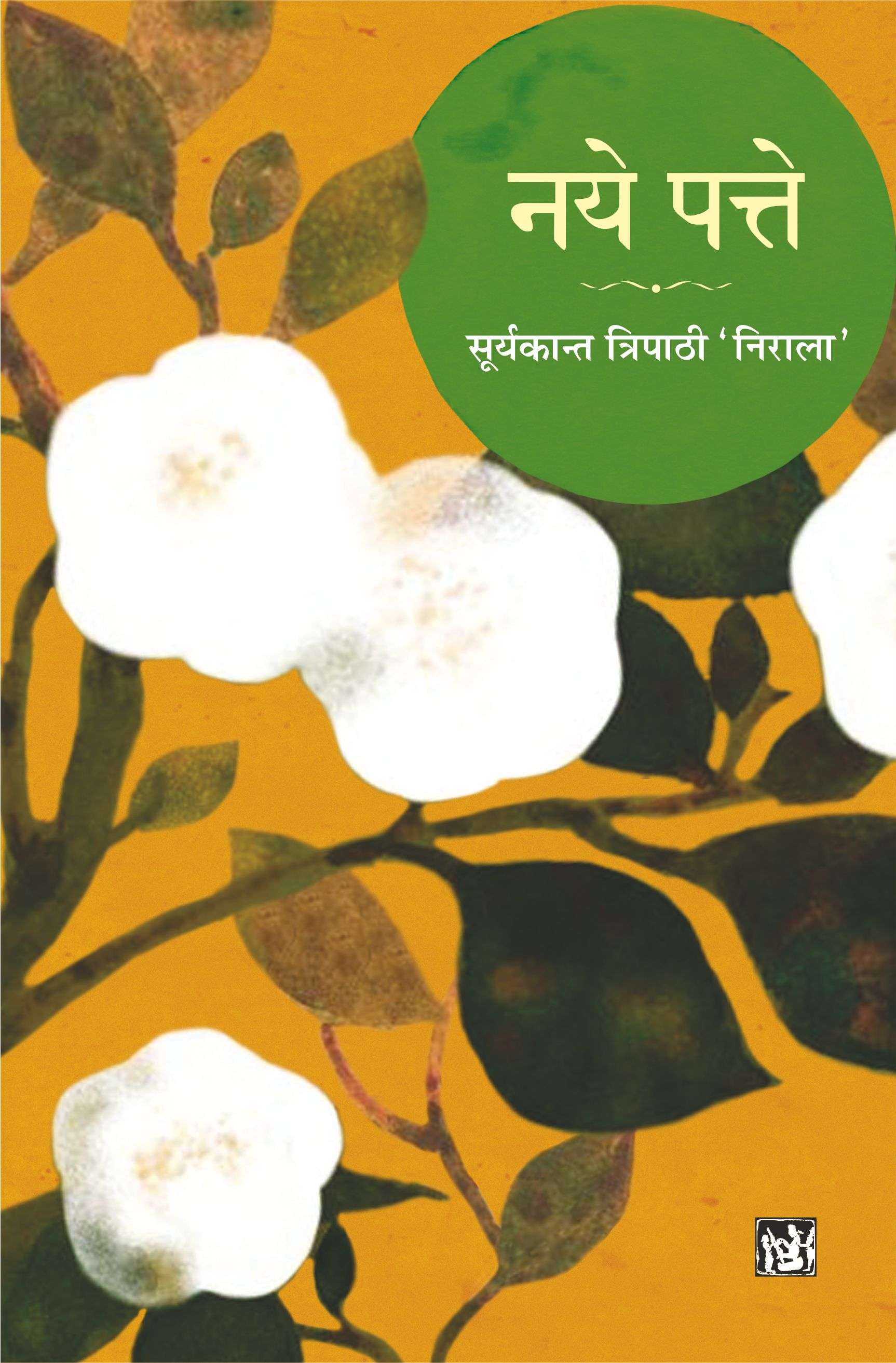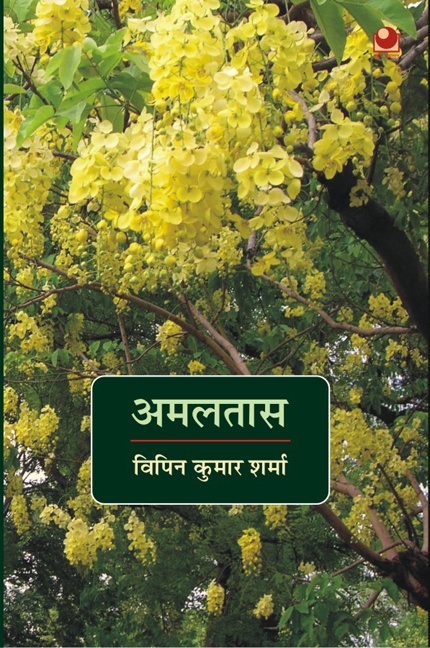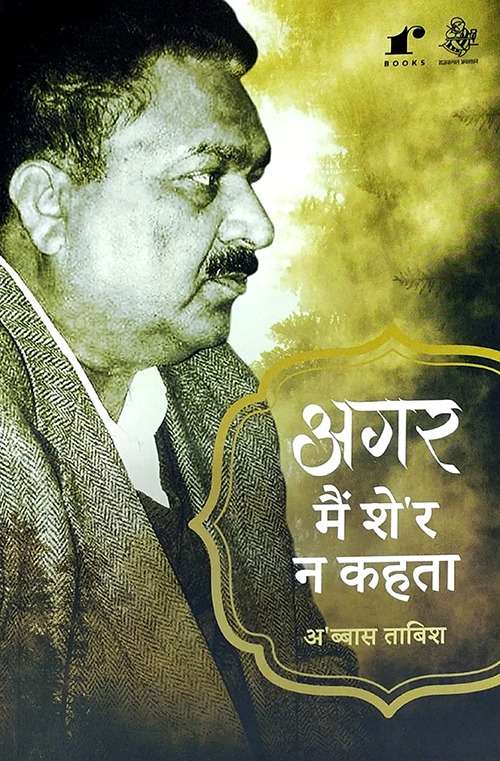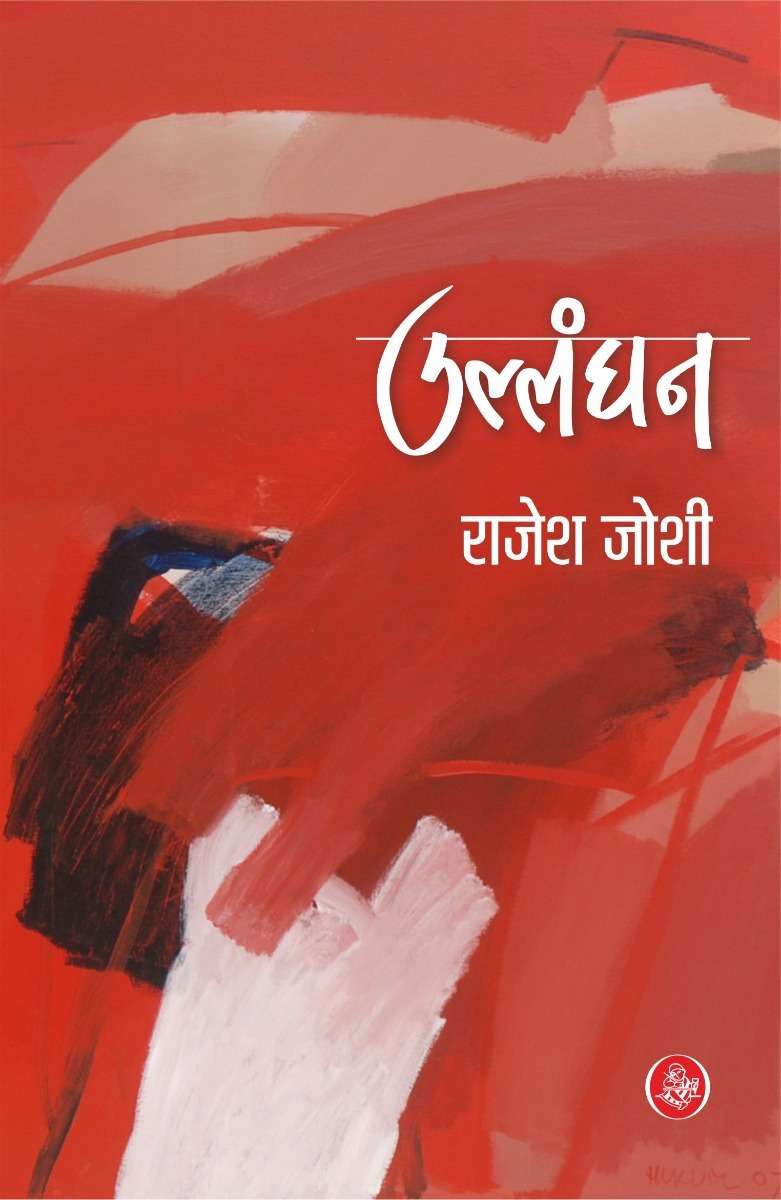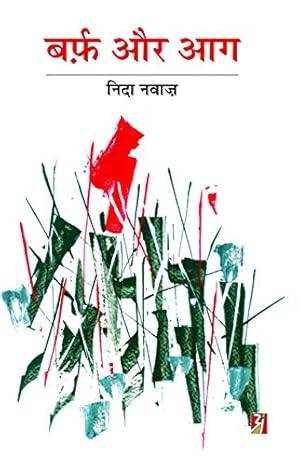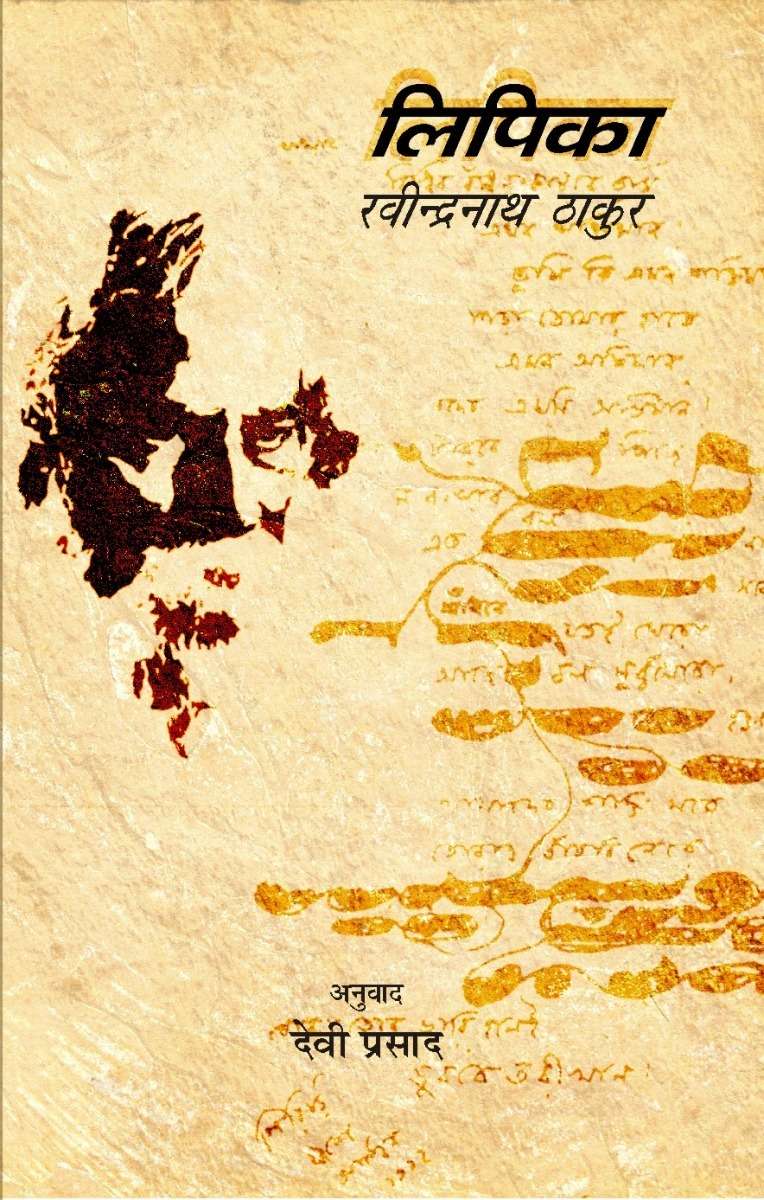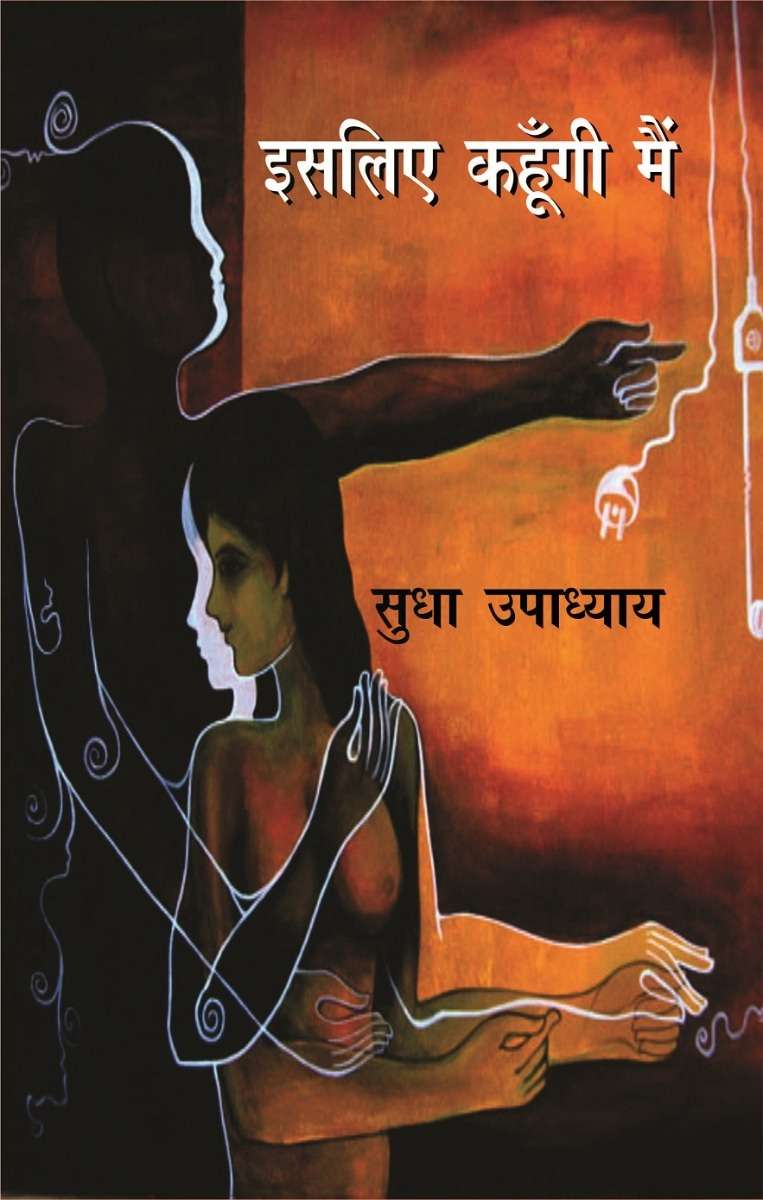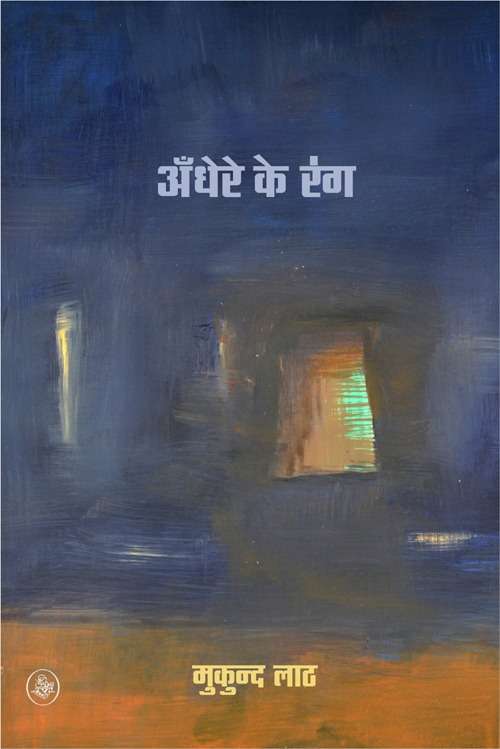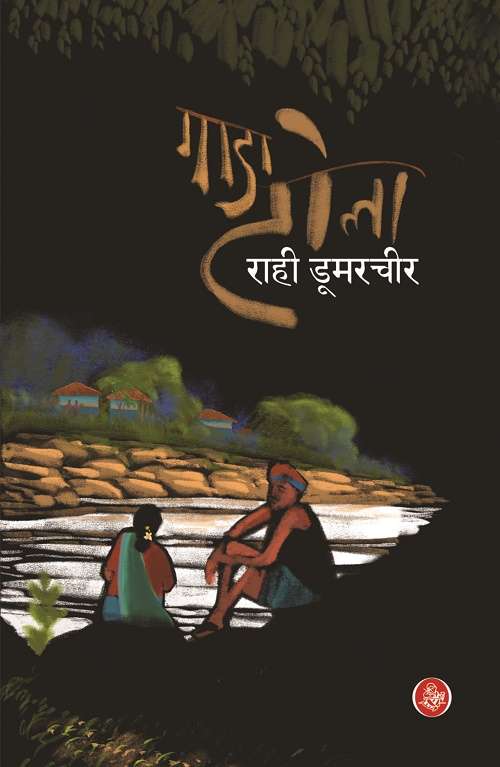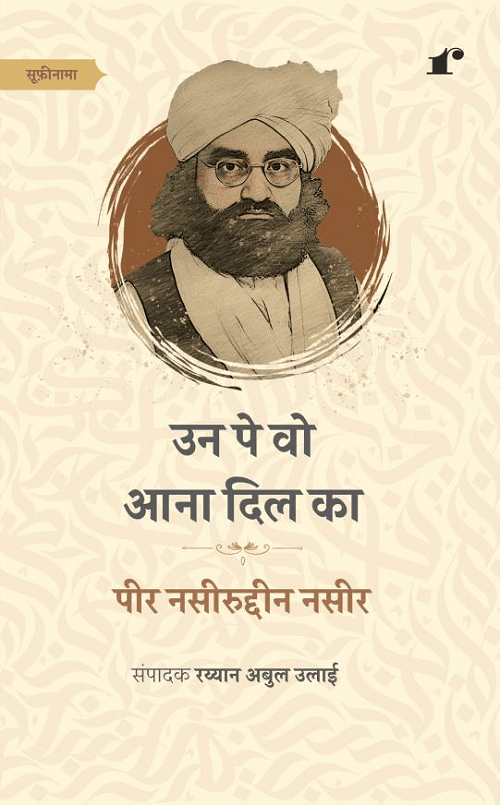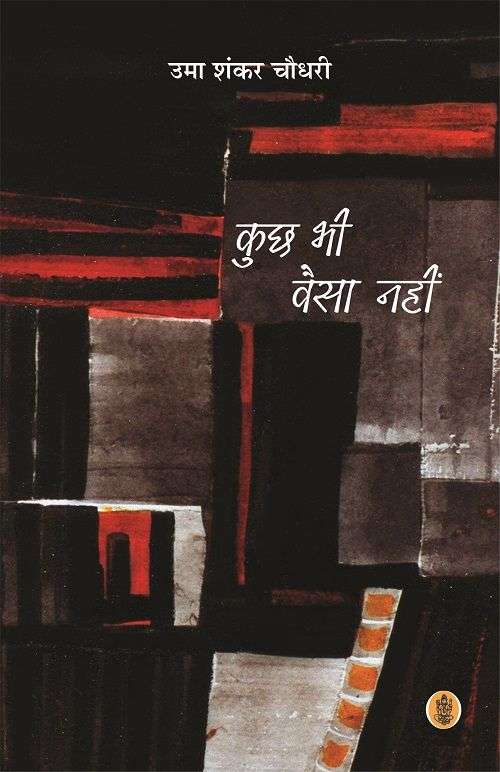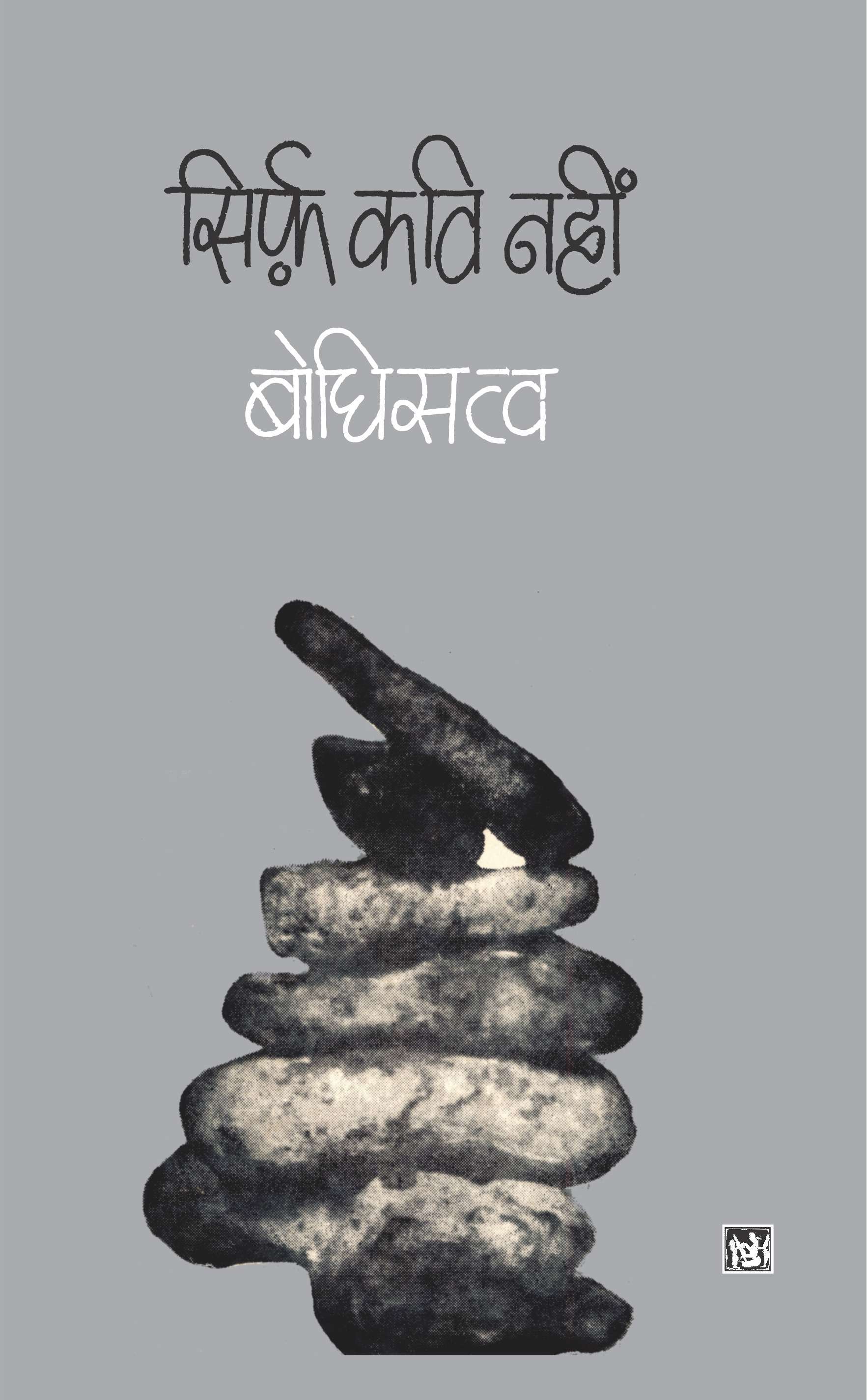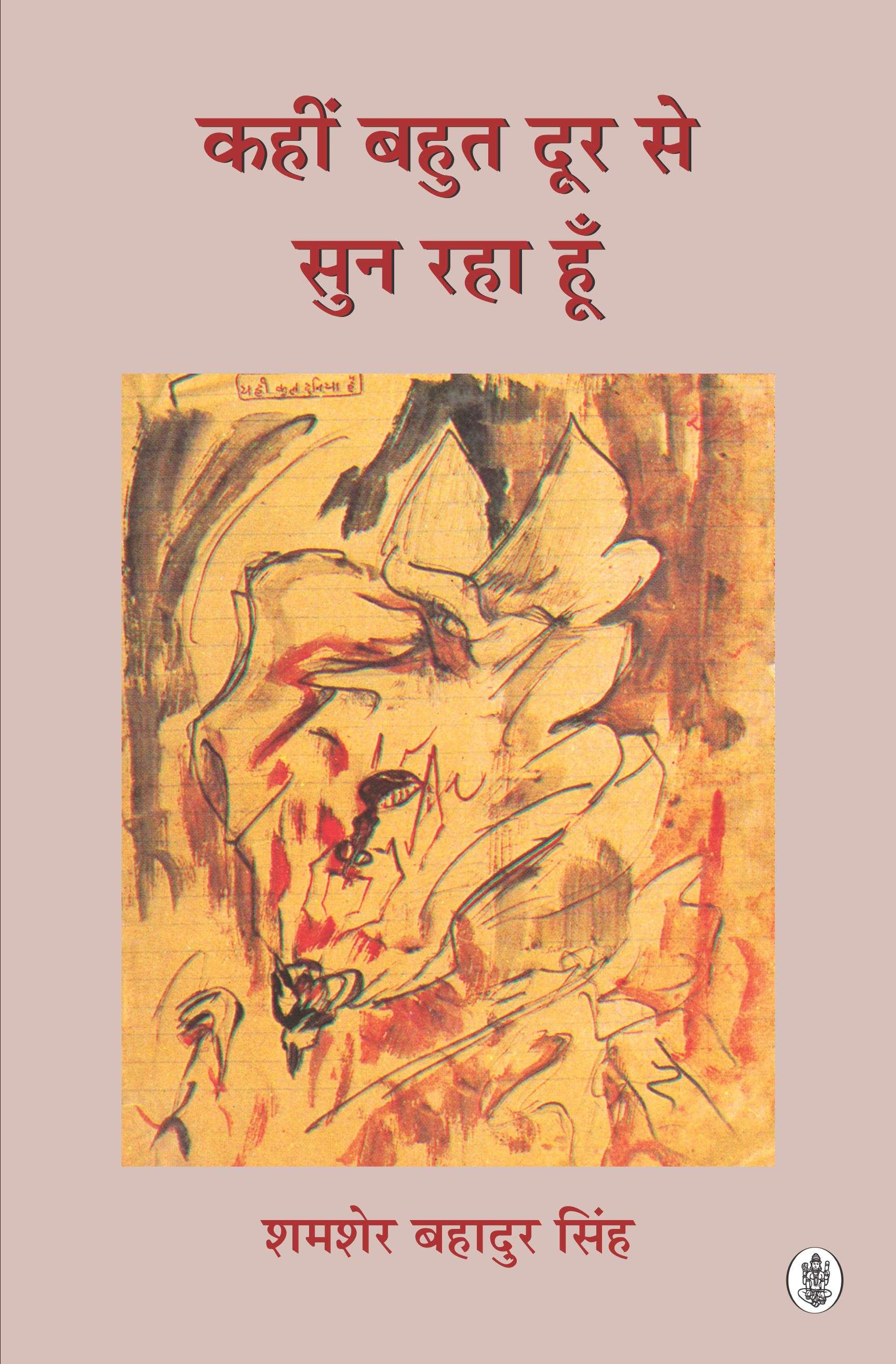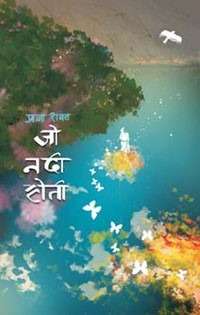
Jo Nadi Hoti
Author:
Pragya RawatPublisher:
Rajkamal Prakashan SamuhLanguage:
HindiCategory:
Poetry0 Ratings
Price: ₹ 120
₹
150
Unavailable
प्रज्ञा रावत का हिन्दी कविता-संसार में प्रवेश एक विरल घटना है। घर-परिवार के तमाम कार्यभार के बीच अपने निजी एकान्त में निरन्तर सृजनशील प्रज्ञा ने कभी अपने को प्रक्षेपित नहीं किया, बल्कि श्लाघनीय निस्पृहता के साथ अपना रचना-कर्म जारी रखा। निजी अनुभवों के ताप से सिद्ध ऐसी प्रखर कविताएँ पहले कभी लिखी नहीं गईं। इनके सर्वथा नए एवं विलक्षण जीवन-प्रसंग भाषा को नई गृहस्थी प्रदान करते हैं, जहाँ कविता नया कलेवर, नया परिपाक एवं आभरण ग्रहण करती है।</p>
<p>प्रज्ञा रावत की कविताएँ अपने अनूठे सम्भार एवं रूप-विधान के लिए अलग से सराही जाएँगी। दुर्लभ बिम्बों एवं अनगिनत लयों का सम्पुंजन इन्हें एक पृथक् व्यक्तित्व प्रदान करता है। प्रज्ञा की कविताएँ अपने सौष्ठव एवं संरचनागत दृढ़ता के लिए सहृदय समालोचकों द्वारा पहले भी समादृत हो चुकी हैं। यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि प्रज्ञा रावत सभी स्त्री रचनाकारों से भिन्न नितान्त नवीन एवं स्वतंत्र स्वत्व से समृद्ध कवयित्री हैं। यहाँ न तो स्त्री-विमर्श का कोई अतिरंजित स्वर है, न ही कोई अन्य ग्रन्थि। जो है, जीवन का सहज स्वीकार और अभिव्यक्ति है, बहुत कुछ सुभद्राकुमारी चौहान की तरह। इसलिए प्रज्ञा रावत का यह संग्रह एक नए रचना उन्मेष के तौर पर स्वीकार किया जाएगा।</p>
<p>—अरुण कमल
ISBN: 9788183615259
Pages: 84
Avg Reading Time: 3 hrs
Age: 18+
Country of Origin: India
Recommended For You
Naye Patte
- Author Name:
Suryakant Tripathi 'Nirala'
- Book Type:

-
Description:
निराला का दूसरे चरण का काव्य भी दो दौरों से गुज़रा है। उसके पहले दौर में ‘कुकुरमुत्ता’ (प्रथम संस्करण) और ‘अणिमा’ की कविताएँ रची गई हैं और उसके दूसरे दौर में ‘बेला’ और ‘नये पत्ते’ की कविताएँ। निराला के पहले चरण के तीसरे दौर की कविताओं में ही उनका यथार्थवादी रुझान प्रबलतर होता हुआ दिखलाई पड़ता है। उसी का विकास दूसरे चरण के पहले दौर की कविताओं में देखने को मिलता है। निराला बहुत ही संश्लिष्ट भाव-बोध के कवि थे, इसलिए वे इस दौर में भी गीत-रचना करते रहते हैं।
‘अणिमा’ की अनेक रचनाएँ इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं कि निराला का सामाजिक यथार्थ का ज्ञान प्रौढ़तर हुआ है। इससे उनका यथार्थवाद नये उत्कर्ष को प्राप्त करता है, जिसे हम ‘नये पत्ते’ की नई कविताओं में, जिनका सम्बन्ध किसानों से है, स्पष्टता से देखते हैं। यह निराला-काव्य की नई मंजिल है। इसी कारण हमने ‘बेला’, ‘नये पत्ते’ की कविताओं को उनके दूसरे चरण के काव्य के दूसरे दौर की कविताएँ माना है।
निराला का यथार्थवाद ‘नये पत्ते’ की ‘कुत्ता भौंकने लगा’, ‘झींगुर डटकर बोला’, ‘छलाँग मारता चला गया’, ‘डिप्टी साहब आए’ और ‘महगू महगा रहा’ जैसी कविताओं में बुलन्दी पर पहुँचता है।
—नन्दकिशोर नवल (निराला रचनावली की भूमिका से)।
Amaltas
- Author Name:
Bipin Kumar Sharma
- Book Type:

- Description: Hindi poems by Bipin Kumar Sharma
Agar Main Sher Na Kahta
- Author Name:
Abbas Tabish
- Book Type:

- Description: Awating description for this book
Ullanghan
- Author Name:
Rajesh Joshi
- Book Type:

-
Description:
उल्लंघन संग्रह में कवि हुक्म-उदूली की अपनी प्राकृतिक इच्छा से आरम्भ करते हुए मौजूदा दौर की उन विवशताओं से अपनी असहमति और विरोध जताता है, जिन्हें सत्ता हमारी दिनचर्या का स्वाभाविक हिस्सा बनाने पर आमादा है।
एक ऐसे समय में ‘जिसमें न स्मृतियाँ बची हैं/न स्वप्न और जहाँ लोकतंत्र एक प्रहसन में बदल रहा है/एक विदूषक किसी तानाशाह की मिमिक्री कर रहा है’—ये कविताएँ हमें निर्प्रश्न अनुकरणीयता के मायाजाल से निकलने का रास्ता भी देती हैं, और तर्क भी।
कवि देख पा रहा है कि ‘सिकुड़ते हुए इस जनतंत्र में सिर्फ़ सन्देह बचा है’, ताक़त के शिखरों पर बैठे लोग नागरिकों को शक की निगाह से देखते हैं, तरह-तरह के हुक्मों से अपने को मापते हैं; कहते हैं कि साबित करो, तुम जहाँ हो वहाँ होने के लिए कितने वैध हो, और तब कविता जवाब देती है–‘ओ हुक्मरानो/मैं स्वर्ग को भूलकर ही आया हूँ इस धरती पर/तुम अगर मुझे नागरिक मानने से इनकार करते हो/तो मैं भी इनकार करता हूँ /इनकार करता हूँ तुम्हें सरकार मानने से!’
लगातार गहरे होते राजनीतिक-सामाजिक घटाटोप के विरुद्ध पिछले चार-पाँच सालों में जो स्वर मुखर रहते आए हैं, राजेश जोशी उनमें सबसे आगे की पाँत में रहे हैं। इस संग्रह की ज़्यादातर कविताएँ इसी दौर में लिखी गई हैं। कुछ कविताएँ महामारी के जारी दौर को भी सम्बोधित हैं जिसने सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने के सरकारी उद्यम पर जैसे एक औपचारिक मुहर ही लगा दी–‘सारी सड़कों पर पसरा है सन्नाटा/बन्द हैं सारे घरों के दरवाज़े/एक भयानक पागलपन पल रहा है दरवाज़ों के पीछे/दीवार फोड़कर निकल आएगा जो/किसी भी समय बाहर/और फैल जाएगा सारी सड़कों पर!’
Barf Aur Aag
- Author Name:
Nida Nawaz
- Book Type:

- Description: Poems
Main Ek Samundar Hoon
- Author Name:
Ram Kumar 'Awara'
- Book Type:

- Description: Hindi Poetry Book is written By Ram Kumar Sinha "Awara". This book consists of poetry related to love and life.
Lipika
- Author Name:
Rabindranath Thakur
- Book Type:

- Description: ‘लिपिका’ रवीन्द्रनाथ ठाकुर का सबसे पहला गद्य-काव्य संग्रह है। किन्तु इसकी केवल एक को छोड़कर और कोई रचना कविता के तौर पर, यानी कविता आवृत्ति के छन्द के हिसाब से कभी प्रस्तुत नहीं की गई। ‘प्रश्न’ नाम की रचना को सन् 1911 में, पुस्तक प्रकाशित होने के तीन साल पहले, ‘भारती’ पत्रिका में कविता के छन्द के अनुसार छापा गया था। तो भी अगस्त, 1922 में पुस्तक प्रकाशित करने के समय कविगुरु ‘लिपिका’ को कविता-संग्रह के तौर पर छापने का साहस नहीं कर पाए। उन्होंने स्वयं ही लिखा है : ‘छापने के समय वाक्यों को पद्य की तरह तोड़ना नहीं हुआ—मैं तो मानता हूँ कि इसका कारण मेरी कायरता ही था।’ जो भी हो, ‘लिपिका’ वह कृति है जो मनुष्य के हृदय और बुद्धि की गहरी परतों को सर्वश्रेष्ठ कला के माध्यम से ऊपर उभारकर पाठक के सामने रख देती है। हर रूपक को पढ़कर एक दर्शन होता है और साथ-साथ अपने-आपको टटोलने की तरफ़ एक इशारा भी मिलता है। इस कृति की तरफ़ हिन्दी साहित्य जगत का ध्यान उतना नहीं गया है, जितना, मैं मानता हूँ, जाना चाहिए। मेरे लिए तो इसका अनुवाद करना आनन्द का एक बड़ा स्रोत रहा है। इसके कारण गुरुदेव का जो सामीप्य मिला, वह अपूर्व और बड़ा महत्त्वपूर्ण है। पाठकों के साथ इसमें भागीदारी करने का मौक़ा मिला है, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। —भूमिका से
Isliye Kahungi Main
- Author Name:
Sudha Upadhyaya
- Book Type:

-
Description:
यह दर्ज करना उचित होगा कि इधर की हिन्दी कविता में अभिधा के प्रति बढ़ती उदासीनता के बावजूद सुधा उपध्याय उसकी शक्ति और सम्भावनाओं का अन्वेषण करने से नहीं हिचकतीं और सीधी बात को सीधे तरीक़े से कहने में संकोच नहीं करतीं...
‘उन सबका आभार/जिनके नागपाश में बँधते ही/यातना ने मुझे रचनात्मक बनाया उनका भी हृदय से आभार/जिनके घात-प्रतिघात/छल-छद्म के संसार में/मैं घंटे की तरह बजती रही।/मेरे आत्मीय शत्रु/तुमने तो वह सब कुछ दिया/जो मेरे अपने भी न दे सके।’
यहाँ कटुता या प्रतिहिंसा नहीं, जीवन की शर्तों का सामना उद्वेगरहित भाव से करनेवाला साहस है। वह इस कवयित्री को ‘अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी—आँचल में है दूध और आँखों में पानी’ वाली पारम्परिकता से तो भिन्न बनाता ही है; बल्कि सुधा उपाध्याय की इन कविताओं में जो नारी-चेतना आदि से अन्त तक फैली हुई है, वह न अबला की ‘हाय’ से शुरू होती है, न जगत के दु:ख-संकटमय जंत्र को ‘चकनाचूर’ करने की दुराशा में ख़त्म दिखती है। उलटे, वह हालात को बदलने में यक़ीन करती है जिसके तमाम पड़ावों में से कुछ ये हैं—‘सुना है वह स्त्री/हो गई है अब ख़ुद के भी ख़िलाफ़/चीख़-चीख़कर दर्ज करा रही है सारे प्रतिरोध/कहती है, सहना और चुपचाप रहना/कल की बात थी।’
यदि कोई पूछे कि अँधेरों से लड़ने की क़ूवत/औरत, तूने कहाँ से जुटाई/ये आईना जो दरक गया था कभी का/इसे फिर कहाँ से उठा लाई?’ तो सुधा के पास उत्तर मौजूद है—‘अब पेंसिलों की धार बनाने से पहले/हँसिए की धार बनानी होगी/दिमाग़ चलाने के साथ, चलाने होंगे हाथ/दूसरों को कहने से पहले/अब दिखाना होगा ख़ुद करके।’
लेकिन यह समझने के लिए दूर जाना ज़रूरी नहीं कि सुधा को हँसिए की धार बनानी है—ख़ुद करके दिखाने के लिए, न कि प्रतिपक्ष की गरदन रेतने के लिए : ‘जब पक कर खड़ी हो जाए फ़सल/बाँट दो बूरा-बूरा/चूरा-चूरा/यही है सृजन।’
सन्तोष का विषय यह है कि सुधा उपाध्याय की दृष्टि निकट और तत्काल तक सीमित नहीं; वह इतिहास और अतीत को भी अपने फलक का हिस्सा बनाती हैं। वहाँ सम्भावनाओं के अनेक द्वार खुलने की प्रतीक्षा में होंगे।
Andhere Ke Rang
- Author Name:
Mukund Laath
- Book Type:

-
Description:
मुकुन्द लाठ हमारे मूर्धन्य विचारकों और संगीतवेत्ताओं में से एक हैं। सुखद संयोग यह है कि उन्होंने कविताएँ भी लिखी हैं और वे अपने ढंग के अकेले कवि हैं। विस्मय की बात यह है कि उनकी कविता में संसार की पदार्थमयता और उनकी सहज वैचारिकता में न तो कोई अलगाव है और न ही एक का दूसरे पर कोई बोझ। वे अपने आसपास को जिस सजग संवेदनशीलता और नन्हीं सचाइयों में देख पाते हैं, वह अनोखा गुण है। उनके अवलोकन में सूक्ष्मता है, उनकी अभिव्यक्ति में सफ़ाई है। वे मर्म के कवि हैं, किसी विचार के प्रवक्ता नहीं। उनकी कविता का वितान बड़ा है पर उनमें सहज विनय है, कोई महत्त्वाकांक्षा नहीं। वे सहज भाव से कह पाते हैं : ‘उडऩा तो/चिडिय़ा से सीख लिया/अब तो आकाश कहाँ पूछता हूँ।’ उनके अलावा हिन्दी में और कवि हैं जो कह सके ‘है इन्हीं पत्तों में कहीं/ढूँढ़ना मत/पंख हूँ, आकाश है।’ रज़ा पुस्तक माला में अपनी आयु के आठवें दशक में लिखी गईं एक कवि की इन कविताओं को हम सादर-सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।
—अशोक वाजपेयी
Gada Tola
- Author Name:
Rahi Dumarchir
- Book Type:

- Description: पहले अन्दर मारी जाती है नदी/तब मिटता है नक़्शे से गाडा टोला। गाडा टोला यानी नदी टोला। राही डूमरचीर की ये कविताएँ नदी, पहाड़, जंगल और उनके साथ बसे मनुष्यों के विस्थापन, विलोप और निर्वासन से उपजे अफ़सोस और पीड़ा की कविताएँ हैं। कुछ ‘बनने’ के लिए या सिर्फ़ ‘जी सकने’ के लिए लोग अपनी ज़मीनों से उठकर शहरों की ओर निकल जाते हैं, पहाड़ उन्हें रास्ता देते हुए पीछे रह जाते हैं, नदियाँ भी, सखुआ के जंगल भी। राही अकसर इस विवशता की सबसे भीतरी कोर से अपनी कविता उठाते हैं। इसके लिए उन्होंने अपना एक खुला मुहावरा गढ़ा है, जो ख़बरों से भी कोई मार्मिक कविता निकाल लेता है, चिट्ठियों और संवादों से भी। इस तरह वह जीवन जस-का-तस सम्प्रेषित हो पाता है, जिसकी पीड़ा को कवि हम तक पहुँचाना चाहता है। ‘ऐदेल किस्कू’ और ‘हिम्बो कुजूर’ जैसी कई कविताएँ हैं, जो इसी प्रविधि से पंक्ति-दर-पंक्ति और सघन होती जाती हैं। ‘गीतों के आयोजन को तुम लोग सुरों का महासंग्राम कहते हो’—कहा रिमिल टुडू ने। राही जीवन के इस पहलू को भी देखते हैं जो जंगल से दूर सभ्यता के बीच गढ़ा जा रहा है, जहाँ ज्ञान किताबों में बन्द है, और किताबें अलमारियों में। सभ्यता की विडम्बनाओं को आईना दिखाते हुए, एक कवि के रूप में राही समय के, प्राकृतिक अवयवों के, पेड़ों, पत्तों, दूब, पानी, बच्चों और नदियों के मन से बतियाते हैं और हर हाल में उनके पक्ष में खड़े रहते हैं— अच्छा आप उसी गाँव के हैं न/जहाँ मन्दिर के किनारे नदी है देवघर के उस भले मानुष से कहा मैंने—जी नहीं/उस गाँव का हूँ/जहाँ नदी के किनारे मन्दिर है।
Un Pe Wo Aana Dil Ka
- Author Name:
Peer Naseeruddin Naseer
- Book Type:

- Description: शाह नसीर के प्रसिद्ध सूफ़ी कलाम से हिंदी पाठक पहली बार रु-ब-रू हो रहे हैं. शाह नसीर के उर्दू, फ़ारसी और हिन्दवी कलाम के साथ यह किताब संग्रहणीय है. इसका संपादन रय्यान अबुल उलाई ने किया है.
Antas
- Author Name:
Dr. Yashika
- Book Type:

- Description: ‘अंतस’ डॉ. यशिका के अंतकरण की अनुभूतियों का सीधा-सरल काव्यानुवाद है। किसी काव्य-कौशल की स्पर्धा में प्रस्तुत संग्रह की कविताएँ खुद को शामिल नहीं करतीं, ये केवल मन की निष्पाप, पवित्र और प्रांजल अनुभूतियों की छलकन हैं और फिर भी पूर्ण हैं। भारतीय स्त्री के संस्कार, उसका सहज समर्पण और नेह जैसे इन कविताओं में साकार देह पाकर इठला रहा है। मन्नत पूरी हो जाने जैसी उपलब्धि और जिस्मोजान निछावर कर डालने के समर्पित अहसास, सामीप्य की सिहरन और दूरी होते ही हृदय का अरमान बना लेने की सोच...एक स्त्री के समर्पण और प्रेम का इससे आगे क्या उदाहरण हो सकता है?
Tulsi Rachnawali Vol-2
- Author Name:
Dr. Ramji Tiwari
- Book Type:

- Description: गोस्वामी तुलसीदास की विलक्षण प्रतिभा से प्रसूत अनंत काव्य-कीर्ति-कौमुदी में स्नात होकर समस्त विश्व के काव्य-रसिक धन्य, रससिक्त और श्रद्धानवत होते रहे हैं, किंतु सभी के दृष्टि-पथ में 'रामचरितमानस' ही आकाशदीप की भाँति विराजमान है। अन्य ग्रंथरत्न छायावेष्टित ही रह जाते हैं। जबकि लोक-परलोक चिंतन, व्यावहारिक चेतन जीवन और अध्यात्मबोध, संस्कृति और संस्कार, संघर्ष और आस्था तथा जय और पराजय से युक्त विलक्षण व्यक्तित्व उनके सभी ग्रंथ-रत्नों को देखने के बाद ही सगुण साकार हो पाता है। संस्कारशील और सुरुचि-संपन्न पाठक भी इस विश्वकवि के संपूर्ण वाड्मय का रसास्वादन कर लेने के बाद ही पूर्ण परितोष का लाभ ले पाता है। गोस्वामीजी के सभी ग्रंथरत्नों को एकत्र उपलब्ध कराने के पुनीत उद्देश्य से ही इस 'रचनावली' की योजना बनाई गई है। ग्रंथावली का प्रथम खंड सुविज्ञ पाठकों को समर्पित है। इसमें गोस्वामीजी की 'रामलला नहछू', 'वैराग्य संदीपनी', 'बरवै रामायण', 'जानकी मंगल', 'पार्वती मंगल', 'रामाज्ञा-प्रश्न', 'दोहावली', 'श्रीकृष्ण गीतावली' कृतियों का समावेश है। आशा है, सुधी पाठकों को अभीप्सित परितोष मिल सकेगा।
Kuchh Bhi Vaisa Nahin
- Author Name:
Uma Shankar Choudhary
- Book Type:

-
Description:
हिन्दी कविता में अपनी अलग पहचान बना चुके उमा शंकर चौधरी का यह कविता-संग्रह हाल के वर्षों में सामाजिक-राजनीतिक स्तर पर हुए उन तमाम बदलावों का साक्ष्य है जिन्होंने आम आदमी की मुश्किल जिन्दगी को और मुश्किल बना दिया है। संग्रह की कविताएँ समाज की गति और दिशा का बेबाक आकलन ही नहीं करती हैं, उनके निहितार्थों को भी उद्घाटित करती हैं।
कम ही कवि ऐसे हैं जिनके यहाँ राजनीतिक कविताएँ इतनी शिद्दत से अनवरत आती रही हैं जितनी उमा शंकर के यहाँ। उनका राजनीतिक पक्ष स्पष्ट है, इसलिए उनकी कविताएँ भी अपना पक्ष तय करती हुई आम आदमी के हक में जाकर खड़ी हो जाती हैं। समसामयिक राजनीति जिस नए सत्य को गढ़ने और समाज को उसे अपनाने के लिए बाध्य करने को प्रयासरत है, उसकी वास्तविकता को ये कविताएँ सूक्ष्मता से रेखांकित करती हैं। कविता को अपने समय से किस तरह सम्पृक्त होना चाहिए और किस तरह उसे अपने समय का एक अन्तर्पाठ तैयार करना चाहिए ये कविताएँ इसका उदाहरण हैं।
इन कविताओं में अपने समय के प्रति कवि का क्षोभ और क्रोध तो है लेकिन उनसे कहीं ज्यादा दुख है। यहाँ स्त्री का दुख है तो घरों में बन्द होने को मजबूर बच्चों का दुख भी। यहाँ हमारे भीतर की मरती जा रही संवेदनशीलता का दुख है तो सड़कों पर उतर चुकी भीड़ के उन्मादी हो जाने का दुख भी। यहाँ सत्ता की बढ़ती निरंकुशता के कारण दुख है तो उसके खिलाफ उठ रहे प्रतिरोध की आवाज को दबाए जाने का दुख भी। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने समय की भयावहता को दर्ज करते कवि में दुख एक स्थायीभाव की तरह स्थापित हो गया है। कहना न होगा कि इस दुखबोध में ही मनुष्यता का भविष्य निहित है।
दरअसल ये कविताएँ अपने समय-समाज का एक ऐसा दस्तावेज हैं जो मनुष्यता की पक्षधरता में हमेशा प्रासंगिक बनी रहेंगी।
Fati Hatheliyan
- Author Name:
Neha Naruka
- Book Type:

-
Description:
नेहा नरूका की कविताओं में भारतीय राजनीति के नवीन संस्करणजन्य भय और आशंकाएँ विन्यस्त हैं। वे रेखांकित करती हैं कि इस सदी में, ख़ासतौर पर पिछले दशक में राजनीति ने किस-किस तरह समाज को, जनचेतना को संक्रमित और प्रदूषित करने के उपक्रम किए हैं। उसके अक्स आम जीवन की दिनचर्या, विचार-प्रक्रिया, प्रेमिलता और सहजीविता पर नाख़ूनों की गहरी खरोंचों की तरह आए हैं। इनकी त्रासदियाँ सहज मानवीय जीवन की आकांक्षा को नाना प्रकार चोटिल कर सकती हैं, उसके विचलित करनेवाले, मार्मिक ब्योरे यहाँ दर्ज हैं। वे इन कविताओं में संचित आवेग, प्रतिवाद और पीड़ाजन्य क्रोध में समेकित हैं। हम देख सकते हैं कि काली राजनीति से गाढ़े होते इस सामाजिक अन्धकार में नेहा संवेदित स्पर्श और दृष्टि-सम्पन्नता से अपनी कविता अग्रसर करती हैं।
तमाम तरह के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दुराचारों से लथपथ इस समय में घर के बाहर और भीतर जितने अत्याचार और ख़तरे हैं, वे नेहा की कविताओं के प्रस्थान-बिन्दु हैं। ये कविताएँ एक रचनाकार की तकलीफ़ और तलछट के साक्षात जीवनानुभवों से निसृत हैं। इनसे गुज़रते हुए निम्न-मध्यवर्गीय, निम्नवर्गीय और वंचित जीवन के बारीक फ़र्क़ को बेहतर समझा जा सकता है, हिन्दी कविता में इधर जिसका संज्ञान दुर्लभ हो गया है। स्त्रियों पर आरोपित अन्धविश्वासों, धार्मिक पाखंड से सनी कुरीतियों पर सीधे प्रश्नों की तीक्ष्णता इन्हें अधिक प्रभावी बनाती है। प्रेम पर लिखते हुए वे समाज में व्याप्त विषमताओं और अन्तर्विरोधों पर लगातार निगाह रखती हैं।
यहाँ स्त्रीवाद की जिरहें, पितृसत्तात्मकता, स्त्री-निर्मिति आदि के पहलू रोज़मर्रा की मुश्किलों और समझ से प्रेरित हैं। जहाँ वे इंगित कर सकती हैं कि व्यापक सुख व्यापक संवेदनहीनता में बदल रहे हैं। स्त्री की व्यथा स्त्री-कथा में बदल गई है। प्रकारान्तर से स्त्री-दशा की बृहत् तस्वीर बनती चली जाती है। इस हेतु वे तथाकथित वांछित काव्यात्मकता या लयकारी के बरअक्स उस ज्ञानात्मक संवेदित गद्य में कविता मुमकिन करती हैं जो समकालीन कविता का हासिल है। ये कविताएँ आँसुओं की नहीं सवालों की झड़ी लगाती हैं, एक सजग स्त्री, नागरिक की तरफ़ से आरोप-पत्र दाख़िल करती हैं। बाध्यकारी नैतिकताओं और पवित्रताओं को प्रश्नांकन के दायरे में लेती हैं। पहले ही कविता-संग्रह में यह सब देखना सुखद है, स्वागतेय है।
—कुमार अम्बुज
Sirf Kavi Nahi
- Author Name:
Bodhisatwa
- Book Type:

- Description: समकालीन हिन्दी कविता के उपादान आज कुछ इतने सरल हो गये हैं कि ‘कोई कवि बन जाय, सहज सम्भाव्य है।’ कविता के इस संकट में ऊपरी तौर पर अच्छी कविताएँ लिख लेना कठिन नहीं है। लेकिन ऐसी कविता जो एक ‘नयी शुरुआत’ करे, जो अचानक ‘ताज़गी के एक अनहोनेपन’ से पाठक को अपने अनुरूप ढाल ले, ऐसी कविता कहीं नहीं दिखती। ‘ताज़गी (वस्तु और शिल्प) के इसी अनहोनेपन’ के अनुभव को व्यक्त करती हैं बोधिसत्व की कविताएँ। बोधिसत्व की कविताएँ कविता की एक नयी भाषा की खोज में पैदा हुई हैं। गढ़ी हुई, उपलब्ध काव्य-भाषा के नकार और गैरपहचान से बोधिसत्व की काव्य-भाषा का निर्माण हुआ है। नये ढंग की अछूती बिम्ब-मालाओं के माध्यम से यह कवि अपनी बात कहता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कवि करता है जो हमारी संस्कृति के अछूते कोनों से आकर सहसा कविता में एक बिल्कुल नये सांस्कृतिक व्यक्तित्व की रचना करते हैं। इस तरह बोधिसत्व की कविताएँ ‘कविता के एक नये संसार को जन्म देती हैं। निपट भोलेपन के बीच एक तार्किक और जनोन्मुखी अन्तर्दृष्टि सम्पन्न ये कविताएँ अपनी विविधता में एक अद्भुत ‘कोलाज़’ की रचना करती हैं।
Kahin Bahut Door Se Sun Raha Hoon
- Author Name:
Shamsher Bahadur Singh
- Book Type:

-
Description:
शमशेर की कविता का स्थायी मूल्य है, स्वच्छ और निर्मल कविता की परख। इसी नाते शमशेर रूपवादी आलोचकों की तरह, परम्परावादी या यथास्थितिशील नहीं हैं। आधुनिक कविता की स्थायी मूल्यदृष्टि की खोज वह कवि के अनुभव और काव्य के उपकरणों की ज़रूरत के अनुसार करते हैं। इस कसौटी पर वे बड़े कड़े हैं। वे परम्परा की श्रेष्ठतम कविता, कला और सौन्दर्य की ‘प्राचीन या आधुनिक’ हार्दिकताओं को विकसित करते हैं। विकास की उनकी ज़मीन व्यापक है। शमशेर हिन्दी-उर्दू के दोआब के कवि हैं।
ग़ालिब और निराला की मार्मिक भाषाओं के स्वरूप और नाद को शमशेर ने अपनी कविता में आत्मसात् कर लिया है। शमशेर का कलाकार कवि अपनी कला-प्रयोगशाला में तल्लीन रहनेवाला एक वैज्ञानिक कवि है। वह प्रयोगशाला में ‘अत्याधुनिक मर्म की सूचनाएँ’ खोजता रहता है। पतनशील आधुनिक सभ्यता के बाज़ार की चीख़-पुकार से असन्तुष्ट...शमशेर आत्मज्ञान से विकसित होती कविता या कला के विज्ञान को टटोलते चलते हैं।
शमशेर का खोजी सौन्दर्य संगीत की स्वच्छ और निर्मल ऊँचाइयों से कभी निराश नहीं होता। शमशेर के लिए नया रूप लेती मानवीय कला, ऊँची कला का आईना है। वे जानते हैं कि कब पूँजीपति या सत्ता उनकी कविता या कला को संरक्षण देते हैं। शमशेर की ख़ामोशी में एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनती है, जहाँ कलानुभव का इतिहास, भूले-बिसरे मित्रों की यादें, और अपनी मौत का विडम्बना-भरा प्रसंग घुल-मिल जाता है—कोलाज जैसा। घुल-मिल जाने के अनेक कलानुभवों को वे व्यंग्य की शैली में चित्रित करते हैं और कभी रंगमंच पर ‘जात्रा’ या ‘बाउल’ से लीला करते नज़र आते हैं।
‘काल से होड़ लेता शमशेर’ में
—विष्णुचन्द्र शर्मा
Mere Rashk-E-Qamar
- Author Name:
Fanah Buland Shehri Shoaib Shahid
- Book Type:

- Description: फ़ना बुलन्दशहरी का मूल नाम हनीफ़ मोहम्मद था। आपका बुनियादी ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश सूबे के बुलन्दशहर से था। आपकी पैदाइश का वक़्त मुस्तनद तौर बता पाना मुमकिन है, न ही बुलन्दशहर में आपकी पैदाइश की जगह और शिजरा। इसकी वाहिद वजह यही है कि फ़ना साहब एक सूफ़ी शायर थे। और सूफ़ी शायर अपना कलाम सिर्फ़ अपने महबूब के लिए लिखते हैं और ख़ुद को दुनिया से छुपा कर गुमनाम कर लेना उनका तरीक़ा रहा है। आपकी पैदाइश के कुछ बरस बाद ही आप हिजरत करके पाकिस्तान चले गए। शायरी का शौक़ बचपन से था। उस दौर के मशहूर शायर क़मर जलालवी के शागिर्द हो गए। आपका सूफ़ियाना ताल्लुक़ मोहम्मद शरीफ़ मियाँ क़ादरी नक़्शबंदी पीलीभीत से था और आपका आख़िरी वक़्त गुजराँवाला और लाहौर की ख़ानक़ाहों में गुज़रा। यहीं 1 नवम्बर 1986 को आपका इन्तिक़ाल हो गया।
Aashna
- Author Name:
Yogita bajpaye Kanchan
- Book Type:

- Description: Yogita bajpaye Kanchan Potry Book
Aashad Ki Duphari
- Author Name:
Harsh Ranjan
- Book Type:

- Description: मेरे छठे काव्य संग्रह को मैं आपके हाथों में दे रहा हूँ। ये पुस्तक काफी इंतज़ार के बाद निकली है पर जब निकली है तो क्या निकली है। ये संग्रह एक प्रयोग के लिए जाना जाएगा जो इसमें शामिल वक्तव्य के रूप में हैं। ये वक्तव्य एक कौंध जैसे हैं और आपको इसमें मेरे विचार एक क्षण के लिए पर बिल्कुल स्पष्ट दिखेंगे। सूई से लेकर रॉकेट तक पर कविता लिखने की शिक्षा हमें मिली है और हर बार की तरह संसद से सड़क तक को मैंने लपेटने का प्रयास किया है। आप कविताओं का आनंद लें और मैं अगली पुस्तक की तैयारी में लगता हूँ।.
Customer Reviews
Be the first to write a review...
0 out of 5
Book