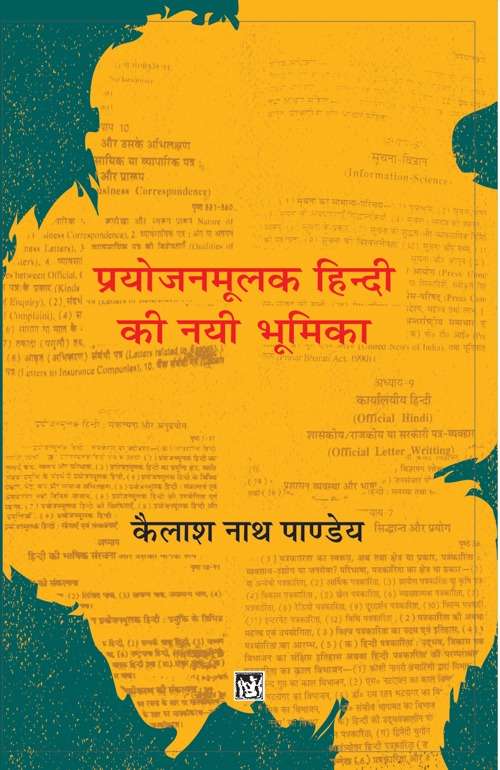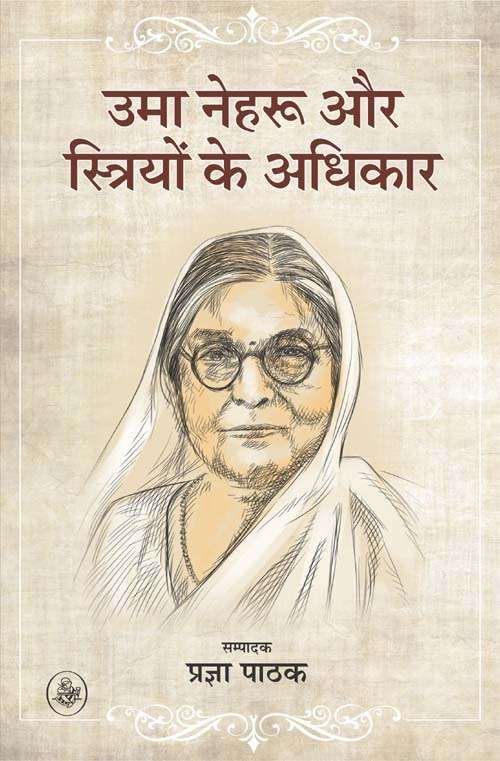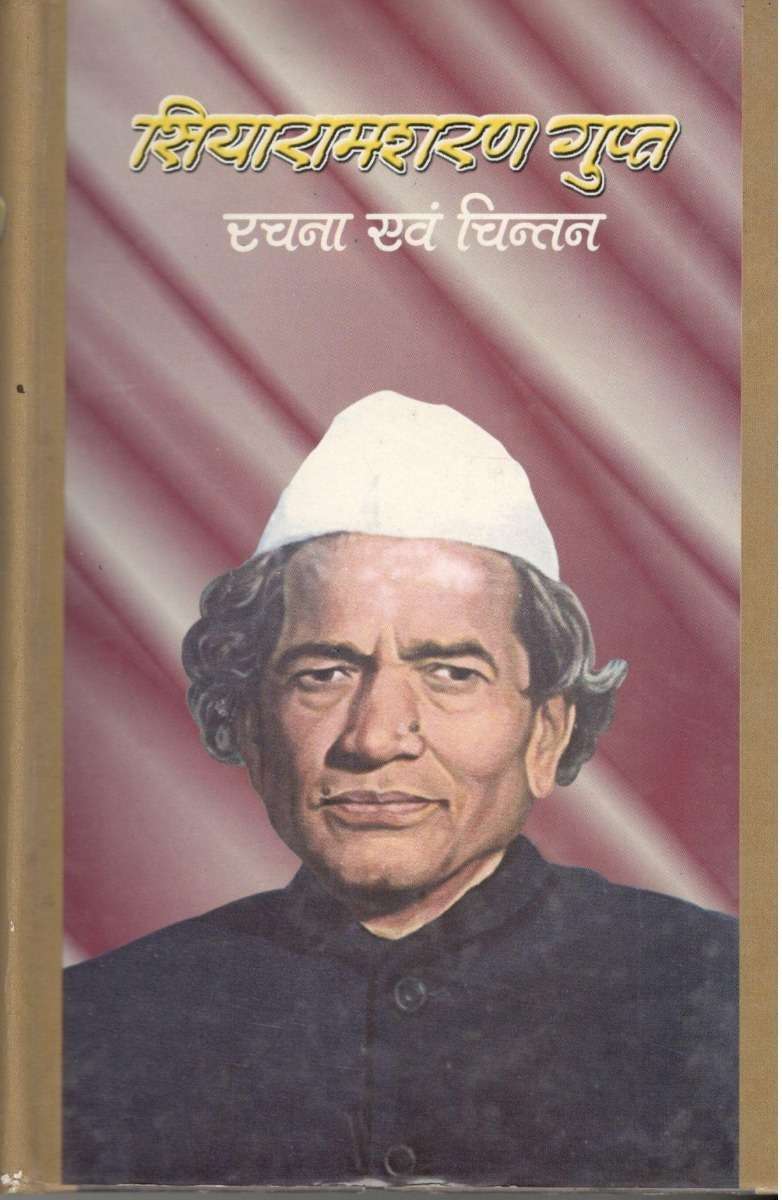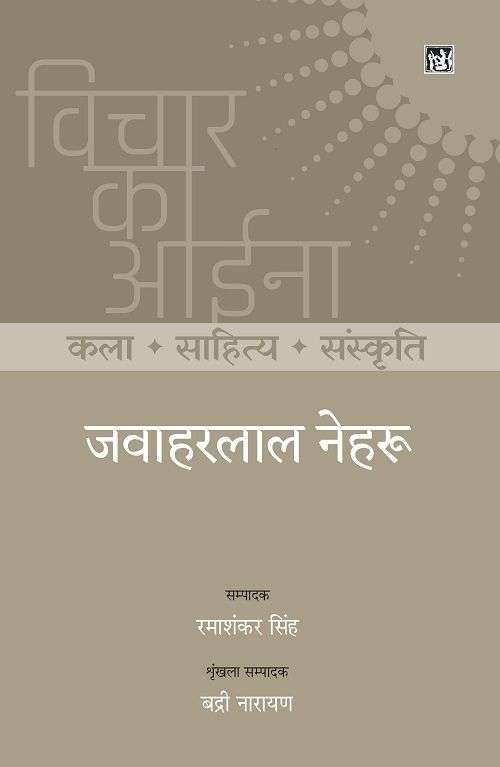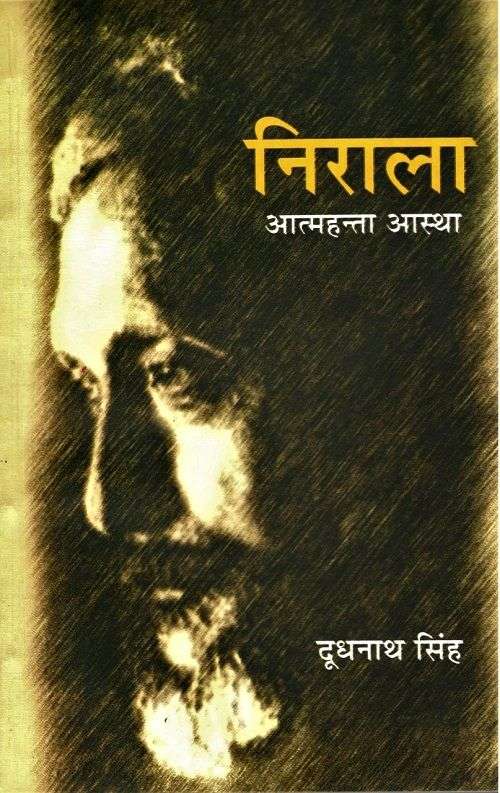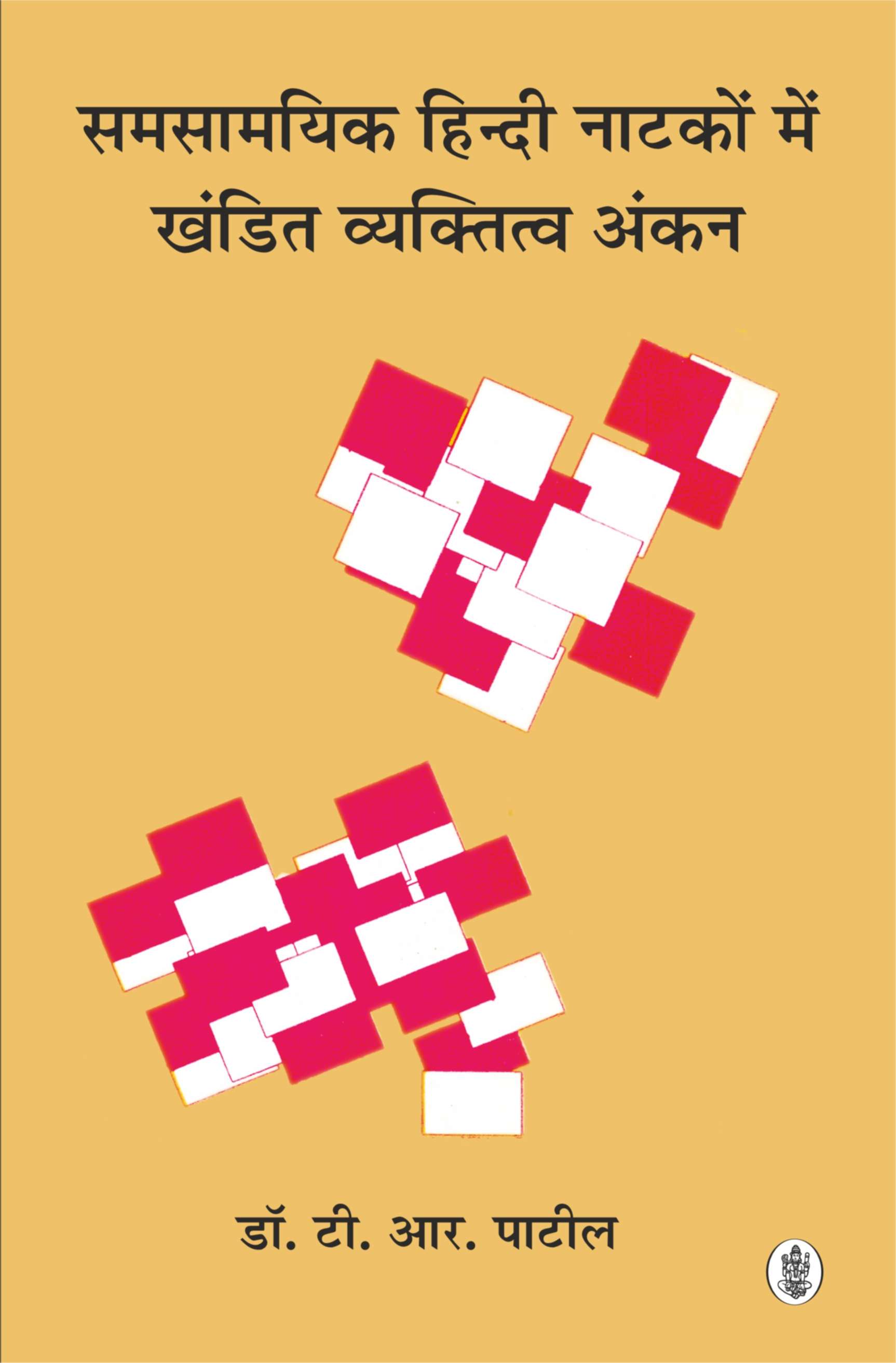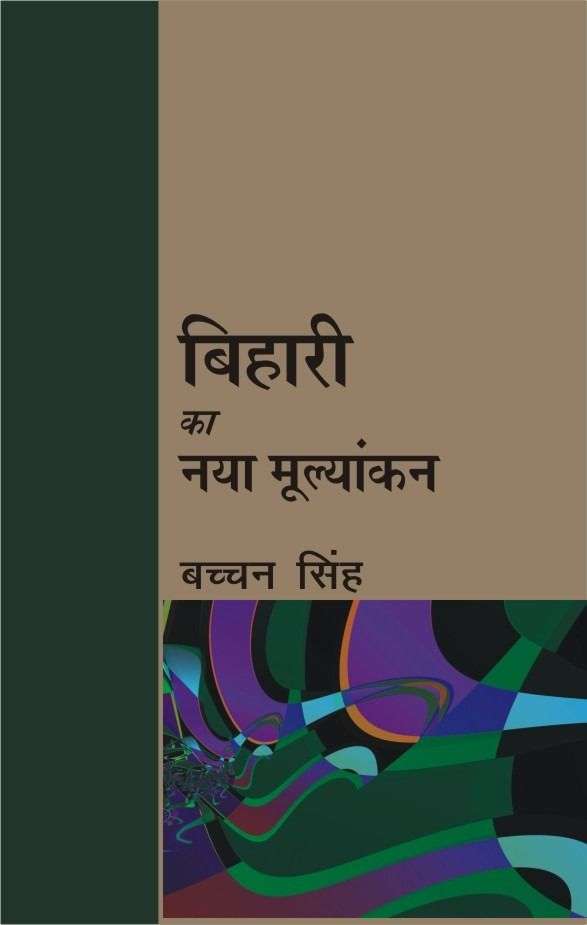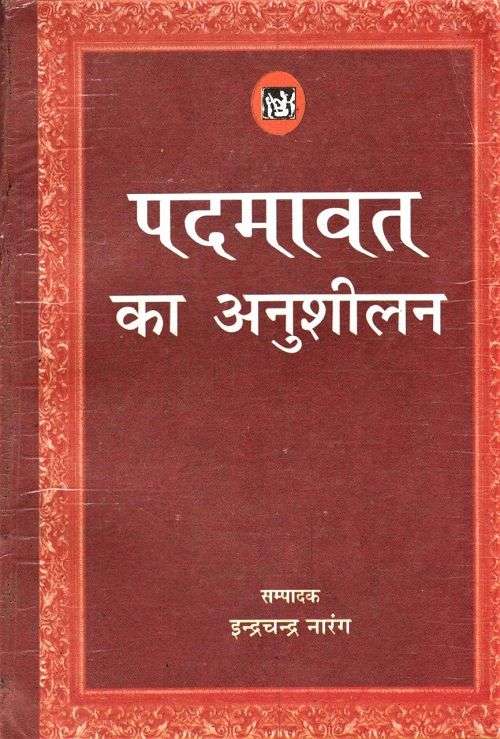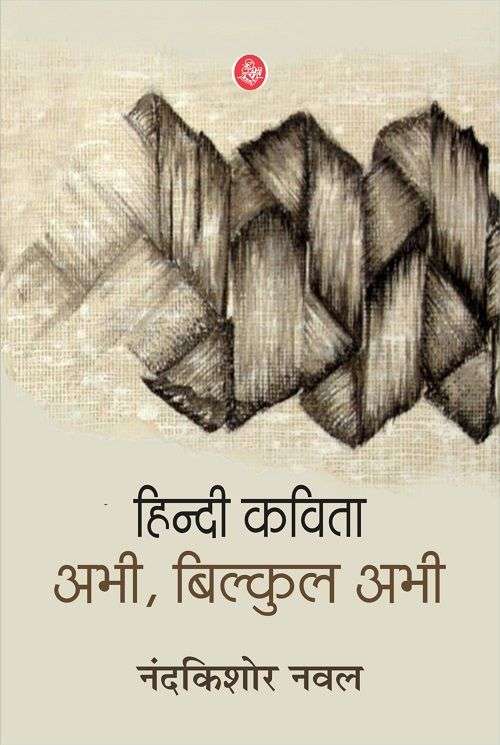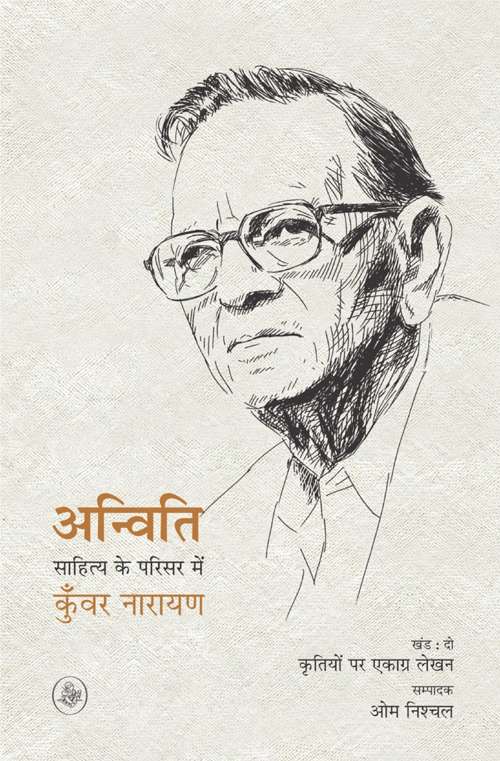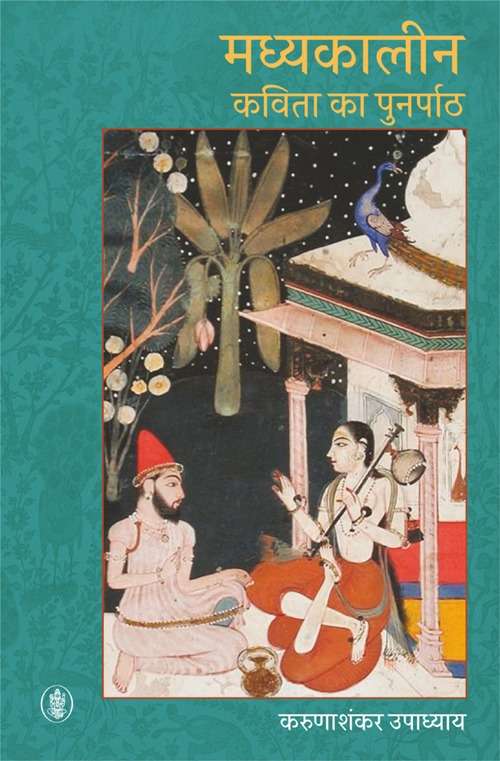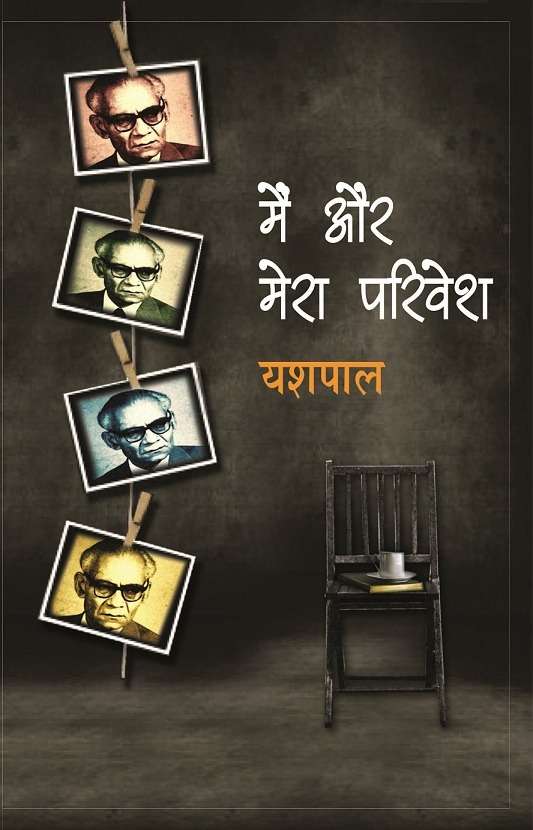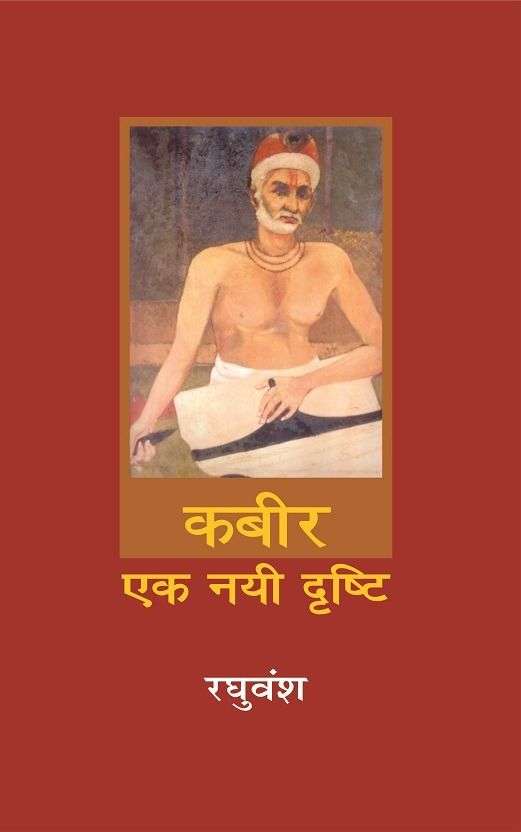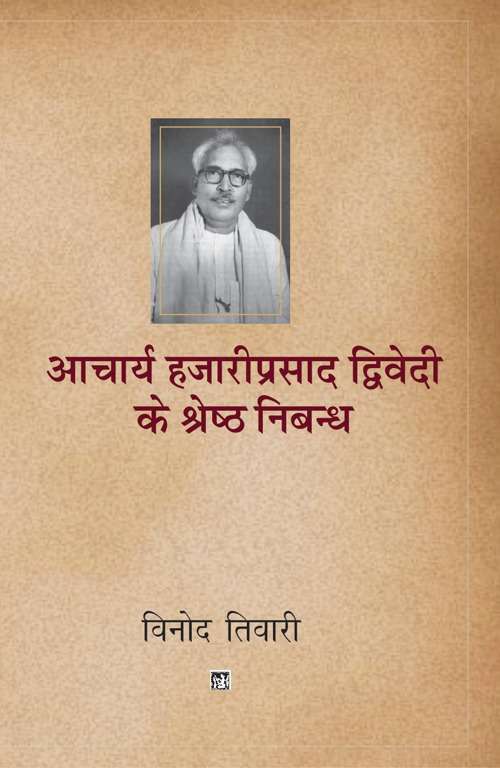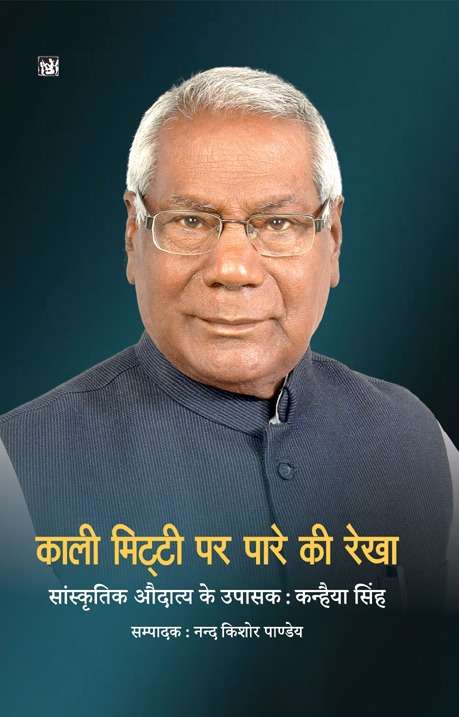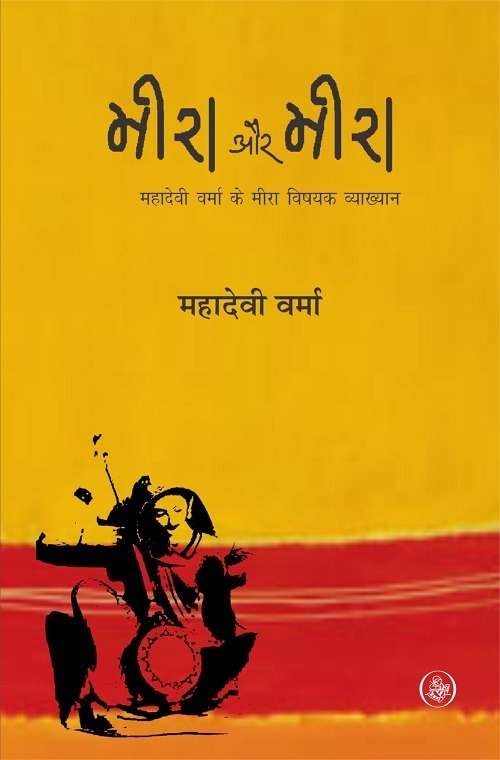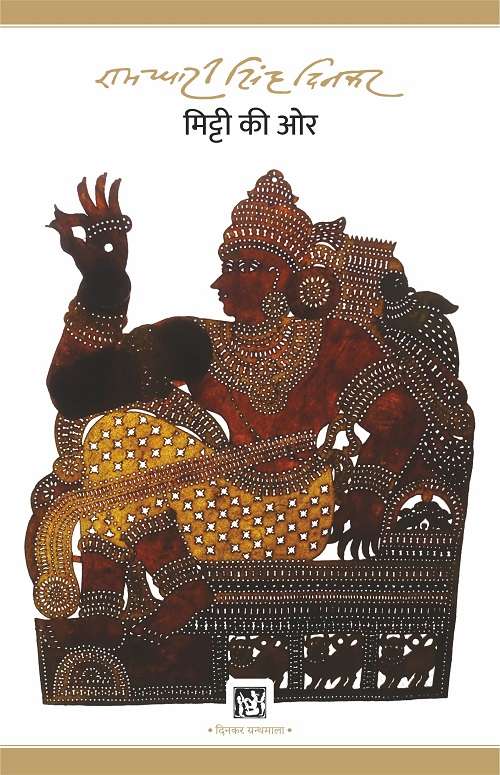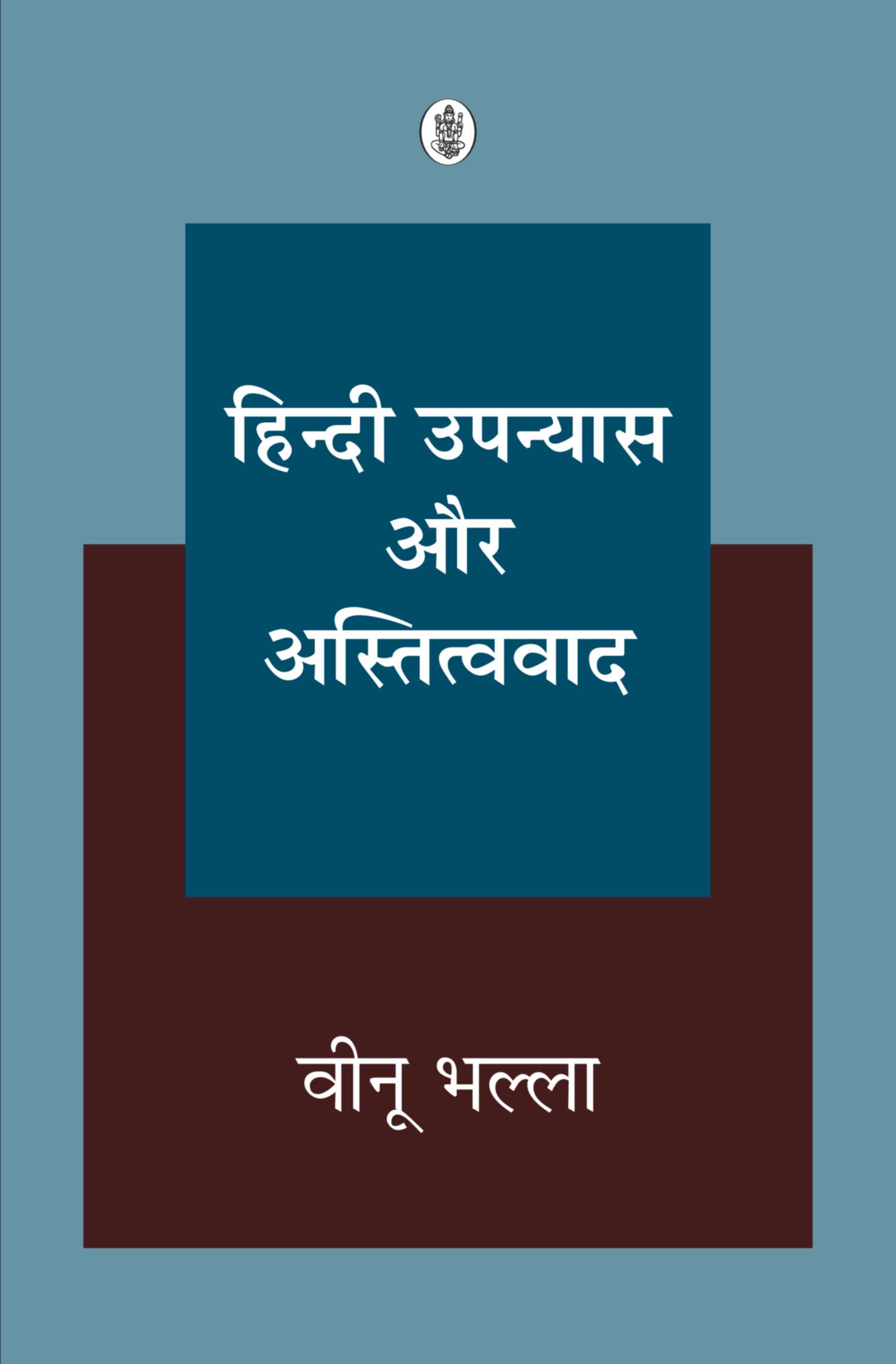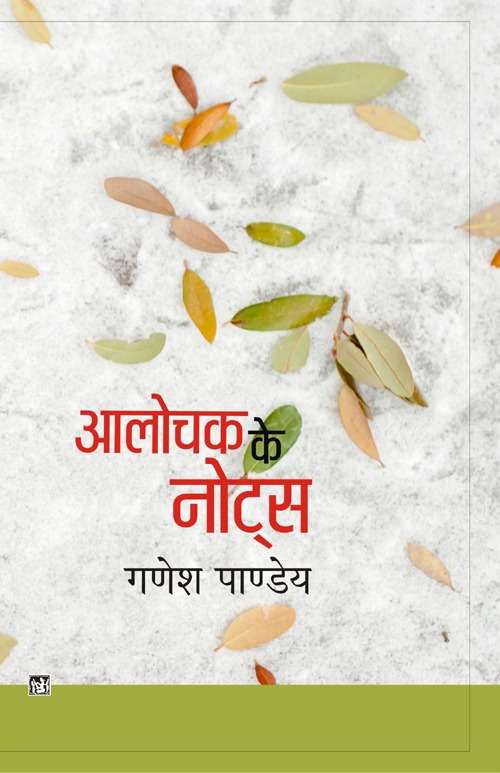
Aalochak Ke Notes
Author:
Ganesh PandeyPublisher:
Rajkamal Prakashan SamuhLanguage:
HindiCategory:
Language-linguistics0 Ratings
Price: ₹ 320
₹
400
Available
‘आलोचक के नोट्स' गणेश पाण्डेय की आलोचना की नई किताब है। उनकी आलोचना अपने समय के साहित्यक परिदृश्य पर एक ज़रूरी हस्तक्षेप है। आलोचना से रचना और रचना से आलोचना का काम लेना लेखक की ख़ूबी है। उनके लिए आलोचना का मतलब पाठकों के भीतर ज़रूरी बेचैनी और सवाल पैदा करना है। इसीलिए अपनी आलोचना में सुन्दर कविता बरक्स मज़बूत कविता का सवाल उठाते हैं। वे अपने समय की रचना और आलोचना की दुनिया की निर्मम चीरफाड़ करना साहित्य के सुदीर्घ और स्वस्थ जीवन के लिए ज़रूरी मानते हैं। रचना और आलोचना, दोनों की प्रवृत्तियों और विचलन पर नज़र रखते हैं। यह बताना ज़रूरी है कि कवि के रूप में भी गणेश पाण्डेय एक पल के लिए भी आलोचक के दायित्व से मुक्त नहीं होते। जैसे उनके दिमाग़ में कोई पेंसिल है, आप से आप नोट करती रहती है, कवि और आलोचक की कारस्तानी। उनकी आलोचना हिन्दी की प्रशंसामूलक आलोचना का विकास ऩहीं है। वे आलोचना में उद्धरणों की कबूतरबाज़ी और क़तरनबाज़ी में विश्वास नहीं करतें हैं, बल्कि उसका जमकर विरोध करते हैं, उसे आलोचना की मुंशीगीरी कहते हैं। आलोचना अपने विस्तार में नहीं, कई बार सूत्रों में ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आलोचना में छोटी और लक्ष्य-केन्द्रित टिप्पणियाँ ज़्यादा मूल्यवान होती हैं। रचना और आलोचना के कोने-अन्तरे में छिपे अँधेरे पर आलोचक की उठी हुई एक उँगली, किसी किताब, लेखकों की किसी पीढ़ी, किसी समूह, किसी सूची की आँख मूँदकर की गई महाप्रशंसा को चीर देती है। पाठक अनुभव करेंगे कि ‘आलोचक के नोट्स’ के लेख और नोट्स उन्हें अपनी तर्कशीलता, सर्जनात्मकता और चुम्बक जैसी भाषा से अपना बना लेंगे; ऐसी पठनीयता विरल है।
ISBN: 9789388211222
Pages: 206
Avg Reading Time: 7 hrs
Age: 18+
Country of Origin: India
Recommended For You
Prayojanmulak Hindi Ki Nai Bhumika
- Author Name:
Kailash Nath Pandey
- Book Type:

-
Description:
भाषा किसी भी देश की संस्कृति का अक्षय कोष होती है। यही परम्परा से संस्कृति के विचारों को लेकर आधुनिकता से मिलाती है। वस्तुत: भाषा जुम्मा-जुम्मा कह चुकने का अमूर्त माध्यम ही नहीं होती है, बल्कि ख़ुद को अपने समाज और परम्परा से जोड़े रखने का प्रेम-बन्धन भी है। वह भटकाव और गुमनामी के अँधेरे में आस्था की अक्षत मशाल बन 'गाइड' की तरह आगे-आगे चल राह दिखाती है। सौभाग्य से, भारतीय सर्जनात्मकता का अपराजेय संकल्प हिन्दी उक्त सभी गुणों को जीती है। व्यक्ति द्वारा विचित्र रूपों में बरती जानेवाली इस हिन्दी भाषा को भाषा-विज्ञानियों ने स्थूल रूप से सामान्य और प्रयोजनमूलक इन दो भागों में विभक्त किया है।
सुखद सूचना यह है कि हिन्दी की इन नितान्त ताज़ा-टटकी और कई सन्दर्भों में बेहद नई भाषिक-संरचना या नवजात शिशु रूप को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ-साथ तक़रीबन हर प्रादेशिक विश्वविद्यालयों ने अपने-अपने पाठ्यक्रमों में शामिल कर इसे सम्मानित किया है। प्रयोजनमूलक हिन्दी आज इस देश में बहुत बड़े फलक और धरातल पर प्रयुक्त हो रही है। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच संवादों का पुल बनाने में आज इसकी महती भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आज इसने एक ओर कम्प्यूटर, टेलेक्स, तार, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीप्रिंटर, दूरदर्शन, रेडियो, अख़बार, डाक, फ़िल्म और विज्ञापन आदि जनसंचार के माध्यमों को अपनी गिरफ़्त में ले लिया है, तो वहीं दूसरी ओर शेयर बाज़ार, रेल, हवाई जहाज़, बीमा उद्योग, बैंक आदि औद्योगिक उपक्रमों, रक्षा, सेना, इंजीनियरिंग आदि प्रौद्योगिकी संस्थानों, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों, आयुर्विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, ए.एम.आई.ई. के साथ विभिन्न संस्थाओं में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सरकारी-अर्द्धसरकारी कार्यालयों, चिट्ठी-पत्री, लेटर पैड, स्टॉक-रजिस्टर, लिफ़ाफ़े, मुहरें, नामपट्ट, स्टेशनरी के साथ-साथ कार्यालय-ज्ञापन, परिपत्र, आदेश, राजपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, प्रेस-विज्ञप्ति, निविदा, नीलाम, अपील, केवलग्राम, मंजूरी पत्र तथा पावती आदि में प्रयुक्त होकर अपने महत्त्व को स्वत: सिद्ध कर दिया है।
कुल मिलाकर यह कि पर्यटन बाज़ार, तीर्थस्थल, कल-कारख़ाने, कचहरी आदि अब प्रयोजनमूलक हिन्दी की जद में आ गए हैं। हिन्दी के लिए यह शुभ है। अनेक विद्वानों के सहयोग से लिखी यह गम्भीर कृति अपने पाठकों को सन्तुष्ट अवश्य करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
Uma Nehru Aur Striyon Ke Adhikar
- Author Name:
Pragya Pathak
- Book Type:

-
Description:
भारत में स्त्री-आन्दोलन के लिहाज़ से बीसवीं सदी के शुरुआती तीन दशक बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। स्वतंत्रता आन्दोलन के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर जो आत्ममंथन की प्रक्रिया चल रही थी, उसी के एक बड़े हिस्से के रूप में स्त्री-स्वातंत्र्य की चेतना भी एक ठोस रूप ग्रहण कर रही थी।
हिन्दी में तत्कालीन नारीवादी चिन्तन में जिन लोगों ने दूरगामी भूमिका अदा की उनमें उमा नेहरू अग्रणी हैं। यह देखना दिलचस्प है कि स्त्री की निम्न दशा के लिए उनकी आर्थिक पराधीनता मुख्य कारण है, इस सच्चाई को उन्होंने उसी समय समझ लिया था; और पुरुष नारीवादियों द्वारा पाश्चात्य स्त्री-छवि के सन्दर्भ में किए गए ‘किन्तु-परन्तु’ वाले नारी-विमर्श की सीमाओं को भी। उमा नेहरू ने इन दोनों बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए स्त्री-पराधीनता और स्वाधीनता, दोनों की ठीक-ठीक पहचान की।
‘अच्छी स्त्री’ और ‘स्त्री के आत्मत्याग’ जैसी धारणाओं पर उन्होंने निर्भीकतापूर्वक लिखा कि ‘जो आत्मत्याग अपनी आत्मा, अपने शरीर का विनाशक हो...वह आत्महत्या है।’ भारतीय समाज के अन्धे परम्परा-प्रेम पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और राजनीतिक प्रश्नों के अलावा जो सबसे बड़ा प्रश्न संसार के सामने है, वह यह कि आनेवाले समय और समाज में स्त्री के अधिकार क्या होंगे।
यह पुस्तक उमा नेहरू के 1910 से 1935 तक विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छपे आलेखों का संग्रह है। संसद में दिए उनके कुछ भाषणों को भी इसमें शामिल किया गया है जिनसे उनके स्त्री-चिन्तन के कुछ और पहलू स्पष्ट होते हैं।
परम्परा-पोषक समाज को नई चेतना का आईना दिखानेवाले ये आलेख आज की परिस्थितियों में भी प्रासंगिकता रखते हैं और भारत में नारीवाद के इतिहास को समझने के सिलसिले में भी।
Siya Ram Sharan Gupt : Rachana Avam Chintan
- Author Name:
Lalit Shukla
- Book Type:

- Description: Awating description for this book
Vichar Ka Aina : Kala Sahitya Sanskriti : Jawaharlal Nehru
- Author Name:
Jawaharlal Nehru
- Book Type:

-
Description:
विचार का आईना शृंखला के अन्तर्गत ऐसे साहित्यकारों, चिन्तकों और राजनेताओं के ‘कला साहित्य संस्कृति’ केन्द्रित चिन्तन को प्रस्तुत किया जा रहा है जिन्होंने भारतीय जनमानस को गहराई से प्रभावित किया। इसके पहले चरण में हम मोहनदास करमचन्द गांधी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, राममनोहर लोहिया, रामचन्द्र शुक्ल, सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’, महादेवी वर्मा, सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन ‘अज्ञेय’ और गजानन माधव मुक्तिबोध के विचारपरक लेखन से एक ऐसा मुकम्मल संचयन प्रस्तुत कर रहे हैं जो हर लिहाज से संग्रहणीय है।
जवाहरलाल नेहरू ऐसे चिन्तक राजनेता हैं जिन्होंने भारत को आधुनिक विश्व परिदृश्य में एक समर्थ देश के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। जिनके दिखाए रास्ते पर आधुनिक भारत आगे बढ़ा। गांधी की अगुआई में स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय नेहरू लम्बे समय तक जेलों में रहे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का सपना देखा जिसने दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया। उनके मन में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बहुलता के प्रति अथाह सम्मान था। आज जब भारत की सांस्कृतिक बहुलता को खंडित करने का सपना देखनेवाली राजनीतिक ताकतें मजबूत हुई हैं, ऐसे में हमें उम्मीद है कि नेहरू के कला, साहित्य और संस्कृति सम्बन्धी प्रतिनिधि निबन्धों की यह किताब भारत की सांस्कृतिक विरासत और बहुलता को दूर करने और उनकी अपरिहार्य आवश्यकता को समझाने में सहायक होगी।
Mopala Kand-1921
- Author Name:
Go. Sthanumalayan
- Book Type:

- Description: 1921 में केरल के मलबार में मोपलाओं द्वारा किए गए हिंदू नरसंहार के जघन्य कुकृत्य को एक शताब्दी बीत चुकी है | लेकिन इस लंबे कालखंड में भी इस बृशंस हत्याकांड के बारे में झूठा और मिथ्या दुष्प्रचार किया जाता रहा | हिंदुओं पर अत्याचार करना, हिंदुओं की संपत्तियों को लूटना, धर्मांतरण आदि जैसे नीच कार्य करनेवालों को स्वतंत्रता सेनानी के समान जनता के सामने पेश करने का दुस्साहस वामपंथियों की बौद्धिक रीति का आक्रमण ही है ।कांग्रेस और वामपंथियों ने मोपला दंगे को स्वतंत्रता-संग्राम और किसानों के आंदोलन के रुप में प्रस्तुत कर इतिहास को बदलने का अक्षम्य कार्य किया | साजिश के तहत मोपला दंगे को कांग्रेस व कम्युनिस्टों ने मजदूरों और जमींदारों के बीच का झगड़ा बताया | आध्यात्मिक प्रदेश केरल में बेचारी अल्पसंख्यक हिंदू जनता ने मुसलमानों के अत्याचारों और बर्बरता की जितनी यातनाएँ झेलीं, उन्हें ठोस प्रमाण के साथ लेखक ने इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है मंदिरों को ध्वस्त करना, स्त्रियों का मान भंग करना, हिंदुओं की संपत्तियों को लूटना, हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराना तथा दंगों के समय भारत के अन्य प्रदेशों से मोपलाओं को इस कुकृत्य में मदद मिली-ऐसे अनेक विषयों का भी उल्लेख लेखक ने इस पुस्तक में किया है | आज की पीढ़ी हिंदुओं के उस बीभत्स नरसंहार के पीछे की कुत्सित मानसिकता को जान पाए, इस मंतव्य से यह पुस्तक लिखी गई है |
Main Aryaputra Hoon
- Author Name:
Manoj Singh
- Book Type:

- Description: ‘‘हे आर्य! कोई बाहरी आक्रमणकारी जब किसी अन्य देश में प्रवेश करता है तो बाहर से भीतर आता है या भीतर से बाहर जाता है?’’ ‘‘यह कैसा प्रश्न हुआ, आर्या! स्वाभाविक रूप से बाहर से भीतर आता है।’’ ‘‘और इसी स्वाभाविक तर्क के आधार पर ही मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। अगर यह मान लिया जाए कि हम आर्य बाहर से आए थे तो पश्चिम दिशा से प्रवेश करने पर सर्वप्रथम सिंधु के तट पर बसना चाहिए था और फिर पूरब दिशा की ओर बढ़ना चाहिए था। लेकिन वेद और पुरातत्त्व के प्रमाण कहते हैं कि हम आर्य पहले सरस्वती के तट पर बसे थे, फिर सिंधु की ओर बढ़े। यही नहीं, सरस्वती काल से भी पहले हम आर्यों का इतिहास विश्व की प्राचीनतम नगरी शिव की काशी और मनु की अयोध्या से संबंधित रहा है। और ये दोनों नगर भारत भूखंड के भीतर सरस्वती नदी की पूरब दिशा में हैं अर्थात् हम आर्य पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बढ़े थे।...तो फिर ये कैसे बाहरी (?) आर्य थे जो भीतर से बाहर (!!) की ओर बढ़े थे।...झूठ के पाँव नहीं होते हैं आर्य, ये झूठे इतिहासकार आपके प्रामाणिक प्रश्नों के उत्तर क्या ही देंगे, जब ये मेरे इस सरल तर्क और सामान्य तथ्य पर बात नहीं कर सकते।’’ ‘‘असाधारण तर्क आर्या!’’
Nirala : Aatmhanta Astha
- Author Name:
Doodhnath Singh
- Book Type:

- Description: ‘निराला : आत्महन्ता आस्था’ दरअसल एक नए कवि-कथाकार द्वारा एक-दूसरे कवि का आत्मीय विश्लेषण है। इसका एक नाम यह भी हो सकता था—‘एक लेखक की निजी नोट-बुक में एक दूसरा लेखक’। यह पुस्तक लेखक के उन्हीं ‘नोट्स’ का क्रमबद्ध रूपान्तरण है, उसके निजी आनन्द की अभिव्यक्ति है। लेकिन आनन्द की यह अभिव्यक्ति लेखक के श्रद्धा-विगलित क्षणों की उपज न होकर, उसके दिमाग़ की तार्किक रस-सिद्धि का परिणाम है; उसके सधे हुए सुर की झंकार है। अत: उसमें एक तर्कपूर्ण निजी शास्त्रीयता भी है। इसीलिए वह मात्र प्रशस्ति-वाचन या निन्दा नहीं है, बल्कि निराला की काव्य-ऊर्जा तक पहुँचने के लिए बनाया गया एक नया और निजी द्वार है, जिससे जागरूक पाठक और नए आलोचक एक नई जगह से उस सिंह के दर्शन कर सकें। जब आप इस नए द्वार से प्रवेश करेंगे—तभी समझ सकेंगे कि क्यों निराला दूसरे छायावादी कवियों से विरोधी दिशा के कवि हैं? क्यों उनको बने-बनाए काव्य-सिद्धान्तों में 'फिट-इन' नहीं किया जा सकता? क्यों उनकी रचनात्मकता का अध्ययन करने के लिए काल-क्रम का आधार बेमानी ठहरता है? तब आप उस अँधेरी गुफा में बैठी, उन जलती आँखों के सान्द्र प्रकाश का साक्षात्कार कर पाएँगे। इसी साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत है यह पुस्तक—‘निराला : आत्महन्ता आस्था’।
Samsaamyik Hindi Natkon Mein Khandit Vyaktitwa Ankan
- Author Name:
Dr. T.R. Pateel
- Book Type:

-
Description:
मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में खंडित व्यक्तित्व एक आधुनिक संकल्पना है। आज का मानव टूटा हुआ, थका हुआ, हारा हुआ व्यक्ति है और इसी कारण उसका व्यक्तित्व भी खंडित है। इस विषय पर फुटकर रूप में कुछ विवेचन कतिपय पुस्तकों में अवश्य हुआ है किंतु अपनी समग्रता में खंडित व्यक्तित्व की परिधि में इसके अध्ययन की आवश्यकता बनी हुई थी। डॉ. टी. आर. पाटील की यह पुस्तक ‘समसामयिक हिंदी नाटकों में खंडित व्यक्तित्व अंकन’ इस अभाव की पूर्ति का एक सफल प्रयास है ।
डॉ. पाटील ने अपनी इस महत्त्वपूर्ण पुस्तक में जहाँ खंडित व्यक्तित्व के अर्थबोध और अर्थ-विस्तार के साथ उसकी अवधारणा पर अपने गम्भीर विचार प्रस्तुत किए हैं, वहीं 1947 से 1985 तक प्रकाशित प्रतिनिधि नाटकों को परिलक्षित कर उनमें अंकित खंडित व्यक्तित्व के विविध आयामों को विवेचित-विश्लेषित किया है। इस संदर्भ में उन्होंने प्रेम और यौन समस्या, आत्मविश्लेषणवाद, मानव का असंगत जीवन, राजनीतिक-आर्थिक चेतना, सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना से प्रभावित हिंदी नाटकों में प्रतिबिंबित खंडित व्यक्तित्व को विस्तार के साथ विश्लेषित किया है।
खंडित व्यक्तित्व को रंगमंच पर प्रस्तुत करने की दृष्टि से नाटककारों ने जिस रंगमंच की अभिनव कल्पना की है उसमें मंच-सज्जा, पात्रों के क्रिया-व्यापार, पात्रों का अतर्द्वंद्व, पात्रों की वेश-भूषा, प्रकाश-योजना, ध्वनि-योजना, गीत-संगीत के विशिष्ट प्रयोग, नव्य यांत्रिक साधन तथा विविध रंगकर्मियों और निर्देशकों का योगदान और दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को दिखाने का जो सफल प्रयास डॉ. पाटील ने किया है, वह इस पुस्तक की एक अनुपम उपलब्धि है।
Bihari Ka Naya Mulyankan
- Author Name:
Bachchan Singh
- Book Type:

- Description: प्रस्तुत पुस्तक में ‘बिहारी सतसई’ का मूल्यांकन करते समय तत्कालीन सामन्तीय परिवेश को बराबर दृष्टि में रखा गया है। बिहारी दरबार में रहते थे, पर उनको दरबारी नहीं कहा जा सकता। उनमें चाटु की प्रवृत्ति नहीं थी, वे वेश-भूषा, रहन-सहन, आन-बान आदि में किसी सामन्त-सरदार से कम न थे, उनका दृष्टिकोण पूर्णतः सामन्तीय था, जो ‘सतसई’ के काव्य तथा शैलीगत सतर्कता और सज्जा में अभिव्यक्त हो उठा है। उनके प्रेम, नारी-सम्बन्धी भाव, गाँव-सम्बन्धी विहार सभी पर सामन्त-कवि की छाप है, दरबारी कवि की नहीं। इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करने पर ही ‘सतसई’ का सम्यक् आकलन किया जा सकता था। इसके लिए भी सतसई को ही साक्ष्य माना गया है। इससे सुविधा भी हुई। तत्कालीन परिस्थिति और राजनीतिक स्थिति के नाम पर कहीं से इतिहास के दस-बीस पृष्ठ फाड़कर चिपकाने नहीं पड़े। ‘नयी-समीक्षा’ का आग्रह भी कुछ ऐसा ही है।
Padmavat Ka Anushilan
- Author Name:
Indra Chandra Narang
- Book Type:

-
Description:
पदमावत ने हमारे इतिहास वाड्मय को अत्यधिक प्रभावित किया है। पदमावत का अध्ययन उसके ऐतिहासिक आधार को टटोलते हुए किया गया है। पद्मावत का अनुशीलन पदमावत के ऐतिहासिक आधार', प्रकाशित होने पर संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित करने की जरूरत महसूस हुई, जिससे जिन पाठकों को पूरी पदमावत पढ़ने का अवकाश नहीं है, वे भी इस अमर काव्य का रसास्वादन कर सकें। प्रस्तुत संग्रह उसी प्रयास का फल है। पदमावत का यह संक्षिप्त संग्रह प्रस्तुत करने में प्रयत्न किया गया है कि-
क. पदमावत के कथानक का सूत्र अटूट बना रहे.
ख. काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट सभी अंशों कासमावेश हो जाय,
ग. पदमावत के सभी पात्रों का चरित्र स्पष्ट हो जाय।
ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गम्भीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। इसके पठन-पाठन का मार्ग कठिनाइयों के कारण अब तक बन्द-सा रहा। एक तो इसकी भाषा पुरानी और ठेठ अवधी, दूसरे भाव भी गूढ़, अतः किसी शुद्ध अच्छे संस्करण के बिना इसके अध्ययन का प्रयास मुश्किल था। पदमावत का अनुशीलन पुस्तक इसी ओर एक प्रयास मात्र है।
Hindi Kavita : Abhi, Bilkul Abhi
- Author Name:
Nandkishore Naval
- Book Type:

-
Description:
अपनी इस पुस्तक में नामवरोत्तर हिन्दी आलोचना के अग्रगण्य आलोचक
डॉ. नंदकिशोर नवल ने अपने समकालीन कवियों की कविता पर विचार किया है। ये वे कवि हैं, जिनके साथ वे उठे हैं, दौड़े हैं और झगड़े हैं; स्वभावत: इन कवियों पर लिखना अग्नि–परीक्षा से गुज़रना था, लेकिन साहित्य की पवित्रता की पूरी तरह से रक्षा करते हुए वे उसमें सफल हुए हैं। कभी–कभी उन्होंने कवियों की त्रुटियों की ओर भी संकेत किया है, लेकिन उसका ज़रूरत से ज़्यादा महत्त्व नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य कवियों के वैशिष्ट्य का निरूपण रहा है और यह कार्य उन्होंने पूरे वैदग्ध्य से किया है। एक पीढ़ी के कवियों की पारस्परिक भिन्नता को रेखांकित करना आसान नहीं है, लेकिन उनकी कविताएँ उनकी नसों में इस क़दर प्रवाहित रही हैं कि उसमें उन्हें ज़रा भी दिक़्क़त नहीं हुई है।डॉ. नवल आलोचना साधारण पाठकों को सामने रखकर लिखते हैं। इतना ही नहीं, वे उनके साथ चलते हैं, उन्हें प्रासंगिक संस्मरण सुनाते हैं और घुमाते हुए कवि की सम्पूर्ण चित्रशाला का दर्शन करा देते हैं। वे उस आलोचना के सख़्त ख़िलाफ़ हैं, जो कविता की ज़मीन छोड़कर चील की तरह आकाश की गहराइयों में उड़ती है और वहाँ उड़ते कीड़ों की जगह पाठकों का शिकार करती है। ऐसी आलोचना पाठकों को आतंकित जितना कर ले, उसकी मित्र और बन्धु नहीं बन पाती।
निश्चय ही आलोचना कविता को कहानी या यात्रा–वर्णन बना देना नहीं है, लेकिन यदि उसे ‘रचना’ का ओहदा प्रदान करना है, तो उसमें रचना जैसी संवेदनशीलता लानी होगी। संवेदनशीलता के साथ स्पष्टता और आत्मीयता डॉ. नवल की ऐसी विशेषताएँ हैं, जिन्हें सराहते ही बनता है। अन्त में उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि ‘अब निर्मल जल–भर है, सेवार नहीं है’।
Anviti - Khand : 2
- Author Name:
Kunwar Narain
- Book Type:

-
Description:
कुँवर नारायण हमारे समय के बड़े कवि हैं। यदि विश्व के कुछ चुनिन्दा कवियों की तालिका बनाई जाए तो उसमें निस्सन्देह उनका स्थान होगा। वे आधुनिक बोध और संवेदना के उन कवियों में हैं जिन्होंने सदैव कविता को मनुष्यता के आभरण के रूप में लिया है।
कुँवर नारायण का काव्य मानवीय गुणों का ही नहीं, मानवीय संस्कारों का काव्य है। कविता में उनका प्रवेश चक्रव्यूह से हुआ। अपने गठन में कलात्मक किन्तु दार्शनिक प्रतीतियों वाले इस संग्रह में जीवन की पेचीदगियों को कवि ने सलीक़े से उठाया है। ‘आत्मजयी’ की लगभग अधसदी के बाद ‘वाजश्रवा के बहाने’ की रचना बतौर कुँवर नारायण यह भी जताने के लिए है कि यदि ‘आत्मजयी’ में मृत्यु की ओर से जीवन को देखा गया है तो ‘वाजश्रवा के बहाने’ में जीवन की ओर से मृत्यु को देखने की एक कोशिश है। उनके इस कथन को हम इस रोशनी में देख सकते हैं कि सारा कुछ हमारे देखने के तरीक़े पर निर्भर है—कुछ ऐसे कि यह जीवन विवेक भी एक श्लोक की तरह सुगठित और अकाट्य हो।
उनके रचना-संसार पर समय-समय पर लिखा जाता रहा है। अनेक शोधार्थियों ने उनके व्यक्तित्व और साहित्य पर कार्य किया है। कहना न होगा कि कुँवर नारायण का कृतित्व बहुवस्तुस्पर्शी है। वर्ष 2002 से पहले तक उनके व्यक्तित्व एवं कृतियों पर लिखे महत्त्वपूर्ण लेख ‘उपस्थिति’ नामक संचयन में समाविष्ट हैं। उसके पश्चात् लिखे निबन्धों का यह संकलन दो खंडों में है : ‘अन्वय’ और ‘अन्विति’। ‘अन्विति’ उनकी कृतियों को केन्द्र में रखकर लिखे आलोचनात्मक निबन्धों का चयन है। इसमें हाल की कुछ प्रकाशित कृतियों को छोड़कर बाक़ी कृतियों पर लिखे लेखों को शामिल किया गया है जो उपस्थिति में सम्मिलित नहीं हैं। अधिकांश लेख 2015 तक के हैं जब कुँवर नारायण का प्रबन्ध-काव्य ‘कुमारजीव’ प्रकाशित हुआ।
आशा है, पाठकों को ये दोनों खंड उपयोगी और प्रासंगिक लगेंगे तथा कुँवर नारायण के साहित्य के प्रति रुचि विकसित करेंगे।
Madhyakaleen Kavita Ka Punarpaath
- Author Name:
Karunashankar Upadhyay
- Book Type:

-
Description:
मध्यकालीन साहित्य अपने व्यापक सन्दर्भों और उदात्त मूल्यबोध के कारण निरन्तर प्रासंगिक रहा है। दलितों, वंचितों, पीड़ितों, उपेक्षितों और स्त्रियों समेत जीवमात्र के प्रति गहरी सहानुभूति और संवेदनशीलता के रूप में लोकमंगल की जो भावना इसमें दिखाई पड़ती है, उसने इसको आज और अधिक प्रासंगिक बना दिया है। लेकिन मध्यकालीन साहित्य शास्त्रीय रूढ़ियों, सामाजिक वर्जनाओं, धार्मिक संकीर्णताओं आदि के विरुद्ध लोकचेतना के उन्मेष से उपजे इस साहित्य की अर्थवत्ता को वर्तमान सन्दर्भों में समझने-समझाने के लिए इस पर नए सिरे से दृष्टि डालना आवश्यक है। यह पुस्तक यही काम करती है।
पाठ केन्द्रित आलोचना पर ज़ोर देते हुए यह पुस्तक मध्यकालीन साहित्य को समाज, वस्तु, घटना, विचार, परिवर्तन, अन्तर्वृत्तियों और व्यक्तियों की सापेक्षता में विश्लेषित-मूल्यांकित करती है, ताकि उसका वस्तुनिष्ठ और मानक पाठ तैयार किया जा सके। यह सप्रमाण दिखलाती है कि सतर्क पाठ-विश्लेषण न केवल इस साहित्य के बहुस्तरीय और गहन अर्थ को उद्घाटित कर सकता है, बल्कि युग सापेक्ष दृष्टिबोध भी प्रस्तुत कर सकता है।
इसमें भक्ति साहित्य और रीति साहित्य, दोनों पर विचार किया गया है। मध्यकालीन साहित्य के कवियों की निजी अनुभूति के ‘स्व’ से ‘पर’ और ‘पर’ से ‘सर्व’ में रूपान्तरण और लोकसत्ता से एकाकार होकर सार्वभौम होने की प्रक्रिया का उद्घाटन इस पुस्तक की उल्लेखनीय विशेषता है।
निश्चय ही, यह पुस्तक मध्यकालीन साहित्य के अध्येताओं के साथ-साथ सामान्य पाठकों के लिए भी पठनीय और संग्रहणीय सिद्ध होगी।
Main Aur Mera Parivesh
- Author Name:
Yashpal
- Book Type:

- Description: यशपाल की मूल पहचान भले ही एक कथाकार की हो, लेकिन कथा-साहित्य के बाहर भी उन्होंने बहुत-कुछ लिखा था। उनका यह लेखन उनके पर्याप्त लम्बे और व्यवस्थित रचनाकाल में समय की अपनी ज़रूरतों एवं दबावों के हिसाब से हुआ। ‘विप्लव’ के सम्पादकीय, क्रान्तिकारी जीवन के अपने संस्मरणों, यात्रावृत्त, प्रगतिशील लेखक संघ की गतिविधियों के सम्बन्ध में अभिभूत टिप्पणियों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में उन्होंने राजनीतिक निबन्ध भी लिखे। यशपाल के बारे में एक आम धारणा यह है कि अपने वैचारिक आग्रहों के प्रति वे बहुत अनन्य और दृढ़ थे। इसी कारण अपने समय के साहित्यिक-राजनीतिक विवादों और बहसों में भी उनकी सक्रिय हिस्सेदारी रही। मार्क्सवादी और ग़ैर-मार्क्सवादी दोनों तरह के आलोचकों के विरोध के बीच उनका लेखन हुआ। जब-तब उन्हें अपने इन आलोचकों से भी उलझना होता था, भरसक सैद्धान्तिक रूप में वे अपना पक्ष रखते थे। अनुशासन, व्यवस्था और निरन्तरता सम्भवत: यशपाल के लेखन के केन्द्रीय सूत्र हैं। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर तो लिखा ही, व्यक्तिगत सन्दर्भों पर उनका आत्मगत लेखन भी काफ़ी मात्रा में है। यशपाल के असंकलित इन लेखों में बहुत-सी ऐसी सामग्री है जो आत्मगत प्रकृति की है। इस सामग्री को एक जगह देख और पढ़कर किसी को भी आश्चर्य हो सकता है। यहाँ अपने लेखकीय जीवन के वैविध्यपूर्ण अनुभवों का खुलासा उन्होंने किया है—कभी अपनी इच्छा से और कभी दूसरों के अनुरोध पर। इस संकलन में उनके अनेक विवादास्पद लेख भी हैं जो इधर वर्षों से अप्राप्य थे। इस ढेर सारी सामग्री के एक जगह उपलब्ध हो जाने से यशपाल जैसे बड़े क़द-बुत के लेखक की रचना-प्रक्रिया और रचनात्मक सरोकारों की दृष्टि से भी इस सामग्री का अपना महत्त्व है।
Kabeer : Ek Nai Drishti
- Author Name:
Raghuvansh
- Book Type:

- Description: कबीर अपनी वाणी के विभिन्न अंगों के अन्तर्गत व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक-सामाजिक सम्बन्धों, आर्थिक-राजनीतिक परिस्थितियों से धर्म, साधना और अध्यात्म क्षेत्र तक के मूल्य-बोध को अनेक स्तरों पर नाना रूपों तथा विभिन्न आयामों में अभिव्यक्त करते हैं। उन्होंने प्रचलित-परम्परित रूढ़ियों, मान्यताओं, विकृतियों-विडम्बनाओं तथा मूल्यहीनताओं का प्रभावी शैली में खंडन तथा विघटन किया है।
Aacharya Hazariprasad Dwivedi ke Shresth Nibandh
- Author Name:
Hazariprasad Dwivedi
- Book Type:

- Description: आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का रचना-संसार वैविध्यपूर्ण और साहित्यिक व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे संस्कृत के शास्त्री थे, ज्योतिष के आचार्य। कवि, आलोचक, उपन्यासकार, निबन्धकार, सम्पादक, अनुवादक और भी न जाने क्या-क्या थे। वे पंडित भी थे और प्रोफ़ेसर भी, आचार्य तो थे ही। वे अपने समय के एक बहुत ही अच्छे वक्ता थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे एक कुशल अध्यापक और सच्चे जिज्ञासु अनुसन्धाता थे। बलराज साहनी ने उनकी इस अनुसंधान वृति को लक्षित करते हुए लिखा है, ‘‘सूई से लेकर सोशिलिज्म तक सभी वस्तुओं का अनुसन्धान करने के लिए वे उत्सुक रहते।’’ तभी तो वे, बालू से भी तेल निकाल लेने की बात करते हैं, अगर सही और ठीक ढंग का बालू मिल जाए। उनके इस अनुसन्धान और अध्ययन-मनन की सबसे बड़ी ताक़त थी एक साथ कई भाषाओं और परम्पराओं की जानकारी। वे जहाँ संस्कृत, पालि, प्राकृत और अपभ्रंश जैसी प्राचीन भारतीय भाषाओं के साथ भारतीय साहित्य, दर्शन चिन्तन की ज्ञान-परम्पराओं को अपनी सांस्कृतिक-चेतना में धारण किए हुए थे, वहीं हिन्दी, अंग्रेज़ी, बांग्ला और पंजाबी जैसी आधुनिक भारतीय व विदेशी भाषाओं के साथ आधुनिक ज्ञान-परम्परा को भी। परम्परा और आधुनिकता का ऐसा मेल कम ही साहित्यकारों में देखने को मिलता है। परम्परा और आधुनिकता के इस प्रीतिकर मेल से उन्होंने हिन्दी साहित्य-शास्त्र को मूल्यांकन का एक नया आयाम दिया। लोक और शास्त्र को जिस इतिहास-बोध से द्विवेदी जी ने मूल्यांकित किया है, वह इस नाते महत्त्वपूर्ण है कि उसमें किसी तरह का महिमामंडन या भाव-विह्वल गौरव गान नहीं मिलता, बल्कि एक वैज्ञानिक चेतना सम्पन्न सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि मिलती है, जिसका पहला और आख़िरी लक्ष्य मनुष्य है—उसका मृत्य, उसकी मबीता और उसका श्रम है।
Kali Mitti Par Pare Ki Rekha
- Author Name:
Kanhaiya Singh
- Book Type:

-
Description:
डॉ. कन्हैया सिंह जी अपने यशस्वी जीवन के 85वें वर्ष पूर्ण कर 86वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर प्रकाशित यह ग्रन्थ पूरे देश के विद्वानों से प्राप्त पत्र-पुष्प है। अल्प समय में इतनी बड़ी संख्या में विद्वानों ने अपने आलेख भेजे हैं जो डॉ. कन्हैया सिंह जी की कीर्ति और साहित्यिक सक्रियता का परिणाम है। राजस्थान के माननीय राज्यपाल
श्री कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोवा की पूर्व राज्यपाल माननीय मृदुला सिन्हा, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के पूर्व उपाध्यक्ष, डॉ. कमल किशोर गोयनका के आलेख ने इस ग्रन्थ की गरिमा को बढ़ाया है। हिन्दी के अनेक यशस्वी साहित्यकारों और आलोचकों के साथ ही युवा लेखकों की भागीदारी ने भी इसे महत्त्वपूर्ण बनाया है।डॉ. कन्हैया सिंह जी का जीवन और उनके द्वारा रचित समस्त साहित्य को केन्द्र में रखते हुए इस पुस्तक को पाँच खंडों में संयोजित किया गया है—‘जीवन पर्व : संघर्ष एवं साधना का उज्ज्वल इतिहास’ पहला खंड है। जिसमें विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गए संस्मरण और
डॉ. कन्हैया सिंह जी के जीवन सम्बन्धी आलेख हैं। पुस्तक का द्वितीय खंड ‘सृजन पर्व : विचार एवं वैभव का ताना-बाना’ है, जिसमें डॉ. सिंह के सृजनात्मक साहित्य को केन्द्र में रखकर लिखे गए आलोचनात्मक लेखों का संकलन किया गया है। इस पुस्तक के तृतीय खंड ‘भाषा पर्व : अक्षर-अक्षर भेद’ में डॉ. कन्हैया सिंह जी के पाठ-सम्पादन एवं भाषाविज्ञान सम्बन्धी कार्यों पर लिखे गए समीक्षात्मक लेखों को संयोजित किया गया है। ‘संस्कृति पर्व : समष्टि का रचनात्मक उछाह’ जो कि पुस्तक का चतुर्थ खंड है, में डॉ. कन्हैया सिंह जी द्वारा किए गए सूफ़ी साहित्य, सन्त साहित्य तथा इतिहास लेखन विषयक कार्यों की समीक्षा है। पुस्तक का पाँचवाँ और अन्तिम खंड ‘चिट्ठी-विट्ठी : हाल-ए-ज़ुबानी और’ है। इसमें हिन्दी जगत के विभिन्न प्रतिष्ठित साहित्यकारों, समाजसेवियों और प्रमुख राजनेताओं का डॉ. कन्हैया सिंह जी के साथ पत्र-व्यवहार एवं उन पर लिखित आलेख सम्मिलित हैं। साथ ही डॉ. कन्हैया सिंह जी का साक्षत्कार भी इसी खंड में संगृहीत है।यह पुस्तक हिन्दी के अध्येताओं के लिए हिन्दी पाठानुसन्धान, सूफ़ी साहित्य, सन्त साहित्य, भाषाविज्ञान तथा डॉ. कन्हैया सिंह जी के सम्पूर्ण रचना-संसार को एक साथ समझने में अत्यन्त सहायक सिद्ध होती है।
Meera Aur Meera
- Author Name:
Mahadevi Verma
- Book Type:

-
Description:
‘मीरा और मीरा’ छायावाद की मूर्तिमान गरिमा महीयसी महादेवी वर्मा के चार व्याख्यानों का संग्रह है। महादेवी जी ने ये व्याख्यान जयपुर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की राजस्थान शाखा के निमंत्रण पर दिए थे।
इन चार व्याख्यानों के शीर्षक हैं–मीरा का युग, मीरा की साधना, मीरा के गीत और मीरा का विद्रोह। इनमें महादेवी ने मध्यकालीन स्त्री की स्थिति का विशेष सन्दर्भ लेकर भक्ति, मुक्ति, आत्मनिर्णय, विद्रोह और निजपथ-निर्माण आदि को विश्लेषित किया है।
‘मीरा और मीरा’ को प्रकाशित करते हुए हमें इसलिए भी विशेष प्रसन्नता है कि यह समय अस्मिता-विमर्श का है। स्त्री-विमर्श के ‘समय विशेष’ में स्त्री-अस्मिता के दो शिखर व्यक्तित्वों का ‘रचनात्मक संवाद’ महत्त्वपूर्ण है। इन दो दीपशिखाओं के आलोक में परम्परा और आधुनिकता के जाने कितने निहितार्थ स्पष्ट होते हैं। ‘शृंखला की कड़ियाँ’ की लेखिका ने ‘सूली ऊपर सेज पिया की’ का गायन करने वाली रचनाकार के मन में प्रवेश किया है। यह दो समयों (मध्यकाल और आधुनिक युग) का संवाद भी है।
यह सोने पर सुहागा ही कहा जाएगा कि प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका सुप्रसिद्ध कवि, कथाकार व विमर्शकार अनामिका ने लिखी है। कहना न होगा कि यह लम्बी भूमिका एक मुकम्मल आलोचनात्मक आलेख है।
Mitti Ki Oar
- Author Name:
Ramdhari Singh Dinkar
- Book Type:

- Description: v data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main"><p>प्रस्तुत निबन्ध-संग्रह में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ के चौदह आलोचनात्मक निबन्ध संगृहीत हैं जो वर्तमान हिन्दी साहित्य के विषय पर लिखे गए हैं।</p> <p>राष्ट्रकवि ने इस निबन्ध-संग्रह में ‘इतिहास के दृष्टिकोण से’, ‘दृश्य और अदृश्य का सेतु कला में सोद्देश्यता का प्रश्न’, ‘हिन्दी कविता पर अशक्तता का दोष’, ‘वर्तमान कविता की प्रेरक शक्तियाँ’, ‘समकालीन सत्य से कविता का वियोग’, ‘हिन्दी कविता और छन्द’, ‘प्रगतिवाद’, ‘समकालीनता की व्याख्या’, ‘काव्य समीक्षा का दिशा-निर्देश’, ‘साहित्य और राजनीति’, ‘खड़ी बोली का प्रतिनिधि कवि’, ‘बलिशाला ही हो मधुशाला’, ‘कवि श्री सियारामशरण गुप्त’, ‘तुम घर कब आओगे कवि’ इत्यादि विचारोत्तेजक निबन्ध संगृहीत हैं।</p> <p>आशा है नए कलेवर में यह संग्रह पाठकों को अवश्य पसन्द आएगा।</p>
Hindi Upanyas Aur Astitvavad
- Author Name:
Veenu Bhalla
- Book Type:

-
Description:
अस्तित्ववादी चिंतकों ने बताया कि हमारे प्रत्येक सत्य और प्रत्येक कर्म में मानवीय संदर्भ और मानवीय आत्मपरकता निहित होती है तथा राज्यसत्ता, नौकरशाही, राजनीतिक दल—सभी निर्वैयक्तिक शक्तियाँ इस मानवीय आत्मपरकता को प्रतिबंधित करती रहती हैं।
अस्तित्ववाद ने इस बात पर बल दिया कि यथार्थ और अयथार्थ, आवश्यक और अनावश्यक के अंतर को समझने के लिए व्यक्ति और उसकी आत्मपरकता को प्राथमिकता देने से ही उसके चारों ओर फैली विसंगतियों को कम किया जा सकता है।
स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासों को आलोचकों ने कुंठा, घुटन और अनगढ़ प्रतीक योजनाओं के कारण अस्तित्ववादी उपन्यास की संज्ञा से अभिहित किया है। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में इस विषय से संबंधित जो शोध हुए हैं उनमें परीक्षण और जाँच कम, स्थापनाएँ अधिक हुई हैं। अस्तित्ववाद के प्रभाव को मानकर चलनेवाले लोगों ने संभवतः इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि हिंदी साहित्य की विधाओं में जो सिचुएशंस दिखाई पड़ती हैं वह अस्तित्ववाद के प्रभाव के कारण हैं अथवा बदलते हुए परिवेश के कारण।
यह पुस्तक अस्तित्ववादी विचारधारा की मूलचेतना 'अस्तित्व' की महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तियों के सैद्धांतिक विवेचन की अपेक्षा उसकी सिचुएंशस (स्थितियों) के आधार पर कुछ महत्त्वपूर्ण हिंदी उपन्यासों की विवेचना का प्रयास है।
Customer Reviews
Be the first to write a review...
0 out of 5
Book