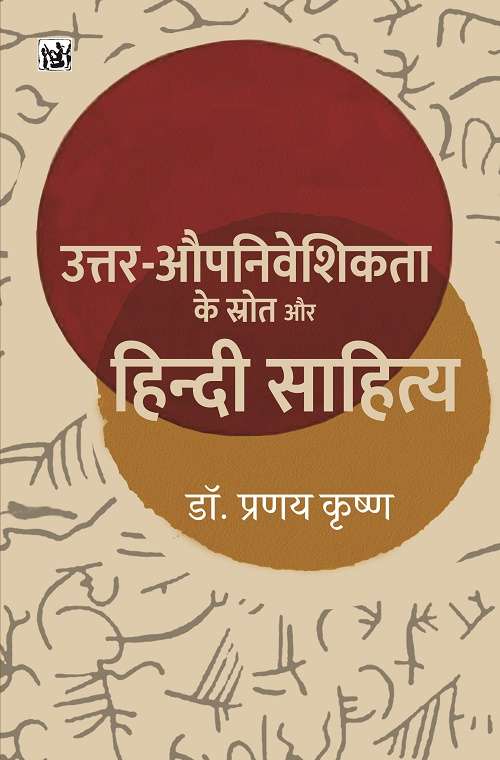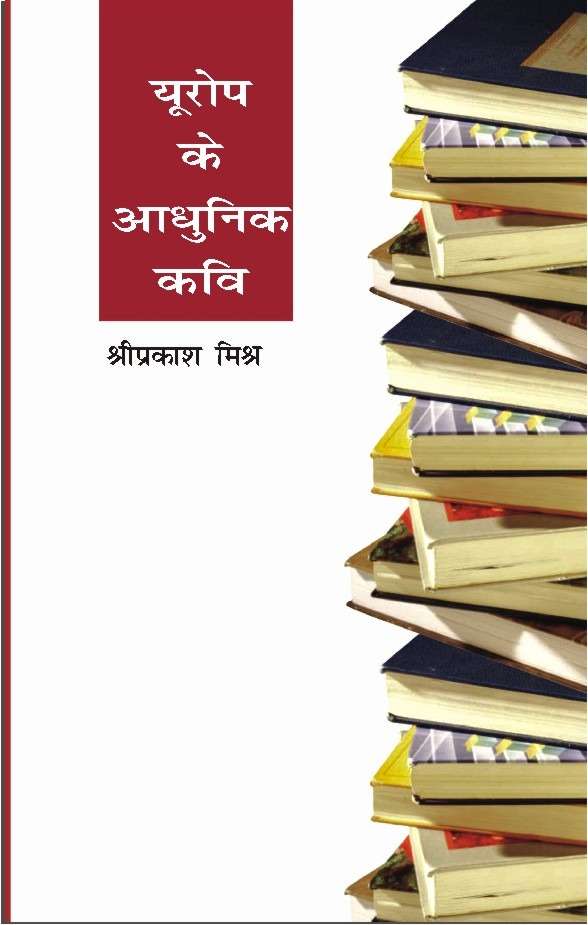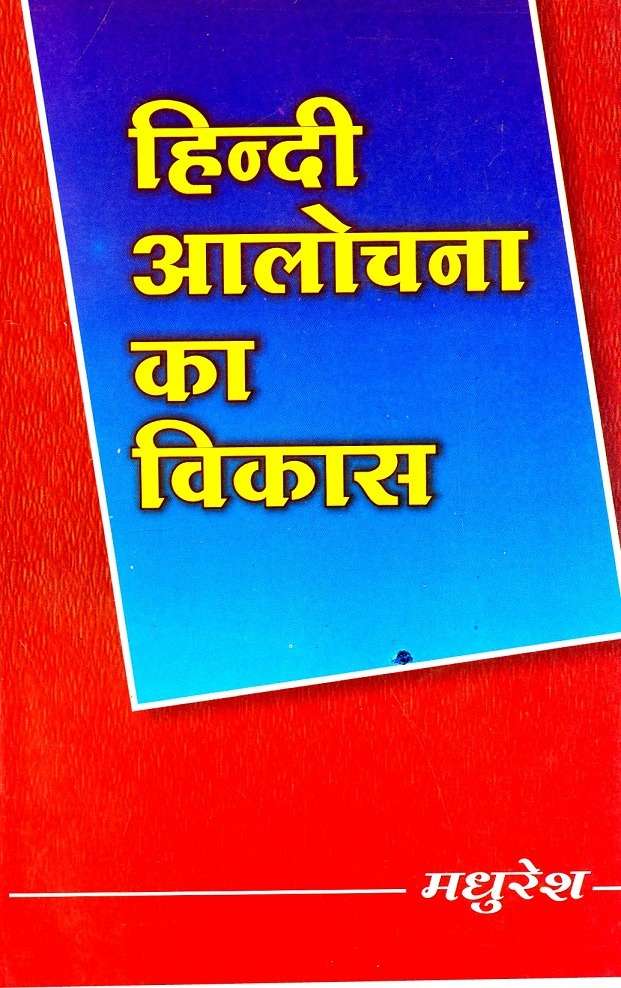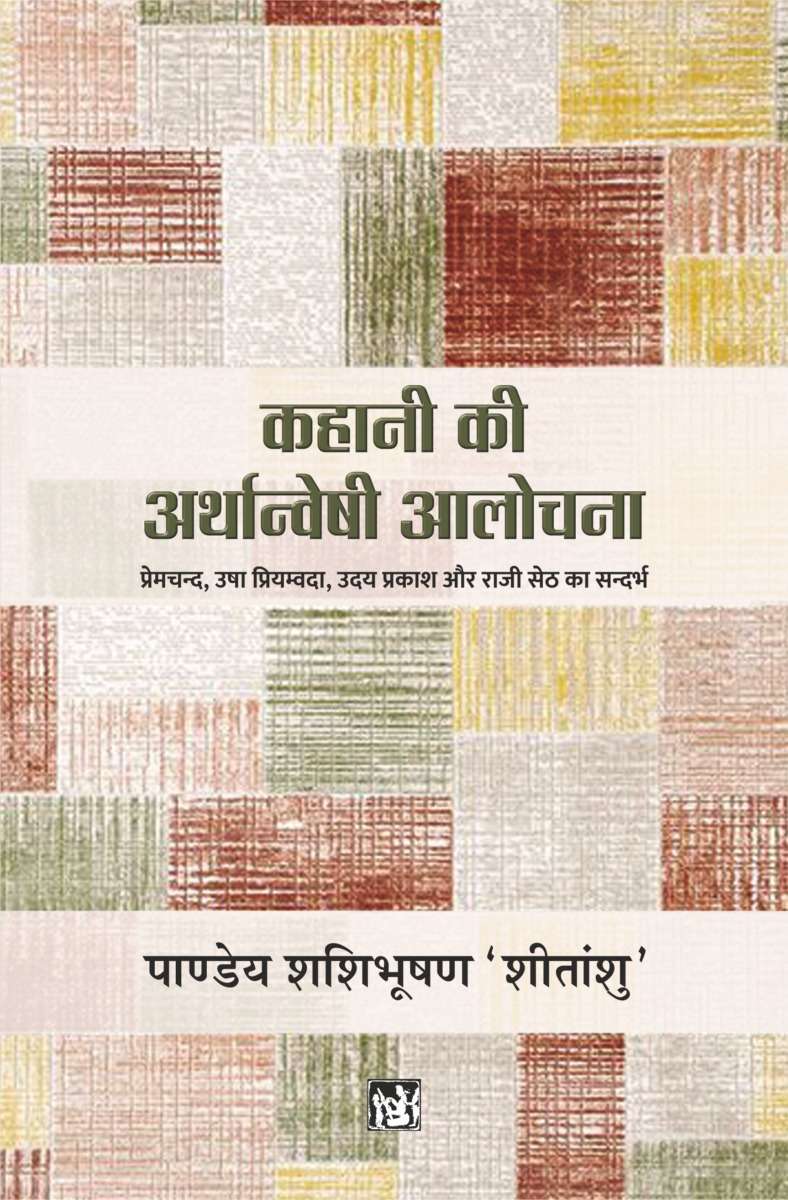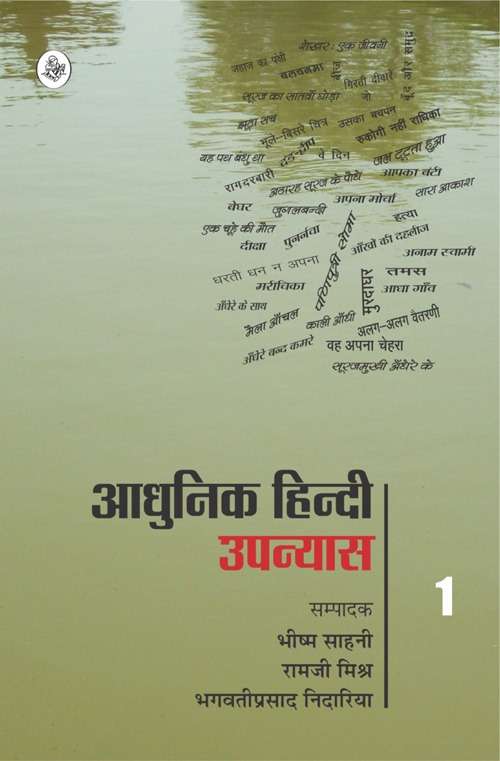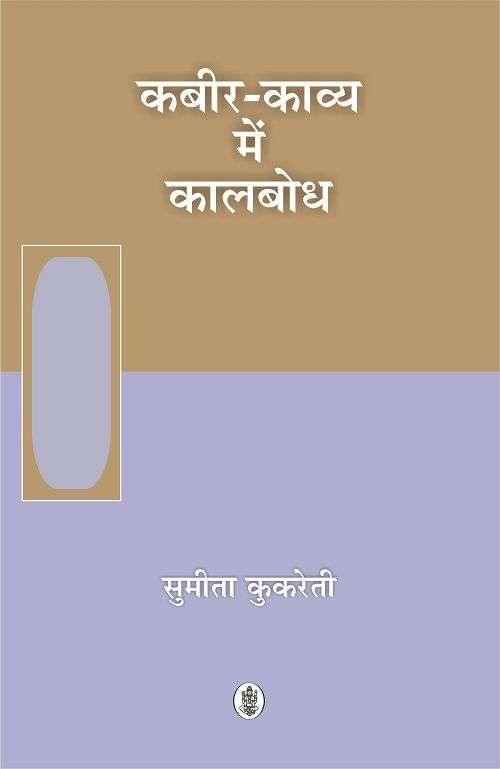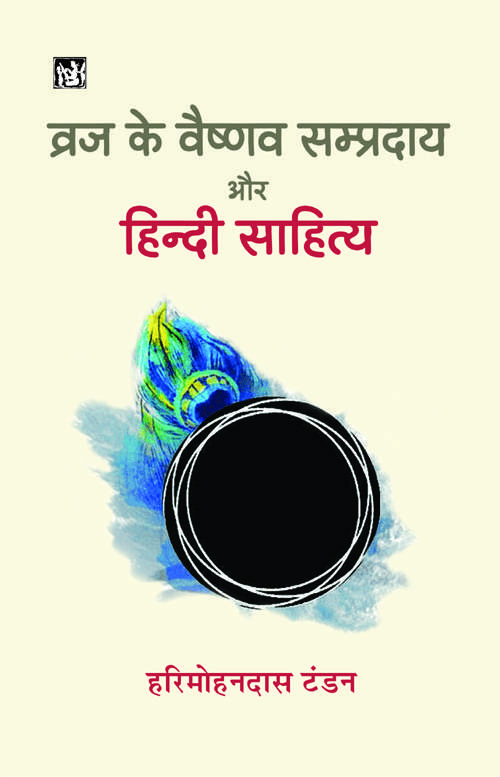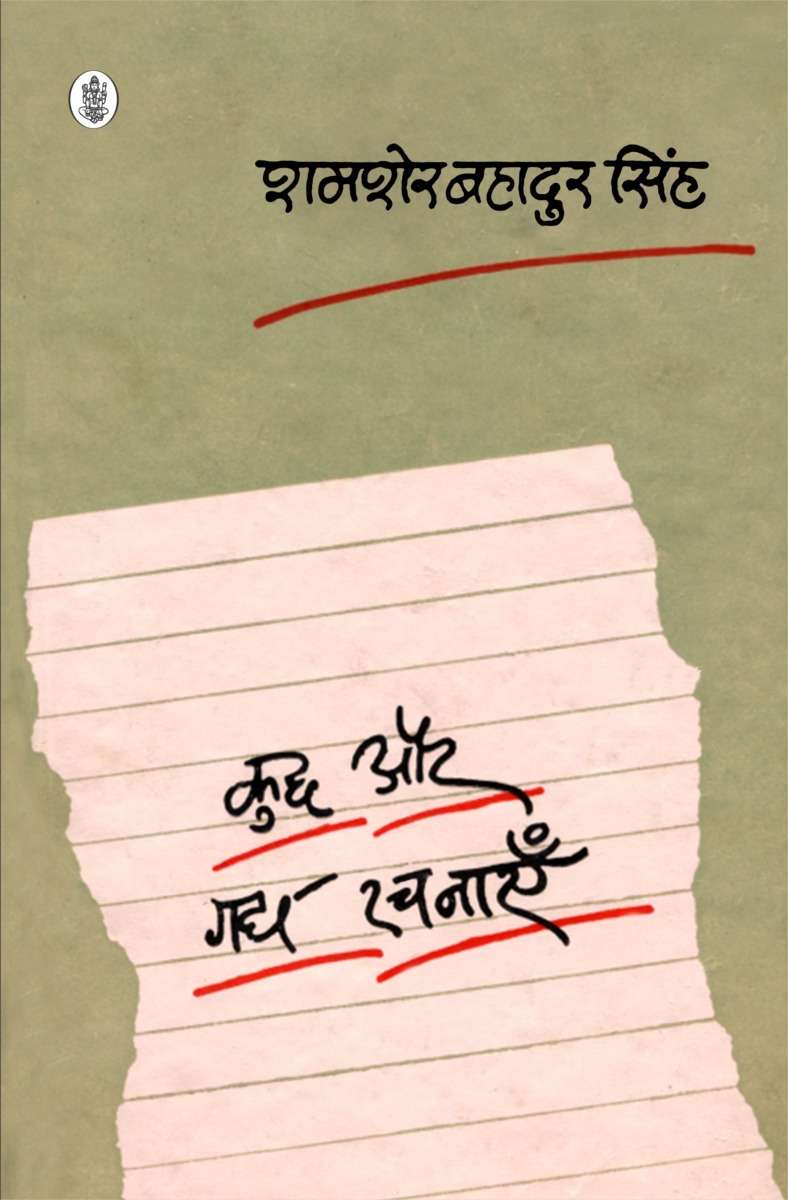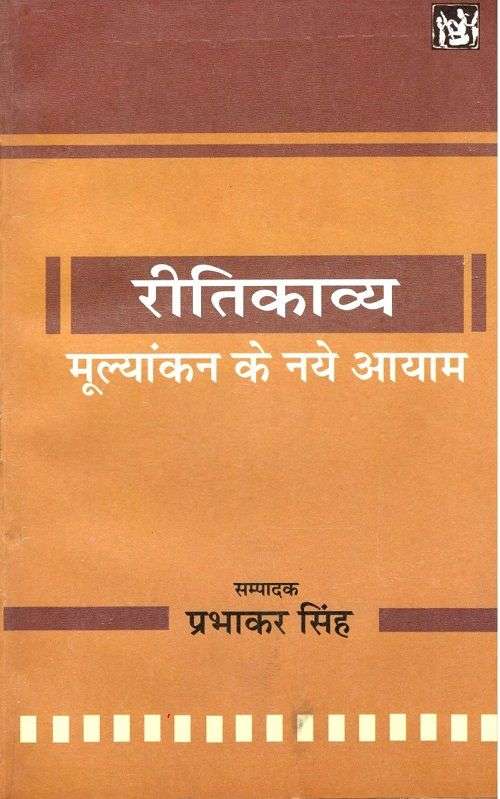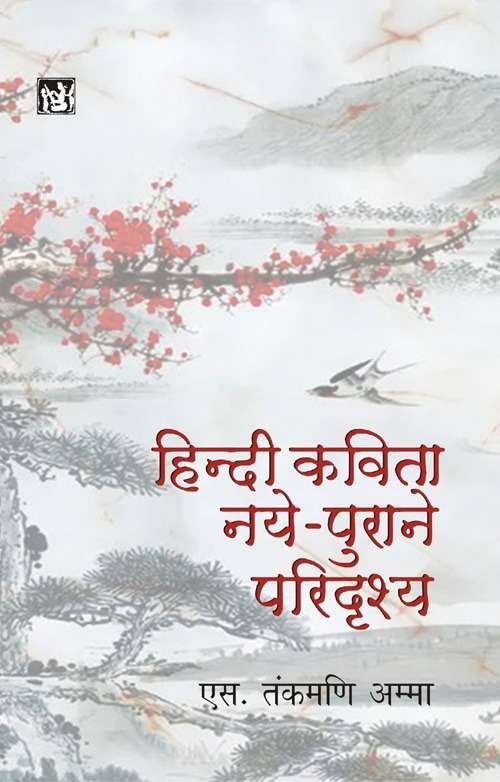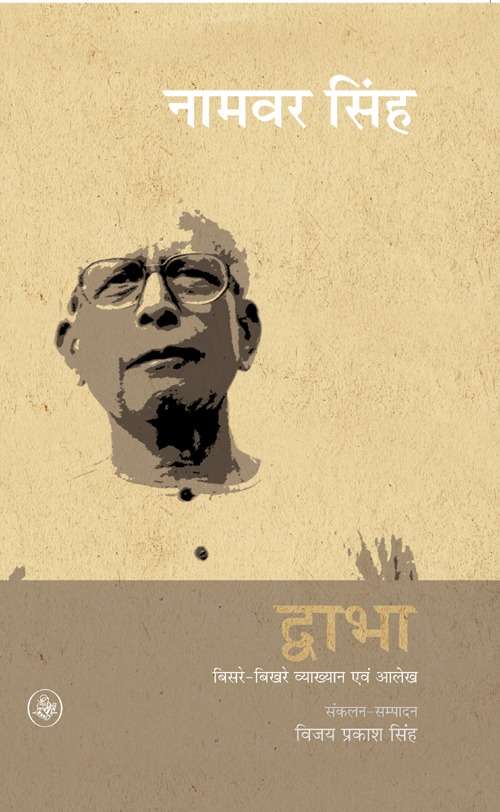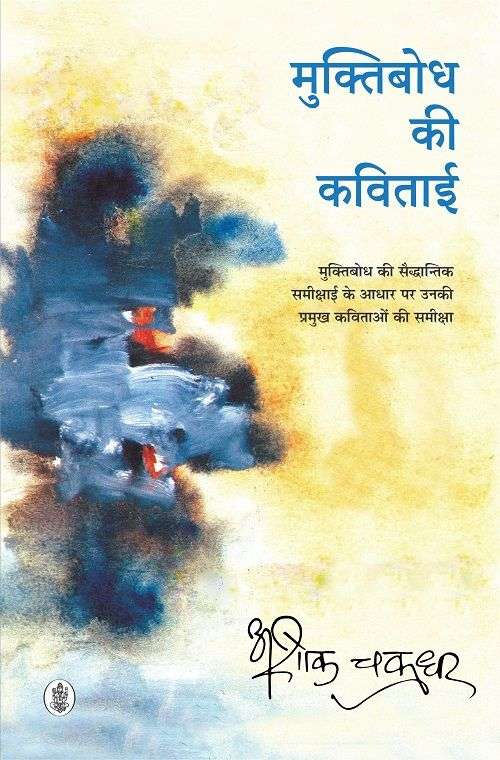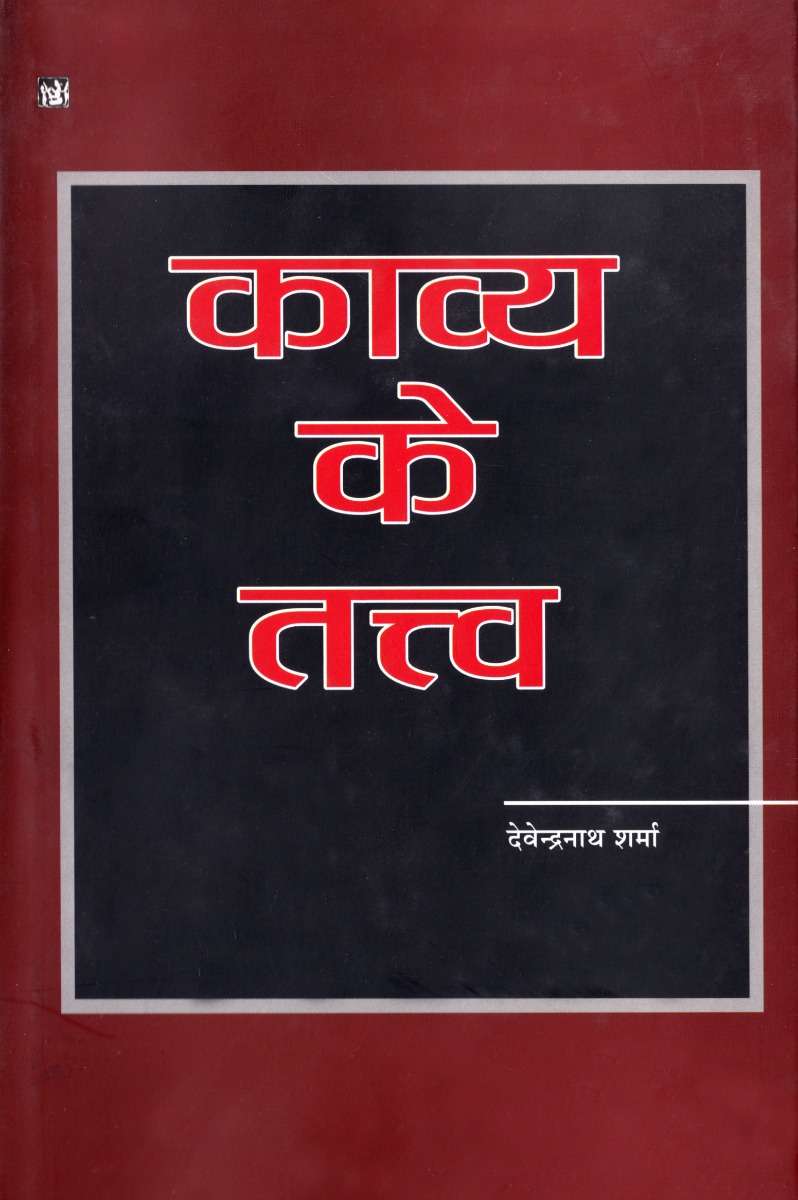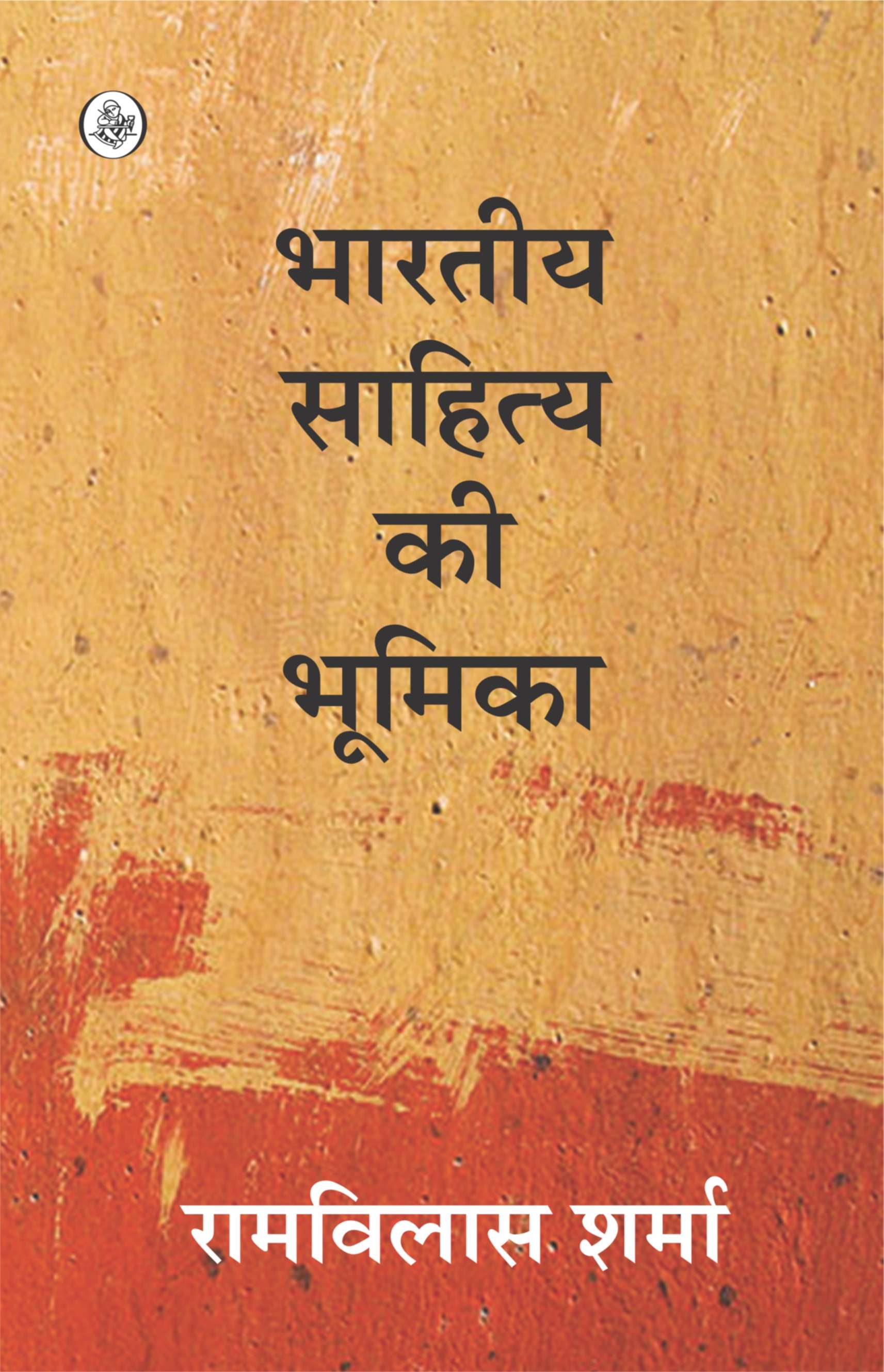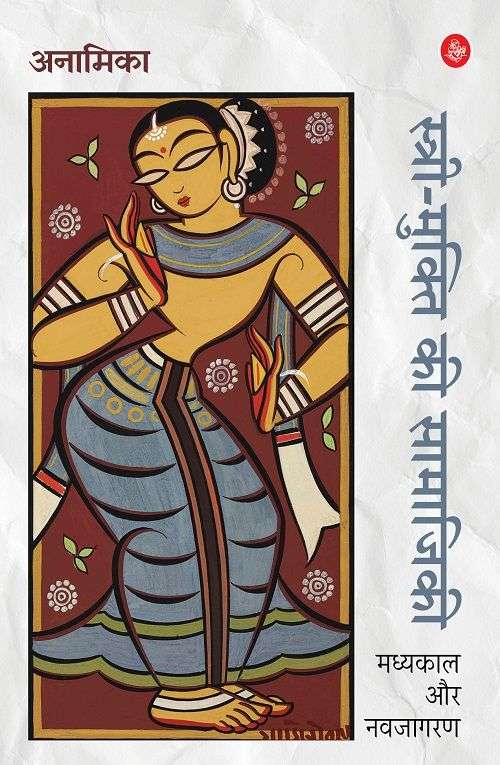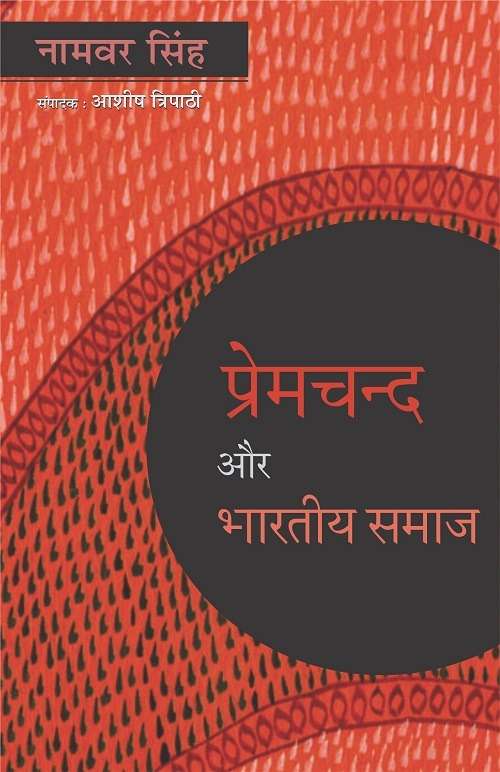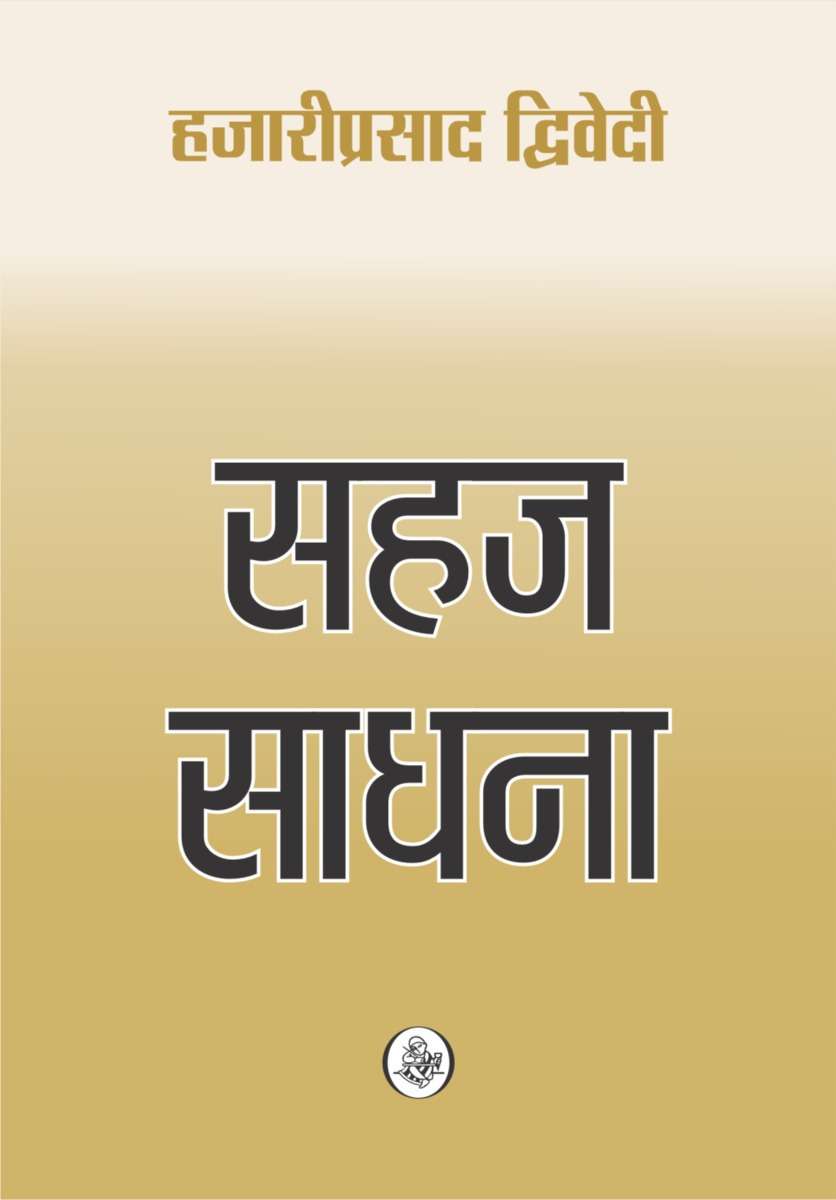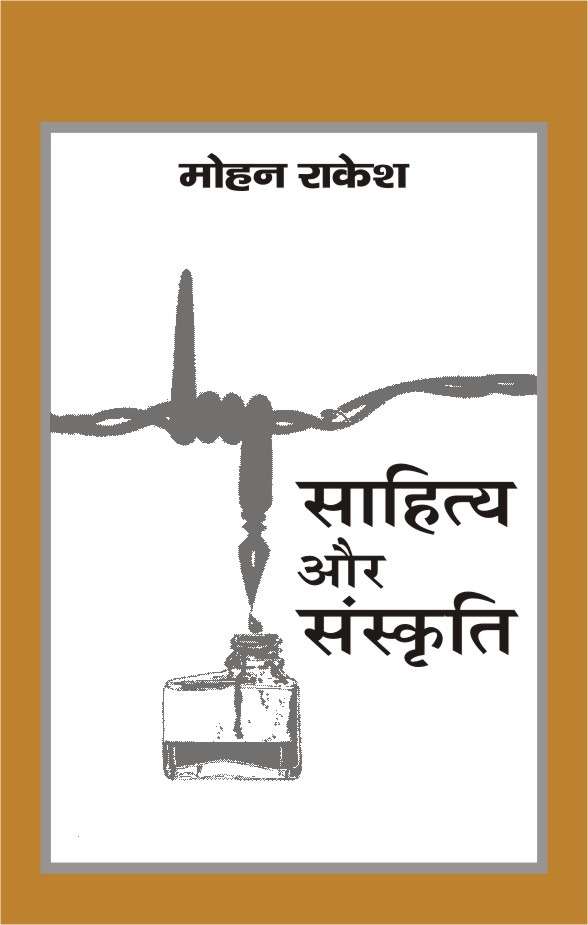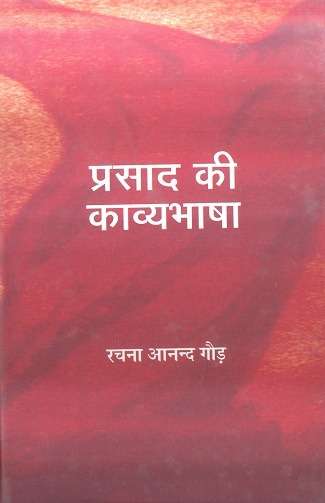
Prasad Ki Kavyabhasha
Author:
Rachna Anand GaurPublisher:
Rajkamal Prakashan SamuhLanguage:
HindiCategory:
Language-linguistics0 Ratings
Price: ₹ 200
₹
250
Unavailable
‘प्रसाद की काव्यभाषा' शीर्षक से प्रकाशित इस पुस्तक में जहाँ एक ओर प्रसाद की काव्यभाषा का विकासात्मक और प्रतीतिपरक मूल्यात्मक विवेचन किया गया है, वहीं दूसरी ओर संवेदना या जनता की चित्तवृत्ति में होनेवाले परिवर्तनों के कारण खड़ीबोली के काव्यभाषा के रूप में विकास का भी अत्यन्त व्यवस्थित वर्णन है। इस दृष्टि से यह पुस्तक दोहरी अर्थवत्ता रखती है।...</p>
<p>प्रसाद की प्रारम्भिक कृतियों से अनेक उदाहरणों द्वारा डॉ. गौड़ ने यह सिद्ध किया है कि कैसे अन्तत: एक बड़े कवि की खोज भाषा की ही खोज होती है।</p>
<p>मेरा मानना है कि इस पुस्तक के द्वारा केवल छायावाद और प्रसाद की काव्यभाषा की क्षमता को ही नहीं समझा जा सकता है, बल्कि खड़ीबोली की सम्भावना को भी रेखांकित किया जा सकता है।...पुस्तक पठनीय और संग्रहणीय है।</p>
<p>— सत्यप्रकाश मिश्र
ISBN: 9788180311147
Pages: 199
Avg Reading Time: 7 hrs
Age: 18+
Country of Origin: India
Recommended For You
Uttar Aupniveshikata Ke Srot Aur Hindi Sahitya
- Author Name:
Pranay Krishna
- Book Type:

-
Description:
उपनिवेशवादी विमर्शों को चुनौती अनेक विचारधाराओं, ज्ञानमीमांसाओं से मिलती रही है, लेकिन सर्वाधिक चुनौती उन वास्तविक उपनिवेशवाद- विरोधी जनसंघर्षों से मिली है, जिनके बगैर कोई भी विमर्श संभव नहीं था। ऐसे में उत्तर-औपनिवेशिकता कोई एक व्यवस्थित सिद्धांत या अनुशासन नहीं है। तेज़ी से बदलती दुनिया में विभिन्न किस्म के विचारों और व्यवहारों के बीच, विभिन्न किस्म की संस्कृतियों और लोगों के बीच बदलते रिश्तों के सन्दर्भ में ही उत्तर-औपनिवेशिक विमर्शों ने आकार ग्रहण किया है। मार्क्सवाद से लेकर नारीवाद तक के राजनीतिक सिद्धांत, उत्तर-संरचनावाद और उत्तर-आधुनिकता के साथ मार्क्सवादी ज्ञानमीमांसा का संघर्ष, संस्कृतिवादियों और भौतिकवादियों के बीच विवाद, पाठकेन्द्रित और यथार्थवादी साहित्य सिद्धान्तों की आपसी बहस उत्तर- औपनिवेशिक विमर्शों में संचरित है। ‘औपनिवेशिक’ का रेखांकन, विश्लेषण और सैद्धांतीकरण अनेक सन्दर्भों और विविध विमर्शों के परिक्षेत्र में होता रहा है। ‘उत्तर-औपनिवेशिक’ सैद्धांतिकी जितनी अधिक योरोपीय भाषाओं और सांस्कृतिक रूपों से बाहर निकलकर अन्य सांस्कृतिक अनुभवों को समेटने की कोशिश करती है, उतनी ही अधिक समस्याग्रस्त होती चली जाती है। भारतीय भाषाओं के साहित्य पर काम करने वाले आलोचकों ने ‘उत्तर-औपनिवेशिक’ सैद्धांतिकी की तमाम कठिनाइयों की ओर इंगित किया है।
विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने औपनिवेशिक परिस्थिति और अनुभव के प्रति जिस आलोचनात्मक दृष्टिपात को संभव किया, वह एक वैश्विक परिघटना उत्तर-औपनिवेशिक आलोचना सिद्धांत ने संस्कृति और राजनीति के पुराने कलावादी द्वैत का तो अन्त कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसके कुछ महत्त्वपूर्ण आलोचकों ने राजनीति को ही कला या पाठ में बदल दिया है।
उत्तर-औपनिवेशिक सांस्कृतिक विश्लेषण ने एक ऐसे लेखन को जन्म दिया है जो कि पश्चिमी और गैर-पश्चिमी लोगों और दुनियाओं को देखने के अब तक के वर्चस्वशाली नज़रिए को चुनौती देता है। वह एक ऐसे सैद्धांतिक ढाँचे को खड़ा करने का प्रयास है जो कि पश्चिमी, यूरो-केन्द्रिक ढाँचे का विकल्प बन सकें।
Europe Ke Adhunik Kavi
- Author Name:
Shriprakash Mishra
- Book Type:

-
Description:
हिन्दी के तमाम पाठक यूरोप की कविता और कवियों को इक्का-दुक्का तथा अपर्याप्त अनुवादों से जानते हैं। इससे वहाँ के कवियों के बारे में उनकी जानकारी आधी-अधूरी ही रहती है। श्रीप्रकाश मिश्र ने करीब साठ कवियों पर अलग-अलग लगभग पूरी जानकारी इस पुस्तक में समाहित की है, जिससे इस कमी की काफ़ी पूर्ति हो सकेगी। उन्होंने एक भाषा के कवियों को उनके कालक्रम के अनुसार एक साथ रखा है और उस सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि की भी जानकारी दी है जिसमें उनकी कविताओं ने जन्म लिया है। यूरोप की आधुनिकतावादी कविताओं की सामान्य विशेषताओं और स्वयं आधुनिकतावाद पर स्वतंत्र अध्याय उस कविता सम्बन्धी जानकारी को और समृद्ध करते हैं। वे स्वयं कवि हैं और
कवि पर उनकी एक निजी दृष्टि है—इसका भी प्रमाण इस पुस्तक में मिलता है। उम्मीद है, यूरोप की कविता के तमाम पाठकों को यह पुस्तक बड़ी उपादेय होगी।
Hindi Aalochana Ka Vikas
- Author Name:
Madhuresh
- Book Type:

-
Description:
मधुरेश की प्रस्तुत पुस्तक ‘हिन्दी आलोचना का विकास’ सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही आलोचना की मुख्य प्रवृत्तियों और आलोचकों के मूल्यांकन का प्रयास करती है। हिन्दी आलोचना में लोगों के अपने कुछ प्रिय आलोचक और युग रहे हैं।
मधुरेश वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय रूप में समूची हिन्दी आलोचना और आलोचकों का मूल्यांकन करते हैं। न उनका कोई प्रिय युग है, न ही आलोचक। वे सदैव सामाजिक विकास के सन्दर्भ में आलोचना को देखते-परखते हैं और कैसी भी चयनवादी दृष्टि से बचते हैं। हिन्दी में मार्क्सवादी और समकालीन आलोचना पर कदाचित् पहली बार यहाँ इतने सम्पूर्ण रूप में विचार हुआ है।
प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी आलोचना और आलोचकों के लिए अनिवार्य और उपयोगी है।
Kahani Ki Arthanveshi Alochana
- Author Name:
Pandeya Shashibhushan 'Shitanshu'
- Book Type:

-
Description:
हिन्दी कथालोचना के लगभग सौ वर्षों के इतिहास में यह आलोचनाकृति एक अन्यतम शिखर उपलब्धि है। यह सुपरिचित कहानियों की दुनिया के अब तक कराए गए प्रत्यक्ष से सर्वथा विलग उसकी अन्दरूनी छिपी दुनिया को पहली बार ‘रिवील’ करती है।
इस कृति से कहानी की आलोचना की एक समीचीन नयी सरणि आविष्कृत और प्रतिष्ठित हुई है।
इस पुस्तक में पहली बार ‘कफन’ में आधुनिकता बनाम उत्तर-आधुनिकता, कर्म-संस्कृति बनाम उपभोक्ता-संस्कृति, ‘पूस की रात’ में प्रकृति बनाम संस्कृति और ‘वर्ग-चेतना’, की विमुखता बनाम सजगता, ‘मंत्र-2’ में बाहरी बनाम आन्तरिक सर्प, ‘ईदगाह’ में मूर्त बनाम अमूर्त ईदगाह, ‘वापसी’ में कालपरक बनाम स्थलपरक, विधेयात्मक बनाम निषेधात्मक वापसी, ‘वारेन हेस्टिंग्स का साँड’ में पशु साँड बनाम हेस्टिंग्स रूपी साँड, ‘और अन्त में प्रार्थना’ में हैजा का संक्रमण बनाम भ्रष्टाचार का संक्रमण, ‘रुको इंतज़ार हुसैन’ में इंतजार हुसैन बनाम जवाहरलाल तथा ‘कब तक’ में परिवार से देश तक में यथास्थितीकरण से मुक्ति की छटपटाहट का यहाँ पहली बार सर्जनात्मक उद्घाटन किया गया है।
इन सबको जानने, समझने हेतु सभी पाठकों के लिए यह कृति पठनीय, विचारणीय और संग्रहणीय है।
Aadhunik Hindi Upanyaas : Vol. 1
- Author Name:
Bhisham Sahni
- Book Type:

-
Description:
प्रेमचन्द ने पहली बार इस सत्य को पहचाना कि उपन्यास सोद्देश्य होने चाहिए अर्थात् उपन्यास या कोई भी साहित्यिक विधा मनोरंजन के लिए नहीं होती वरन् वह मानव-जीवन को शक्ति और सुन्दरता प्रदान करनेवाली सोद्देश्य रचना होती है।
प्रेमचन्द में यथार्थ के जिन दो आयामों (सामाजिक और मनोवैज्ञानिक) का उद्घाटन हुआ, वे प्रेमचन्द के बाद अलग-अलग धाराओं में बँटकर तथा अपनी-अपनी धारा की अन्य अनेक सूक्ष्म बातों में संश्लिष्ट होकर बहुत तीव्र और विशिष्ट रूप में विकसित होते गए। एक ओर मनोविज्ञान की धारा बही, दूसरी ओर समाजवाद की।
प्रेमचन्दोत्तर सामाजिक उपन्यासों में मार्क्सवाद का स्वर प्रधान न भी रहा हो, किन्तु उसका प्रभाव निश्चय ही अन्तर्निहित रहा है। उसके प्रभाव के कारण ही निर्मम भाव से सामाजिक विसंगतियों को उद्घाटित किया गया। आंचलिक उपन्यासों की भी जन-चेतना उन्हें प्रेमचन्द से जोड़ती है, किन्तु अपने स्वरूप और दृष्टि में ये बहुत भिन्न हैं। इन्हें उपन्यास की एक नई विधा के रूप में ही स्वीकारना चाहिए।
यह आकस्मिक नहीं है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उपन्यास तो बहुत सारे लिखे गए किन्तु उपलब्धि के शिखरों को वे ही छू सके जो सामाजिक जीवन के अनुभवों के प्रति समर्पित रहे, जिनकी दृष्टि की आधुनिकता एक मुद्रा या तेवर की तरह टँगी नहीं रही, बल्कि सघन जीवन-यथार्थ के अनुभवों के बीच एक रचनात्मक शक्ति बनकर व्याप्त रही।
'आधुनिक हिन्दी उपन्यास' के सफ़र पर केन्द्रित यह पुस्तक 'गोदान' से लेकर आठवें दशक तक के महत्त्वपूर्ण उपन्यासों तक आती है। उल्लेखनीय है कि चालीस से अधिक जो उपन्यास इस चर्चा के केन्द्र में हैं; उनमें से अधिकांश हिन्दी के 'क्लासिक्स' के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यह पुस्तक केवल समीक्षा-संकलन नहीं है; सन्दर्भित उपन्यासों के रचनाकारों के आत्मकथ्य इसे एक रचनात्मक आयाम भी देते हैं जिनसे हमें इन उपन्यासों की रचना-प्रक्रिया का पता चलता है।
Kabir-Kavya Main Kaalbodh
- Author Name:
Sumita Kukreti
- Book Type:

-
Description:
कबीर का कालविषयक चिन्तन अद्वितीय है। कबीर ने काल के सन्दर्भ को साधारण मनुष्यों से लेकर सुलतानों अर्थात् सत्ता-प्रतिष्ठानों तक कुशलता से जोड़े और यह दिखाया कि सज्जनों को काल त्रस्त नहीं करता, वे कालभय से मुक्त जीवन व्यतीत करते हैं लेकिन अन्यायी और अत्याचारी हमेशा कालभय से गहरे सन्त्रस्त रहते हैं। इस पुस्तक में सुमीता कुकरेती ने यह रेखांकित किया है कि कबीर जैसे कालजयी कवि ने जनमानस को पहचान कर काल का रचनात्मक विश्लेषण किया। कबीर के लिए मृत्यु मानव-जीवन का ऐसा शाश्वत सत्य है जिसके माध्यम से उन्होंने जीवन की महत्ता का प्रतिपादन किया। कबीर का मुख्य उद्देश्य तदयुगीन मानवीय मूल्यों के क्षरण, सामाजिक विषमताओं और अपसंस्कृतियों के बरक्स सही जीवन जीने में विश्वास, समता और न्याय को रखना था। इसीलिए कबीर करुणा का अचूक इस्तेमाल करते हैं और कहीं-कहीं तीखी फटकार लगाते हैं। वह शोषक और अन्यायी वर्ग को उनके जीवन की क्षणभंगुरता समझाकर डराते भी हैं और मानवीय जीवन को उचित तरीके से जीने की राह भी दिखाते हैं।
‘कबीर-काव्य में कालबोध’ पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें अध्ययन-क्षेत्र को केवल युग-विशेष तक सीमित नहीं रखा गया है बल्कि कबीर के समकालीन कवियों के अतिरिक्त देशी-विदेशी आधुनिक कवियों और आलोचकों की दृष्टियों का गहरा अध्ययन और उनका तार्किक प्रयोग भी किया गया है। यह इसका वह उल्लेखनीय पक्ष है जो इसे परम्परित शुष्क और प्रायः नकलची शोध-प्रबन्धों और कथित आलोचनात्मक ग्रन्थों से अलग करता है। कबीर की कविता की अनउद्घाटित खूबियों को उद्घाटित करने वाला यह मौलिक कार्य कबीर-काव्य के पैराडाइम को विस्तृत करता है और ऐसा निर्भ्रान्त विमर्श भी रचता है जिससे सार्थक बहस सम्भव होती है। यहाँ हम कबीर के माध्यम से पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकालीन कविता को समझने की विशिष्ट आलोचनात्मक सरणी से भी परिचित होते हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ‘कबीर-काव्य में कालबोध’ एक महान रचनाकार को समझने की नई साहित्यिक पहल है।
पाण्डित्यपूर्ण दार्शनिक विषय को पठनीय बनाते हुए सुमीता कुकरेती ने कबीर का विचार-सम्पन्न समाजशास्त्रीय विवेचन किया है। उन्होंने कबीर काव्य के वास्तविक स्वभाव को जिस गहरी विश्लेषण-दृष्टि के साथ उकेरा है उसमें विचारोत्तेजक बौद्धिक परामर्श मौजूद है। उनके वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष और मौलिक स्थापनाएँ विशेष अर्थ रखती हैं।
Vraj Ke Vaishnav Sampradaya Aur Hindi Sahitya
- Author Name:
Harimohandas Tandan
- Book Type:

-
Description:
प्रस्तुत पुस्तक में कृष्ण-भक्ति के इतिहास तथा सिद्धान्तों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। सम्यक् ज्ञान के बिना जिज्ञासु विषय अपूर्ण और अस्पष्ट ही रह जाता है। साम्प्रदायिक कृष्ण-भक्ति से अनुप्राणित होकर लिखे गए हिन्दी साहित्य का अनुशीलन उनके सिद्धान्तों को पृष्ठभूमि में करने से अनेक भ्रमों का निराकरण हो जाता है। इस निबन्ध में साहित्य पर उनके प्रभाव का विवेचन व्यष्टि नहीं, अपितु समष्टि रूप से किया गया है।
कृष्ण-भक्ति का प्रारम्भ सहस्राब्दियों पूर्व हुआ था। समयानुसार अनेक धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कारणों से उसका क्रमिक विकास होता गया। आन्दोलन के फलस्वरूप उसके प्रचलित रूप को देखकर अनेक विद्वान् उस पर विदेशी प्रभाव सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। जिन अनेक भारतीय साधनाओं के उपकरणों ने उसे पल्लवित किया है, उनका क्रमिक इतिहास इस प्रकरण का प्रमुख विषय है। अध्ययन की सामग्री यत्र-तत्र विकीर्ण मिलती है। उसका कहीं भी एकत्र उपयोग नहीं प्राप्त होता। यहाँ न केवल उसे शृंखलाबद्ध किया गया है, अपितु उसमें अनेक अस्पष्ट गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास भी है।
वल्लभ और गौडीय सम्प्रदायों के अतिरिक्त अन्य सम्प्रदायों का विस्तृत विवरण भी साहित्य के अध्येताओं के समक्ष रखा गया है। निम्बार्क सम्प्रदाय का विचार इस निबन्ध की सीमा से परे है, क्योंकि हिन्दी साहित्य के सृजन में उसका कोई प्रत्यक्ष योग नहीं रहा है। ब्रजभाषा साहित्य के निर्माण का प्रारम्भ वस्तुत: वल्लभाचार्य की प्रेरणा से हुआ है। इस प्रकरण का महत्त्व अनेक स्थलों पर नवीन सामग्रियों के समावेश से बढ़ गया है। कृष्ण-भक्ति के प्रमुख कवियों का इसमें नाम निर्देश मात्र है। साहित्यिक कृतियों की समीक्षा भी नहीं है। ग्रन्थ के लघु कलेवर में उसकी अपेक्षा भी नहीं है। इस ग्रन्थ को हम एक परिचयात्मक ग्रन्थ ही कह सकते हैं। हिन्दी साहित्य में ब्रजभाषा के योगदान का उल्लेख भी किया गया है। ‘ब्रज के वैष्णव सम्प्रदाय और हिन्दी साहित्य’ के अनुशीलन से जो ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, निश्चित ही पाठक उससे लाभान्वित होंगे।
Kuchh Aur Gadya Rachanayen
- Author Name:
Shamsher Bahadur Singh
- Book Type:

-
Description:
शमशेर जी के ये निबन्ध बरबस इस तथ्य को गहराई से रेखांकित करते हैं कि मात्र कविता में ही नहीं, बल्कि गद्य में भी वे लगातार अपने समकालीनों के कृतित्व से जुड़े रहे हैं। उसको पढ़ते हैं, उस पर सोचते हैं और लिखते भी हैं, बल्कि कहीं न कहीं इसे वे अपना आत्मीय फ़र्ज़ भी मानते रहे हैं। अपने बराबर के साथी अपने ज्येष्ठ व कनिष्ठ समकालीनों पर दिल खोलकर इतना अधिक लिखनेवाले साहित्यकार बहुत कम हैं। ‘दोआब’ की ही तरह इस संग्रह में भी उन्होंने अपनी परम्परा के श्रेष्ठ कवियों पर भी लिखा है, जैसे ग़ालिब और रहीम।
यह एक बात ग़ौर करने की है, शमशेर जी के इन निबन्धों में लालित्य किस तरह छिपा है। एकाध निबन्धों को छोड़ प्रायः सभी निबन्धों में शमशेर जी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू नज़र आते हैं। इन निबन्धों के विषय ललित नहीं हैं, पर अपनी प्रस्तुति और प्रभाव में ये बहुत दूर तक ललित हैं। साहित्य से जुड़े अन्य विषयों पर भी शमशेर जी का चिन्तन इस संग्रह में शामिल निबन्धों में देखा जा सकता है। ये वे चिन्ताएँ हैं, जो शमशेर के अन्दरूनी कलाकार को मथती रहती हैं। चाहे वे ‘सामाजिक सत्य और रचना का माध्यम’ हो या ‘अमूर्त कला’ या फिर हल्का-फुल्का लगनेवाला ‘आशु कविता’ जैसा विषय। उनका जागरूक साहित्यकार भाषा और साहित्य पर एक नए दृष्टिकोण की माँग भी करता है।
Tevari Ka Saundaryabodh
- Author Name:
Rameshraaj
- Rating:
- Book Type:

- Description: तेवरी एक ऐसी विधा है जिसमें जन-सापेक्ष सत्योन्मुखी संवेदना अपने ओजस स्वरूप में प्रकट होती है। तेवरी का समस्त चिन्तन-मनन उस रागात्मकता की रक्षार्थ प्रयुक्त होता है, जो अपने सहज-सरल रूप में नैतिक, निष्छल, निष्कपट और प्राकृतिक है। रागात्मकता की यह प्राकृतिकता आपसी प्रेम, भाईचारे अर्थात् मानवीय सम्बन्धों की प्रगाढ़ता, सद्भाव के मंगलकारी विधान में अभिवृद्धित , अभिसंचित, पुष्पित-पल्लवित और उत्तरोत्तर विकसित होती है।
Ritikavya: Mulyankan Ke Naye Ayam
- Author Name:
PRABHAKAR SINGH
- Book Type:

- Description: रीतिकाव्य साहित्य और संवेदना का सौन्दर्यबोधीय और कलात्मक सृजन है। कोई भी जाति, सौन्दर्य और शृंगार से विलग होकर न तो जीवन के प्रति आकर्षण पैदा कर सकती है न विचारों में तेज। रीतिकाव्य मनुष्य की ऐहिकता को कला और सौन्दर्य के वैभव में सिरजने वाला काव्य है। हिन्दी- उर्दू कविता की साझा भाषायी संस्कृति भी इसी युग में प्रतिफलित हुई। साहित्येतिहास और आलोचना लेखन के विकास में 'रीतिकाव्य' को प्रायः उपेक्षित दृष्टि से ही आकलित किया गया। आलोचना और इतिहास लेखन के आरम्भिक दौर में 'रीतिकाव्य' को औपनिवेशिक विक्टोरियाई नैतिकता के चश्मे से ही देखा गया। द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रीतिविरोधी आलोचना का ऐसा अभियान चलाया कि हिन्दी के मूर्धन्य आलोचक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और रामविलास शर्मा जैसे प्रगतिशील आलोचक भी मूल्यांकन की इस विरोधी परम्परा को पोषित-पल्लवित करते नजर आते हैं। ये आलोचक रीतिकालीन कवियों के काव्य मर्म की तो प्रशंसा करते हैं लेकिन ऐतिहासिक मूल्यांकन करते समय रीतिकाव्य को दरबारी मानसिकता को पोषित करने वाला सामन्ती साहित्य कहकर उसे जनविरोधी कविता के खाँचे में डाल देते हैं। भारतीय चिन्तन परम्परा के वर्चस्ववादी और औपनिवेशिक नैतिकता के संश्लेष से निर्मित इस 'इतिहास दृष्टि' से उबरकर ही 'रीतिकाव्य' के साहित्य की सही पड़ताल की जा सकती है। यह पुस्तक रीतिकाव्य में विन्यस्त कला, सौन्दर्य और सृजन के वैभव को इतिहास की निरन्तरता में मूल्यांकित करने का प्रयास है। पुस्तक में रीतिकाव्य विषयक इतिहास, लेखन और आलोचना दृष्टि पर पुनर्विचार के साथ रीतिकाव्य के परिवेश, प्रवृत्ति और उसकी कविताई को साहित्य के नये विमर्शो और मूल्यों के साथ परखने की कोशिश है। पुस्तक में नामवर सिंह, मैनेजर पाण्डेय, नित्यानन्द तिवारी जैसे वरिष्ठ पीढ़ी के आलोचकों के साथ युवा पीढ़ी के आलोचकों में श्रीप्रकाश शुक्ल, कृष्णमोहन और आशीष त्रिपाठी के आलेख रीतिकाव्य को मूल्यांकित करने की नयी दृष्टि प्रदान करते हैं।
Hindi Kavita : Naye-Purane Paridrishya
- Author Name:
S. Tankmani Amma
- Book Type:

-
Description:
लोकगीतों से शुरू होकर आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के विभिन्न परिवेशों से गुज़रकर आधुनिक काल तक पहुँच गई हिन्दी कविता अपनी विकास-यात्रा की विविध मंज़िलों को तय करके सम्प्रति इक्सीसवीं शदी के दूसरे दशक के अन्तिम चरण तक पहुँच चुकी है। इस लम्बी विकास-यात्रा के दौरान हिन्दी कविता स्थल और काल के परिवेश के अनुकूल नूतन प्रवृत्तियों को आत्मसात् कर कई आन्दोलनों से होकर गुज़री है। प्रचलित प्रवृत्तियों से भिन्न प्रवृत्तियाँ जब काव्यक्षेत्र में घर कर लेती हैं तथा कविता उनके अनुकूल परिभाषित होती है तभी तो नए काव्यान्दोलनों का प्रादुर्भाव होता है। इन काव्यान्दोलनों ने समय-समय पर कविता की संवेदना और संरचना में परिवर्तन और परिवर्द्धन उपस्थित कर दिए हैं। सुखद आश्चर्य की ही बात है कि ‘कवि की मौत', 'कविता की मौत' जैसे वैश्विक नारों और चुनौतियों का सामना करते हुए, अपनी संजीवनी शक्ति के बल पर कविता अब भी सम्पूर्ण मानवराशि को तथा प्रकृति और पर्यावरण को बचाए रखने की कोशिश में लगी हुई है। विनष्ट होते अथवा क्षरित होते श्रेष्ठ मानव मूल्यों को बचाने की चिन्ता ही समकालीन विविध विमर्शों में मुखरित होती है। तभी मुक्तिबोध की ये पक्तियाँ सार्थक सिद्ध होती हैं–
"नहीं होती। कहीं भी ख़त्म कविता नहीं होती
कि वह आवेग त्वरित काल यात्री है...
हिन्दी कविता की यात्रा अभी जारी है–वर्तमान सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याओँ से जूझते हुए...मानव हित की चिन्ता करते हुए।
Dwabha
- Author Name:
Namvar Singh
- Book Type:

-
Description:
नामवर सिंह जीते-जी विशिष्ट शख़्सियत की देहरी लाँघकर एक लिविंग ‘लीजेंड' हो चुके थे। तमाम तरह के विवादों, आरोपों और विरोध के साथ असंख्य लोगों की प्रसंशा से लेकर ‘भक्ति-भाव तक को समान दूरी से स्वीकारने वाले नामवर जी ने पिछले दशकों में मंच से इतना बोला कि शोधकर्ता लगातार उनके व्याख्यानों को एकत्रित कर रहे हैं और पुस्तकों के रूप में पाठकों के सामने ला रहे हैं। यह पुस्तक भी इसी तरह का एक प्रयास है लेकिन इसे किसी शोधार्थी ने नहीं उनके पुत्र विजय प्रकाश ने संकलित किया है।
इस संकलन में मुख्यत: उनके व्याख्यान हैं और साथ ही विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लिखे-छपे उनके कुछ आलेख भी हैं। नामवर जी ने अपने जीवन-काल में कितने विषयों को अपने विचार और मनन विषय बनाया होगा, कहना मुश्किल है। अपने अपार और सतत अध्ययन तथा विस्मयकारी स्मृति के चलते साहित्य और समाज से लेकर दर्शन और राजनीति तक पर उन्होंने समान अधिकार से सोचा और बोला। इस पुस्तक में संकलित आलेख और व्याख्यान पुन: उनके सरोकारों की व्यापकता का प्रमाण देते हैं। इनमें हमें सांस्कृतिक बहुलतावाद, आधुनिकता, प्रगतिशील आन्दोलन, भारत की जातीय विविधता जैसे सामाजिक महत्त्व के विषयों के अलावा अनुवाद, कहानी का इतिहास, कविता और सौन्दर्यशास्त्र, पाठक और आलोचक के आपसी सम्बन्ध जैसे साहित्यिक विषयों पर भी आलेख और व्याख्यान पढ़ने को मिलेंगे।
पुस्तक में हिन्दी और उर्दू के लेखकों-रचनाकारों पर केन्द्रित आलेखों के लिए एक अलग खंड रखा गया है जिसमेँ पाठक मीरा, रहीम, संत तुकाराम, प्रेमचन्द, राहुल सांकृत्यायन, त्रिलोचन, हजारीप्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, परसाई, श्रीलाल शुक्ल, ग़ालिब और सज्जाद ज़हीर जैसे व्यक्तित्वों पर कहीं संस्मरण के रूप में तो कहीं उन पर आलोचकीय निगाह से लिखा हुआ गद्य पढ़ेंगे।
बानगी के रूप में देश की सांस्कृतिक विविधता पर मँडरा रहे संकट पर नामवर जी का कहना है : ‘संस्कृति एकवचन शब्द नहीं है, संस्कृतियाँ होती हैं...सभ्यताएँ दो-चार होंगी लेकिन संस्कृतियाँ सैकड़ों होती हैँ...सांस्कृतिक बहुलता का नष्ट होते हुए देखकर चिन्ता होती है और फिर विचार के लिए आवश्यक स्रोत ढूँढ़ने पड़ते हैं।’ यह पुस्तक ऐसे ही विचार-स्रोतों का पुंज है।
Muktibodh Ki Kavitaai
- Author Name:
Ashok Chakradhar
- Book Type:

-
Description:
मुक्तिबोध के कला-सिद्धान्त कविता को एक सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रिया मानते हैं, उनकी कविताई इसका जागता जीता प्रमाण है। उनकी कविताई में भ्रमों से परिपूर्ण युगीन यथार्थ का जीवन-जाल तो मिलता है, पर उसकी बुनावट में रचनागत अर्थ का कोई भ्रम नहीं है।
जो महानुभाव कविता को प्राय: एक कलात्मक या शिल्पात्मक प्रक्रिया समझते हैं, उनके लिए तो मुक्तिबोध की कविताएँ निश्चित रूप से ‘जटिल’, ‘अधूरी’, ‘आत्मपरक अभिव्यक्ति’, ‘भयानक’ या ‘ऊबड़-खाबड़’ हो सकती हैं, किन्तु यदि हम मुक्तिबोध की रचना-प्रक्रियापरक समझ से परिचित हो लें और उनके सूत्र—‘कला एक सामाजिक प्रक्रिया है’—को आधार मानकर उनकी रचनाओं में जाने की कोशिश करें, तो प्रत्यक्ष पाते हैं कि मुक्तिबोध शब्द के असामाजिक प्रयोग के कवि नहीं थे। हाँ, इतना तो है ही कि उनके कथ्य की सार्थकता तभी पकड़ में आ पाती है, जब हम कविता के बारे में उनके स्वयं के दृष्टिकोण से रूबरू हो लें। ऐसा अगर हम कर लें तो उस ग़लती से भी बचा जा सकता है जो मुक्तिबोध के सन्दर्भ में जाने या अनजाने होती आ रही है।
इस पुस्तक में मुक्तिबोध की सैद्धान्तिक समीक्षाई के आधार पर उनकी छोटी-बड़ी ग्यारह प्रमुख कविताओं की व्यावहारिक समीक्षा की गई है। साथ ही एक साफ़-सुथरा रास्ता बनाने की कोशिश है कि जिस रास्ते पर चलकर मुक्तिबोध की कविताई तक पहुँचा जा सकता है।
अशोक चक्रधर मुक्तिबोध की कविताओं पर कार्य करनेवाले प्रारम्भिक लेखकों में गिने जाते हैं। यही कारण कि उनकी यह पुस्तक आज भी पाठकों के बीच अपने कई कारणों से अत्यन्त उपयोगी बनी हुई है।
Kavya Ke Tattva
- Author Name:
Aacharya Devendranath Sharma
- Book Type:

- Description: प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य है भारतीय दृष्टि से काव्य के उपादानों का परिचय कराना। सुगमता और संक्षिप्तता इसकी विशेषताएँ हैं। उदाहरण विषय को स्पष्ट करने के साधन हैं। अत: उनकी सटीकता तथा उपयुक्तता को महत्त्व दिया गया है और उनके चयन में सावधानी बरती गई है। इस पुस्तक में दिए गए उदाहरण विषय के स्पष्टीकरण एवं स्मरण में निस्सन्देह सहायक सिद्ध होंगे।
Bharatiya Sahitya Ki Bhumika
- Author Name:
Ramvilas Sharma
- Book Type:

-
Description:
यह पुस्तक भारतीय साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नहीं है। यहाँ भारतीय साहित्य और उसकी सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कुछ पक्षों पर विचार किया गया है। प्रयत्न यह है कि देशी रूढ़िवादियों और पश्चिमी संसार के ‘वैज्ञानिक’ विचारकों से अलग हटकर ऐसा रास्ता बनाया जाए जिस पर चलते हुए भारतीय साहित्य के और बहुत से पक्षों का वस्तुगत विवेचन किया जा सके। यह पुस्तक रास्ते की शुरुआत है, उसकी आख़िरी मंज़िल नहीं।
‘ऋग्वेद में कवि और काव्यशिल्प’ से आरम्भ कर भारतीय नवजागरण तक की लम्बी यात्रा में लेखक ने भारतीय समाज व्यवस्था और संस्कृति के विविध पहलुओं पर विचार किया है।
इस पुस्तक का प्रमुख आकर्षण संगीत और अन्य कलाओं के सम्बन्ध पर किया गया विचार है।
डॉ. शर्मा के मतानुसार, ‘‘जिसे हिन्दुस्तानी संगीत कहते हैं, वह हिन्दी भाषी जनता का जातीय संगीत है। और हिन्दुस्तानी संगीत में मुसलमानों का योगदान महत्त्वपूर्ण था।’’सोलहवीं-सत्रहवीं सदियों में कलाओं के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में उनका कहना है कि इन ‘‘सदियों में जैसा भव्य सौन्दर्य स्थापत्य में देखा जा सकता है, वैसा ही उदात्त सौन्दर्य ध्रुवपद की गायकी में है।’’ तथा ‘‘संगीतशास्त्र का इतिहास सन्तों की संगीत साधना के बिना नहीं समझा जा सकता।’’ ऐसी बहुत सी स्थापनाएँ पाठकों को इस विषय पर नए ढंग से सोचने की प्रेरणा देंगी।
उनका कथन कि : ‘‘जिन परिस्थितियों में भारतीय साहित्य का निर्माण और अध्ययन हो रहा है, उनका गहरा सम्बन्ध विश्व पूँजीवाद से है,’’ एक विचारणीय तथ्य की ओर संकेत है। इसके साथ ही, दूसरे महायुद्ध के बाद पूँजी के ज़बर्दस्त केन्द्रीकरण से पैदा होनेवाली परिस्थितियों में वे ‘अपनी जातीय संस्कृति की रक्षा करना हर बुद्धिजीवी का कर्तव्य’ मानते हैं।
यह पुस्तक पाठकों को ‘बड़े पैमाने पर स्वदेशी आन्दोलन की आवश्यकता’ पर सोचने की प्रेरणा देती है।
Stree-Mukti Ki Samajiki : Madhyakal Aur Navjagaran
- Author Name:
Anamika
- Book Type:

-
Description:
आज भी स्त्रीवाद के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि वह मनुष्य मात्र में स्त्री-दृष्टि का विकास करे। यह सिर्फ़ स्त्रियों की अपनी मुक्ति का मसला नहीं है, पुरुष को भी उन जकड़बदियों से मुक्त होने की ज़रूरत है जो एक तरफ़ उसे शक्ति देती हैं कि वह किसी को बाँध सके तो दूसरी तरफ़, ख़ुद उसे भी एक चौखटे में जड़ देती हैं।
बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदलने-बदलने को है। संस्थाओं-प्रतिष्ठानों का पौरुष ढीला पड़ा है और स्त्री-तत्व के प्रवाह के लिए परिवार से लेकर राष्ट्र तक, सभी जगह नए झरोखों-रास्तों ने जन्म लिया है। ख़ासतौर से लेखन में स्त्री का स्वर निर्णायक भंगिमा और अपनी विशिष्ट पहचान के साथ उभरकर आया है। स्त्री ने निसंकोच भाव से अपनी एक भाषा गढ़ी है, आलोचना की अपनी प्रविधियाँ विकसित की हैं, उन विशेषताओं को जाना है जो उसे एक बेहतर मनुष्य बनाती हैं और यह भी समझा है कि उसका होना संसार के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन उसका सहगामी और अब तक वर्चस्व का केन्द्र रहा पुरुष भी क्या उतना ही बदला है? और क्या स्त्री का यह आत्मविश्वास अचानक हुई कोई घटना है या पीछे इतिहास में शुरू हुई किसी लम्बी प्रक्रिया का प्रतिफल?
‘स्त्री-मुक्ति की सामाजिकी : मध्यकाल और नवजागरण’ हिन्दी के मध्यकालीन काव्य तथा सामाजिक सौन्दर्यबोध के पुनर्पाठ के माध्यम से इसी प्रक्रिया का लेखा-जोखा करने की कोशिश करती है। मध्यकाल और पुनर्जागरण के दौर की रचनाओं, रचनाकारों और दूर भविष्य तक को प्रभावित करने वाली प्रवृत्तियों को रेखांकित करते हुए यह किताब स्त्री-विमर्श के उदात्त पक्षों का अन्वेषण और समय तथा समाज की सीमाओं का आकलन दोनों करती है।
मध्यकालीन नायिकाओं और स्त्री-रचनाकारों की विनोद-वृत्ति जो उनकी आन्तरिक मुक्ति की ही एक भंगिमा थी; रहीम की ‘नगर शोभा’ में स्त्रियों का चित्रण और उसकी सामाजिकी; स्त्री भक्त-कवियों का अस्मिताबोध और आधुनिक स्त्री-दृष्टि से रीतिकाल के पुनर्पाठ से लेकर मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में आई स्त्री तक, अनामिका ने इस पुस्तक में अपनी रस-सिद्ध आलोचना-शैली में एक पूरे युग का जायज़ा लिया है।
Premchand Aur Bhartiya Samaj
- Author Name:
Namvar Singh
- Book Type:

-
Description:
प्रेमचन्द स्वाधीनता-संग्राम में साधारण भारतीय जनता की जीवंतता, प्रतिरोधी शक्ति और आकांक्षाओं-स्वप्नों के अमर गायक। उपन्यास और कहानी जैसी, हिन्द में प्रायः लड़खड़ाकर चलना सीखती, विधाओं को ‘स्वाधीनता’ के इस महास्वप्न से जोड़कर रचनात्मक ऊँचाइयों के चरम पर ले जानेवाले परिकल्पक। रचनाशीलता को जनता के ठोस नित-प्रति भौतिक जीवन और उसके अवचेतन में मौजूद उसकी साधारण और असाधारण इच्छाओं को संयुक्त कर एक पूर्ण जीवन का आख्यान बनानेवाले युगदर्शी कथाकार। ‘यथार्थ’ की ठोस पहचान और ‘यथास्थिति’ के पीछे कार्य कर रही कारक शक्तियों की प्रायः एक वैज्ञानिक की तरह पहचान करनेवाले भविष्यदर्शी विचारक और बुद्धिजीवी।
सम्भवतः इन्हीं कारणों से आधुनिक रचनाकारों में इकलौते प्रेमचन्द ही हैं जिनमें हिन्दी के शीर्ष स्थानीय मार्क्सवादी आलोचक प्रो. नामवर सिंह की दिलचस्पी निरन्तर बनी रही। प्रेमचन्द पर विभिन्न अवसरों पर दिए गए व्याख्यान एवं उन पर लिखे गए आलेख इस पुस्तक में एक साथ प्रस्तुत हैं।
यहाँ शामिल निबन्धों एवं व्याख्यानों में प्रेमचन्द के सभी पक्षों पर विस्तार से बातचीत की गई है। प्रेमचन्द की वैचारिकता, जीवन-विवेक और उनकी रचनाओं के सम्बन्ध में प्रगतिशील आलोचना का स्पष्ट नज़रिया यहाँ अभिव्यक्त हुआ है। विशिष्ट सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रेमचन्द की कहानियों और उपन्यासों का विवेचन यहाँ है और भारतीय आख्यान परम्परा के सन्दर्भ में प्रेमचन्द के कथा-शिल्प की विशिष्टता और उसकी भारतीयता पर गम्भीर विचार भी। साम्प्रदायिकता, दलित प्रश्न जैसे विशिष्ट प्रसंगों के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचन्द की रचनात्मकता और उनके विचारों का मूल्यांकन हो या स्वाधीनता-संग्राम के सन्दर्भ में उनकी ‘पोजीशन’ का विवेचन—इन निबन्धों में नामवर जी अपनी निर्भ्रान्त वैचारिकता, आलोचकीय प्रतिभा और लोक-संवेदी तर्क-प्रवणता और स्पष्ट जनपक्षधरता से प्रेमचन्द को उनकी सम्पूर्णता में उपस्थित करते हैं।
Sahaj Sadhna
- Author Name:
Hazariprasad Dwivedi
- Book Type:

-
Description:
पिछले पाँच दशकों में शैक्षणिक-विकास की दिशा में काफ़ी कुछ घटित हुआ है। सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। जहाँ शिक्षा के प्रति हमारी सामाजिक रुचि में इज़ाफ़ा हुआ है, वहीं यह भी सत्य है कि शिक्षा और शिक्षण-पद्धतियों की गुणवत्ता में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आया है। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन निरक्षरों की संख्या में भी कोई कमी नहीं आई है। हमारे शिक्षा-तंत्र का ढाँचा आज भी शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक बालक को भविष्य का कोई नक़्शा और एक सुदृढ़ व्यक्तित्व की गारंटी देने में असमर्थ है। जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें उनकी अपनी और स्कूलों की सम्पन्नता-विपन्नता से वर्ग-भेद की खाई भी कम नहीं हो पा रही है और जो शिक्षा के क्षेत्र से बाहर हैं, उन्हें इस तरफ़ आकर्षित करने के लिए जिस लगन, कर्मठता और संवेदनशीलता की आवश्यकता है, वह भी कहीं देखने में नहीं आती—न सरकारी प्रयासों में और न व्यक्तिगत या संस्थागत स्तर पर। इस पुस्तक में समाहित आलेखों की प्रमुख चिन्ता यही है।
लेखकद्वय ने प्राथमिक शिक्षा को अपने चिन्तन का केन्द्रीय बिन्दु बनाते हुए शिक्षा के पूरे परिदृश्य को समझने और विश्लेषित करने का प्रयास किया है। इन आलेखों के सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि इनकी रचना शिक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक स्तर पर काम करते हुए हुई; विभिन्न शिक्षाविदों, शिक्षकों तथा दूसरे सहयोगियों के साथ काम करते हुए जो अनुभव और सबक़ हासिल हुए, लेखकद्वय ने उन्हीं को इन आलेखों में पिरोने की कोशिश की है।
Sahitya Aur Sanskriti
- Author Name:
Mohan Rakesh
- Book Type:

- Description: मोहन राकेश की प्रतिभा बहुमुखी थी। कहानी, उपन्यास, नाटक-एकांकी, ध्वनि नाटक, बीज नाटक और रंगमंच—इन सभी क्षेत्रों में मोहन राकेश का नाम सर्वोपरि है। इस संकलन में इन विधाओं के विभिन्न पहलुओं पर मोहन राकेश के छिटपुट लेखों को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिनसे उनकी दृष्टि को समझने में पर्याप्त सहायता मिलेगी। लेखों के अतिरिक्त इस संकलन में ‘नयी कहानी’ पर एक गोष्ठी, सोवियत नाटककार के साथ एक बातचीत, हेब्बार और रविशंकर के साथ भारतीयता और आधुनिकता के तत्त्व पर एक चर्चा तथा कार्लो कपोला के साथ उनका अन्तिम इंटरव्यू भी है, जो अपने में अति महत्त्वपूर्ण हैं और राकेश की साहित्यिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि को आलोकित और रेखांकित करते हैं। साथ ही बासु भट्टाचार्य द्वारा मोहन राकेश का एक अन्तरंग परिचय भी है जो अपने में अभूतपूर्व है।
Samkalin Laghukatha ka Samiksha Saundharya
- Author Name:
Jitendra Jeetu
- Book Type:

- Description: लघुकथा लेखन को आसान सी विधा मानकर बहुत लोग इस विधा के लेखन की ओर मुड़े और जाने–अनजाने अपनी अधकचरी बौद्धिकता और अज्ञान के बूते इस विधा का अहित करते चले गए। इन बहुत से लोगों में वे भी थे जो खालिस पाठक थे और लेखक बनना चाहते थे। जो कुछ बनना चाहते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वे बन गए। वे बिना पढ़े लेखक बन गए। उन्होंने बस उसी तरह की लघुकथाएं पढ़ी थीं और वे उसी तरह के लघुकथा लेखक बन गए। यह विराट स्तर पर धर्म परिवर्तन से भी अधिक संगीन मामला था जिसने साहित्य को बहुत बड़े पैमाने पर चोट पहुंचाई लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। इस पुस्तक में लघु कथा के सौन्दर्यशास्त्र पर चर्चा की गई है और इस विधा की महत्ता को स्थापित करने का प्रयास ही प्रधान है।
Customer Reviews
Be the first to write a review...
0 out of 5
Book