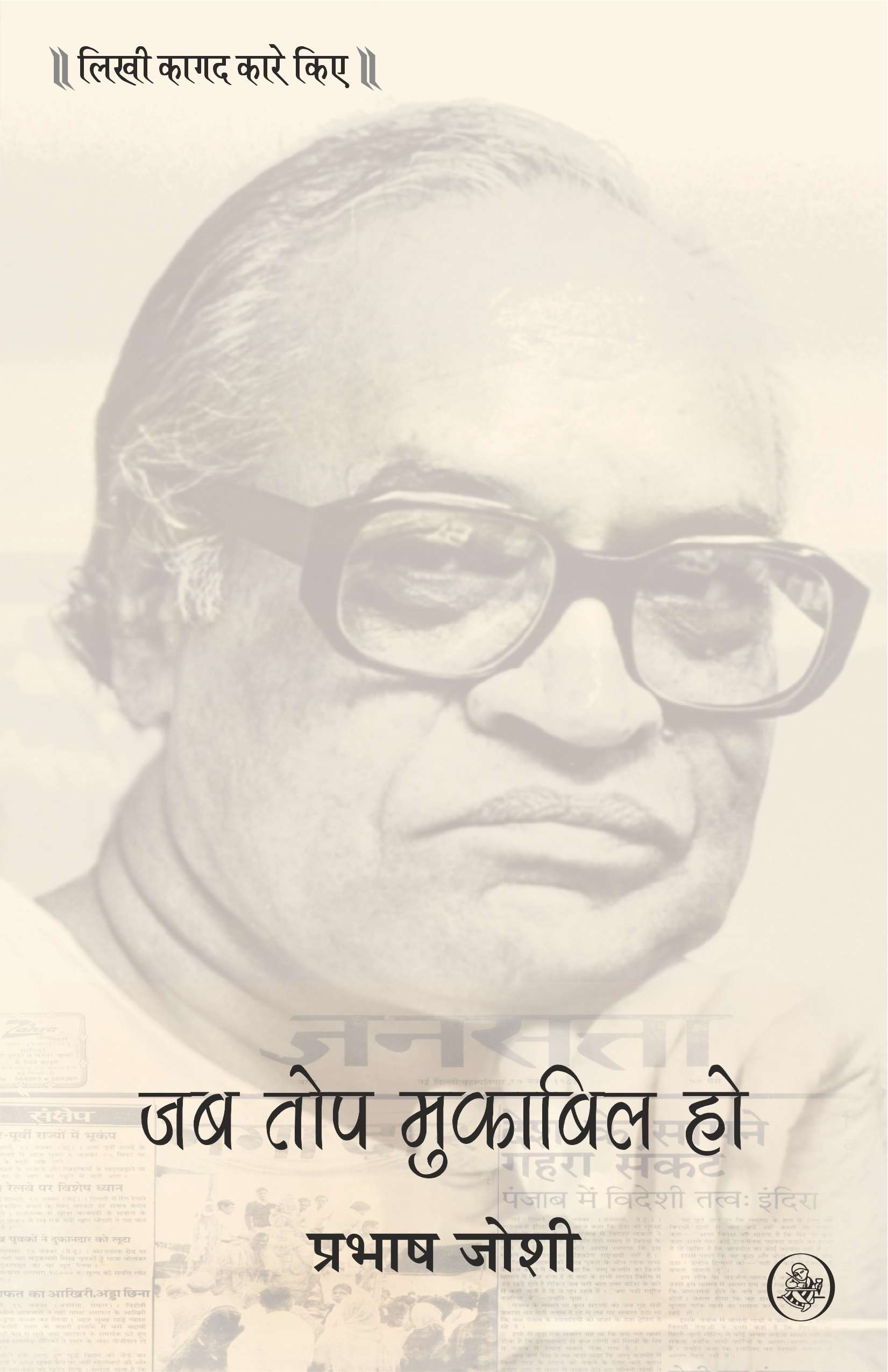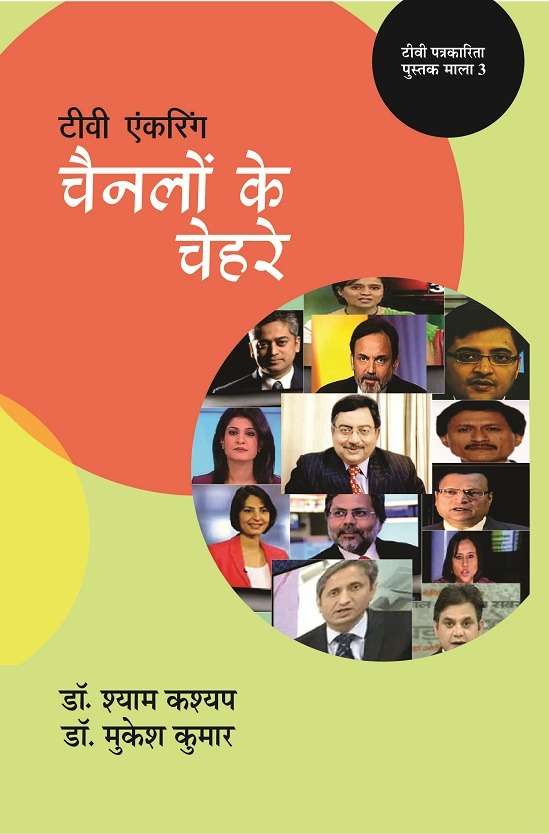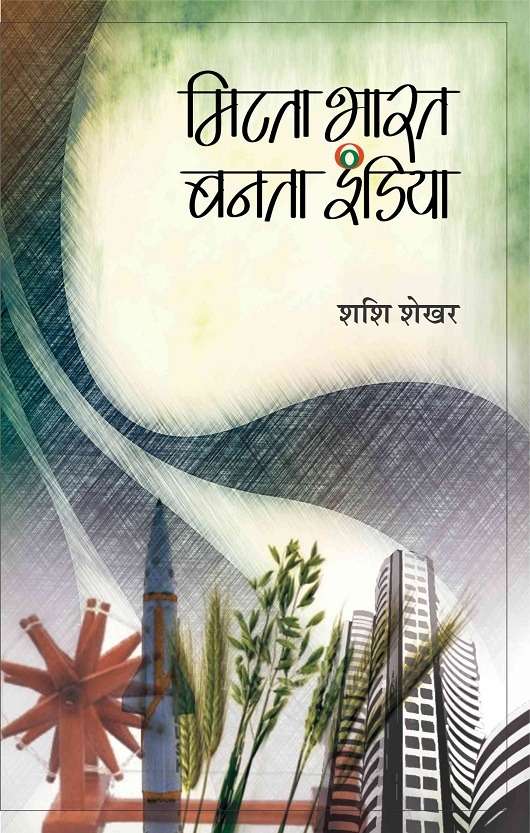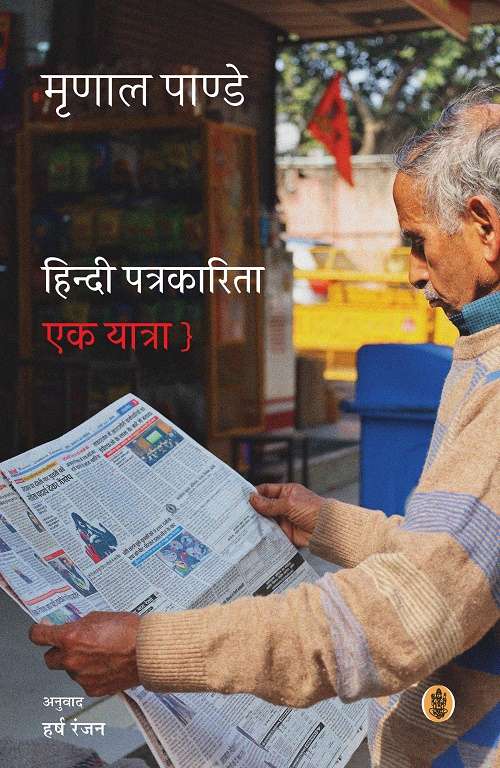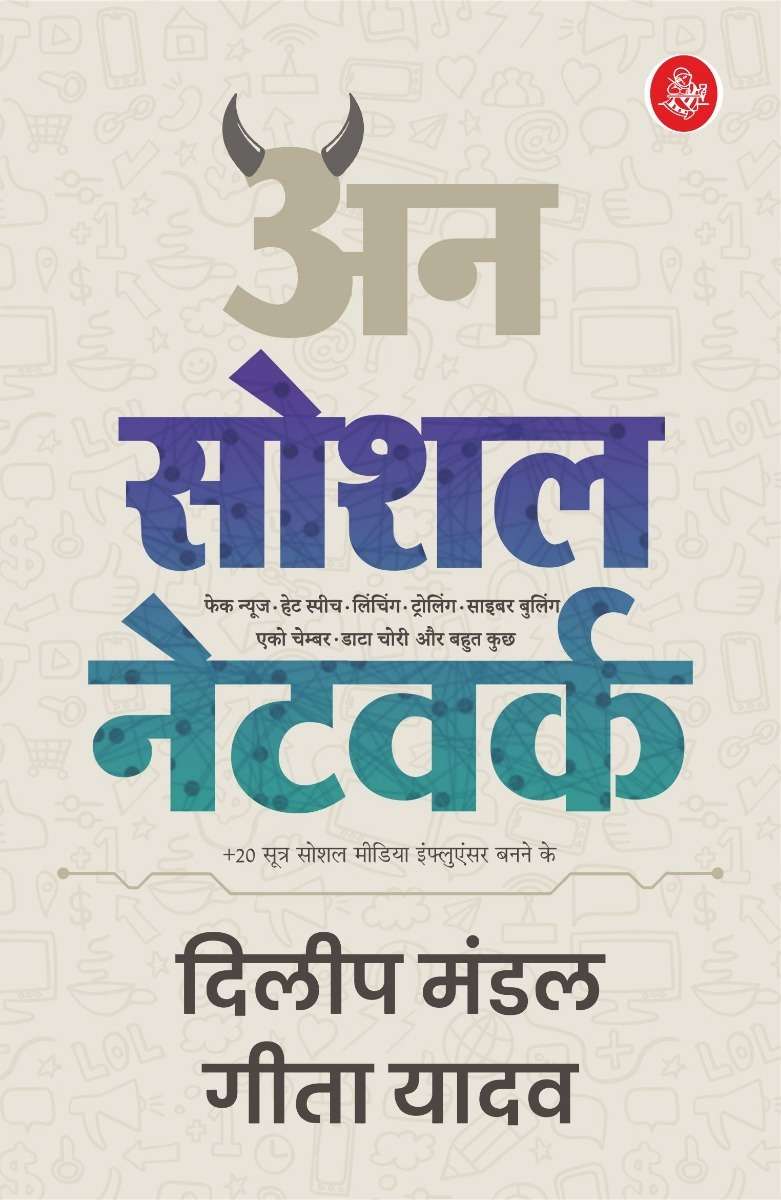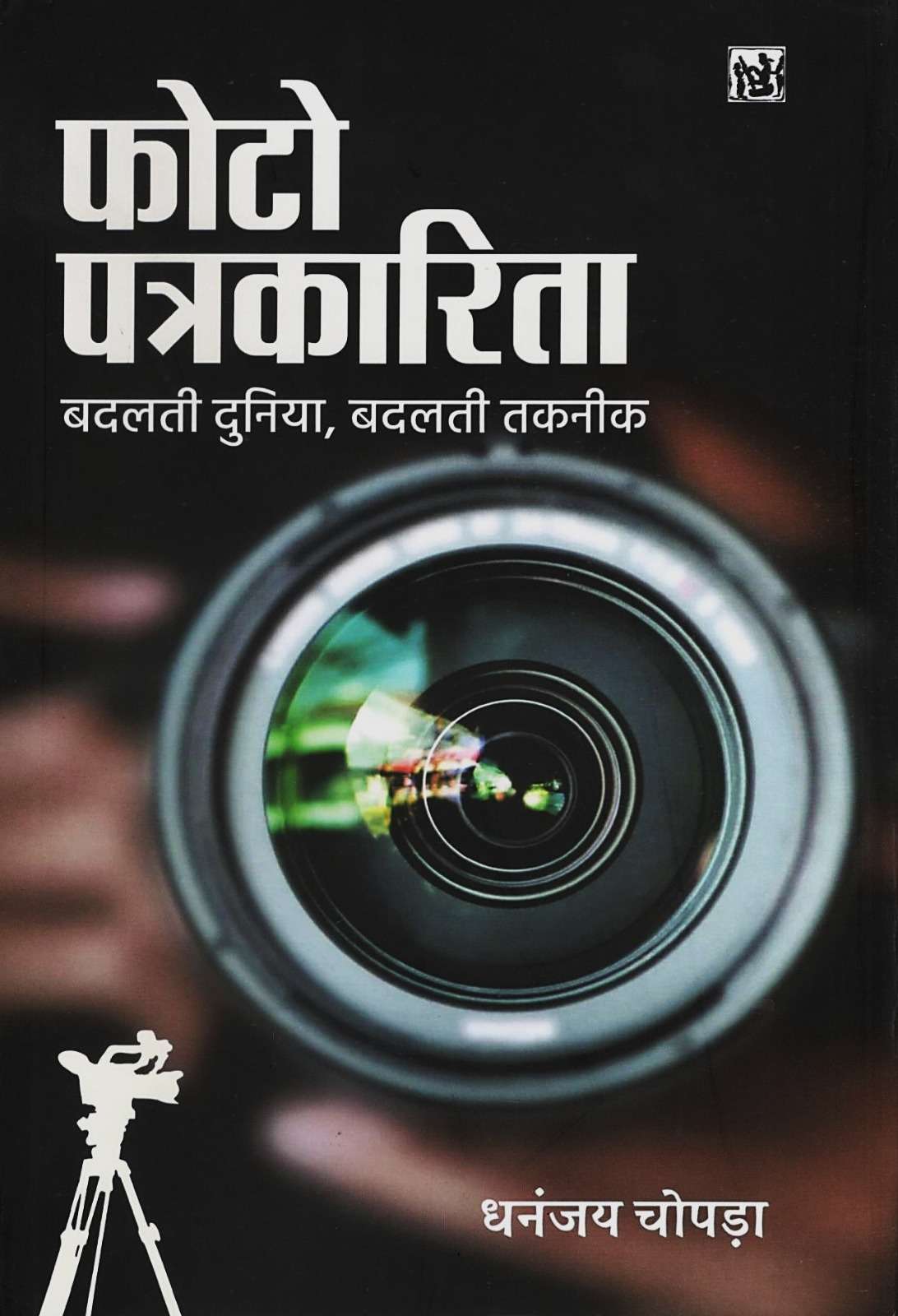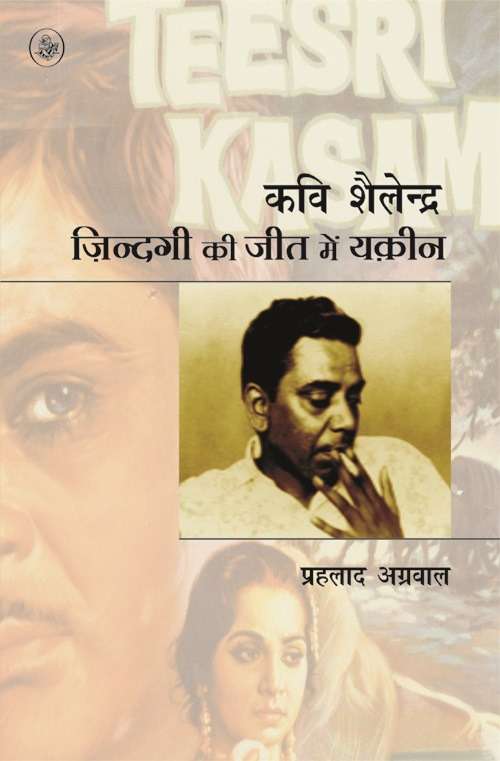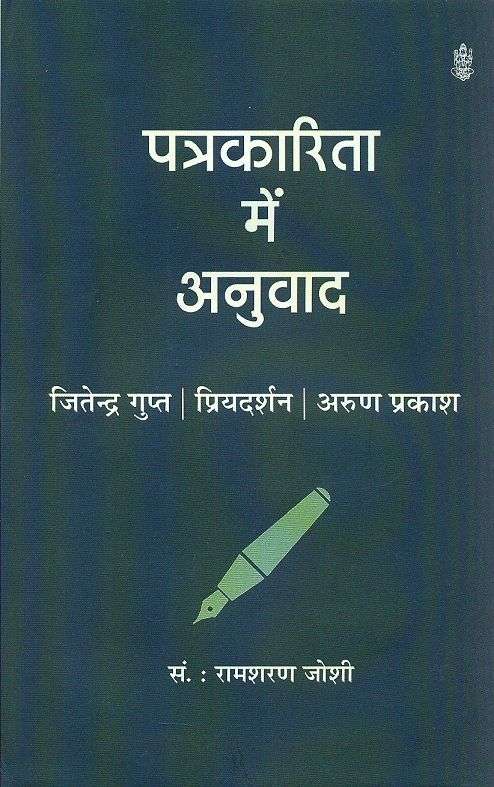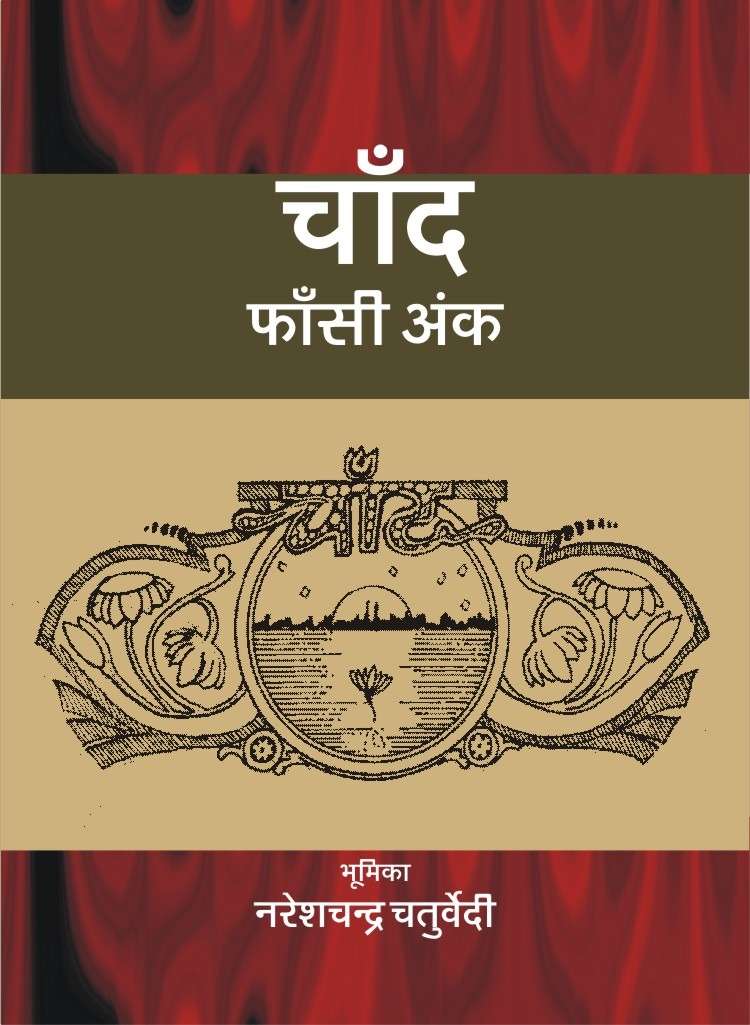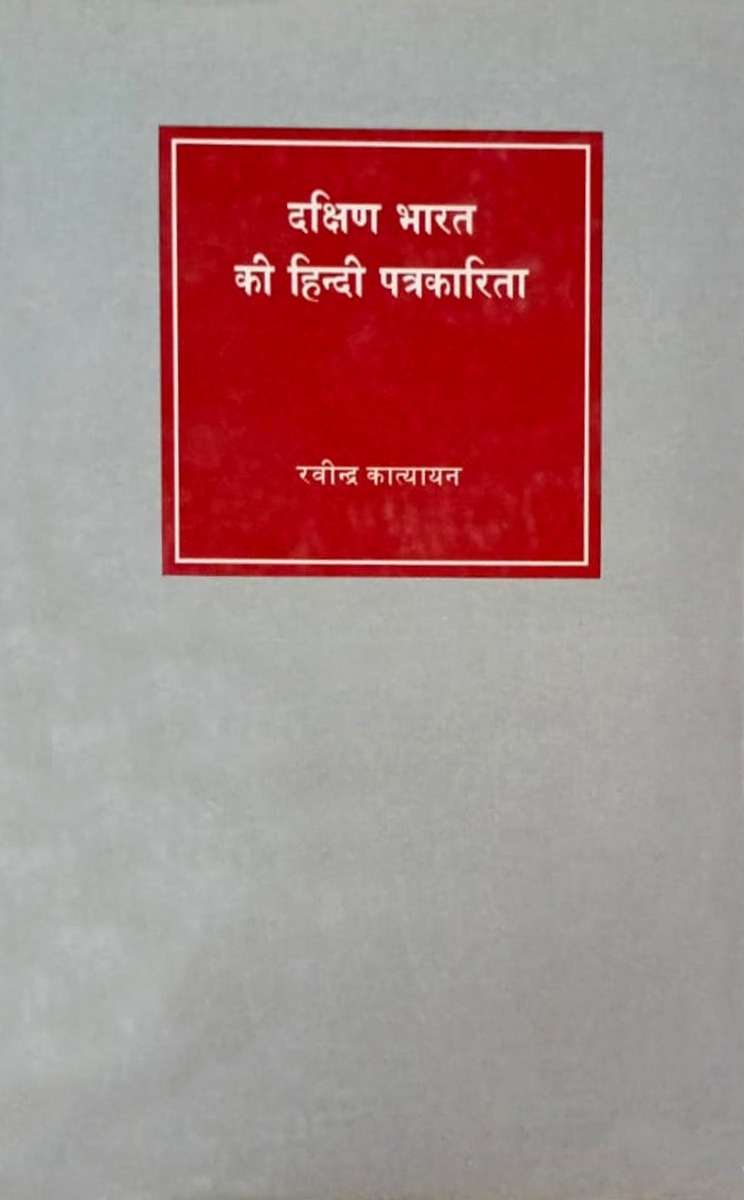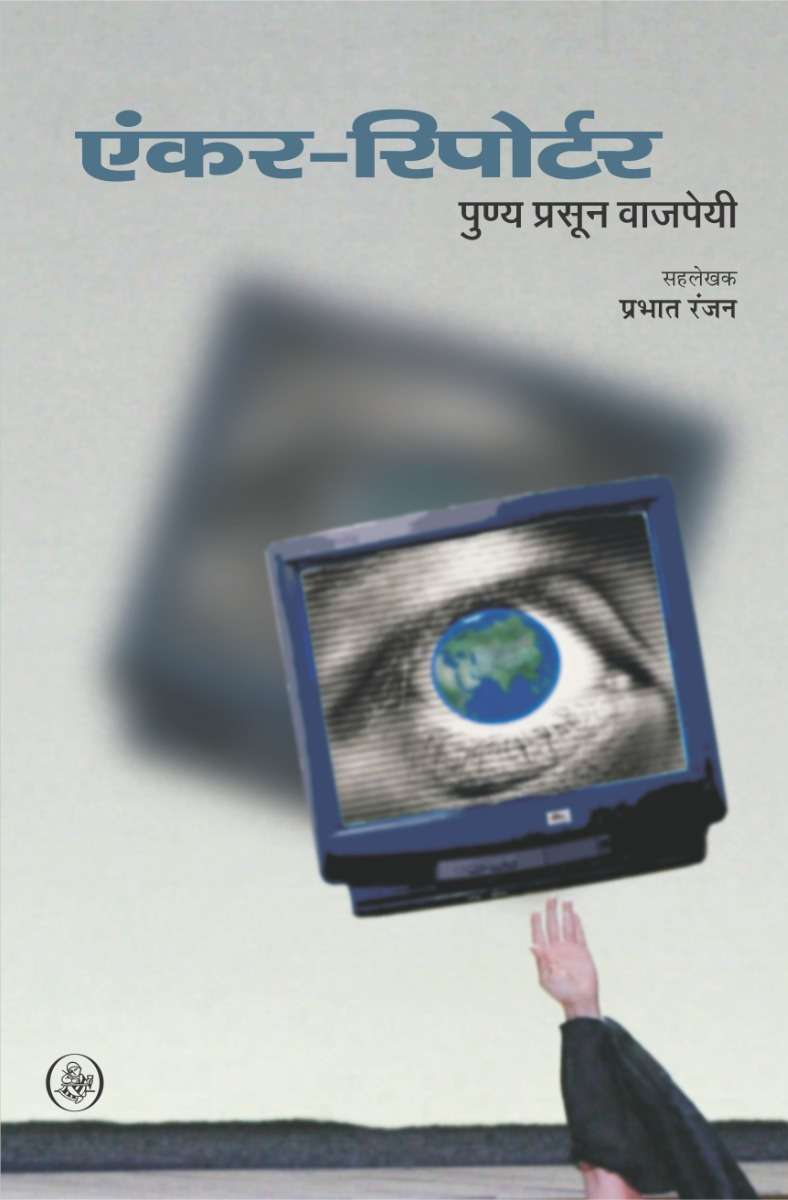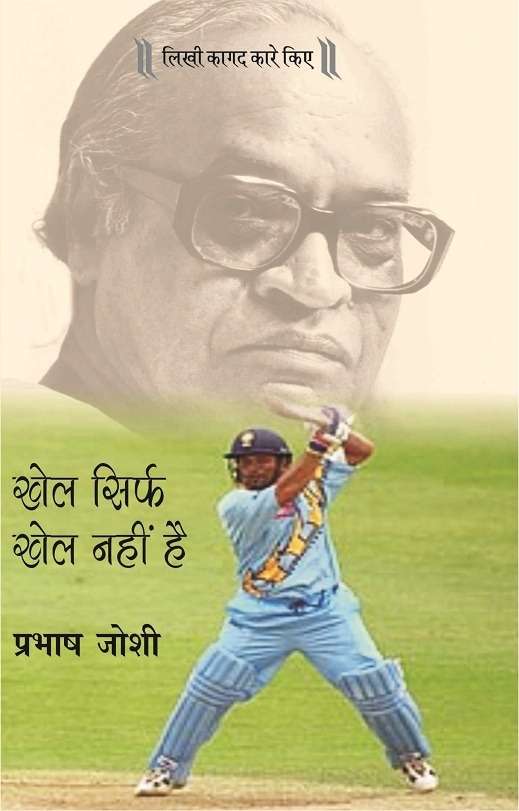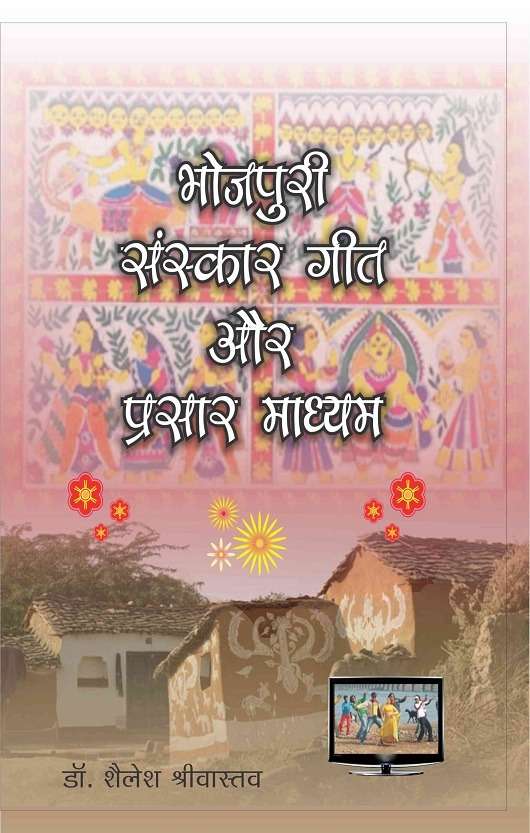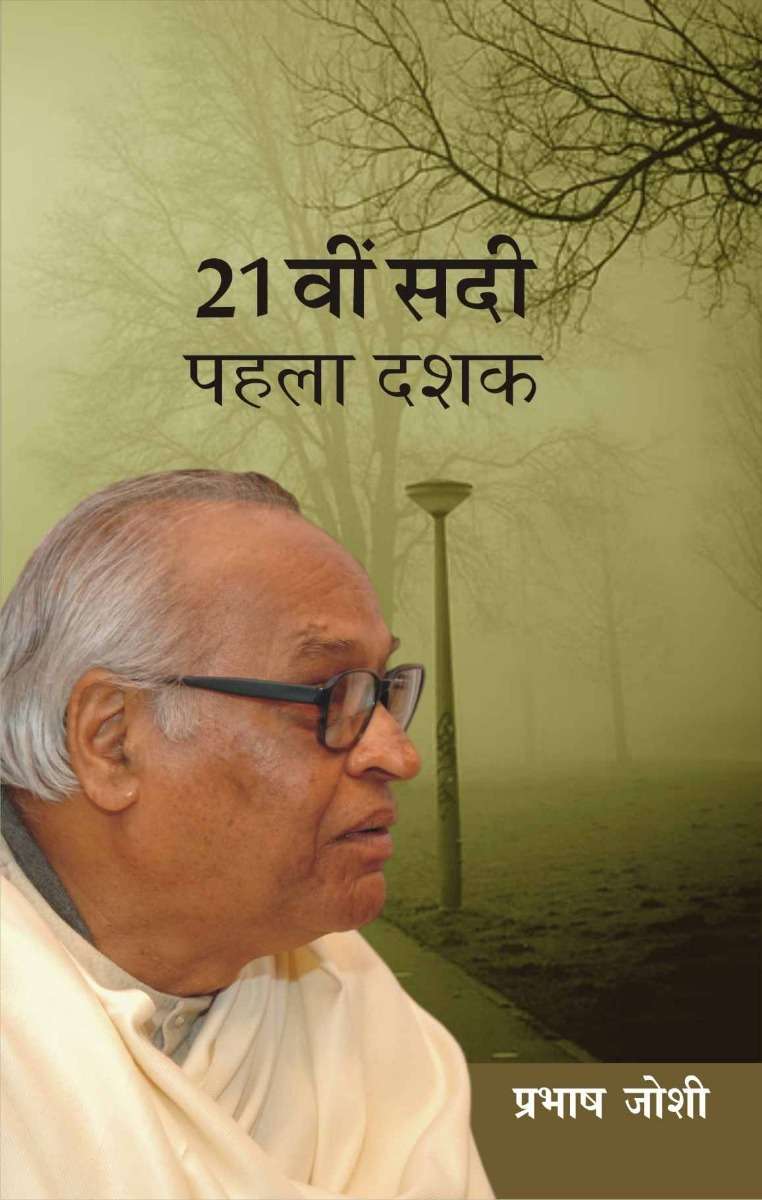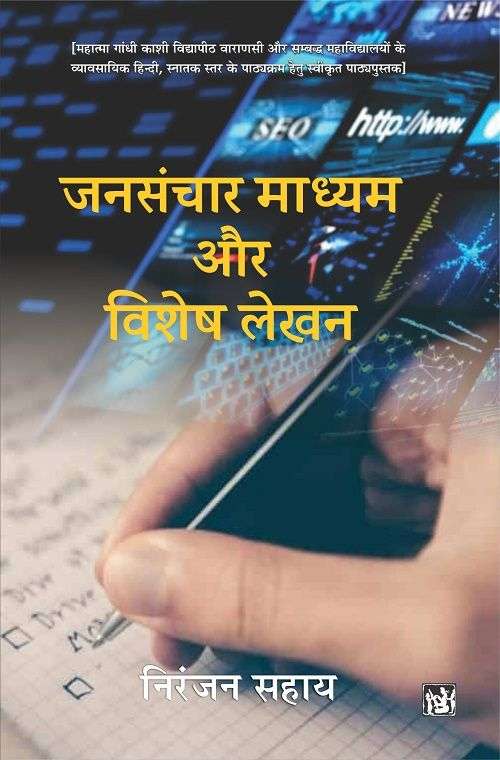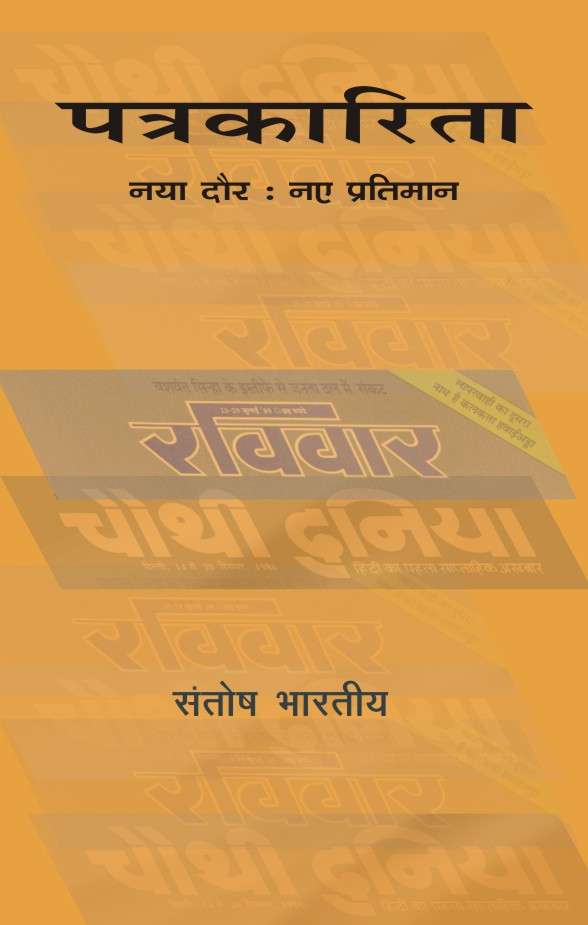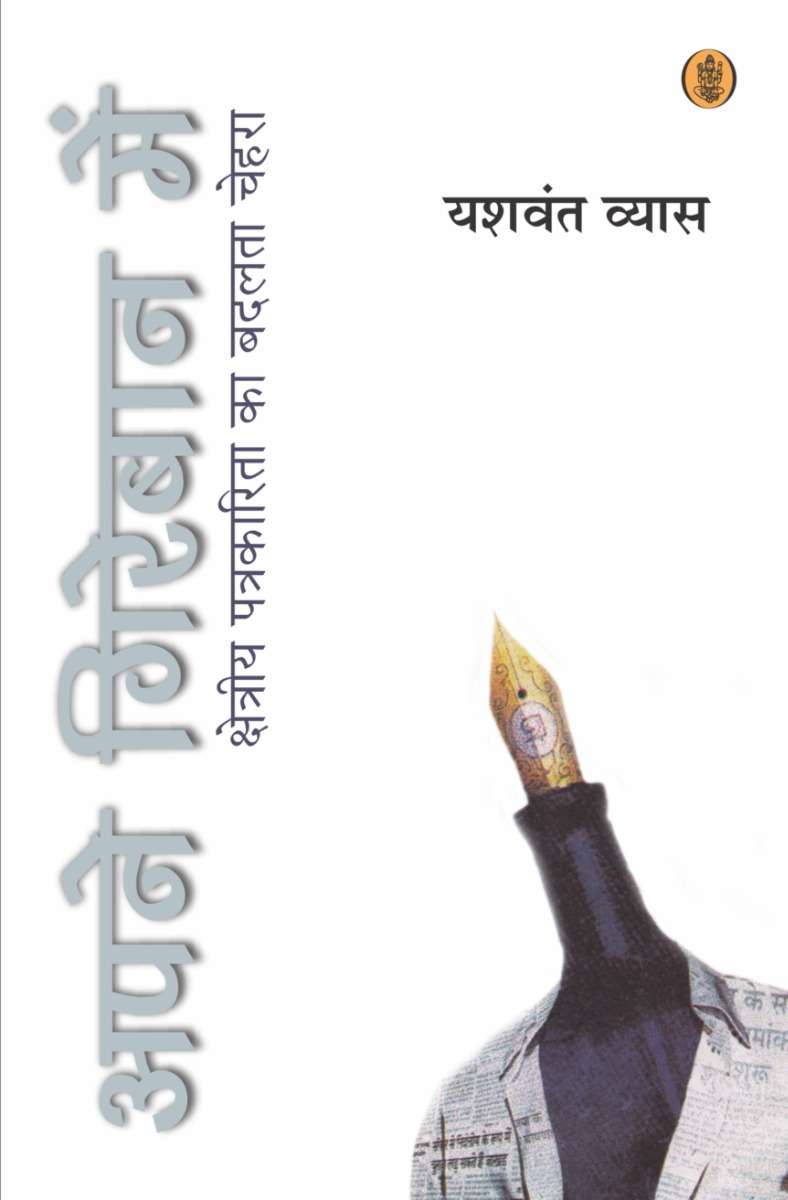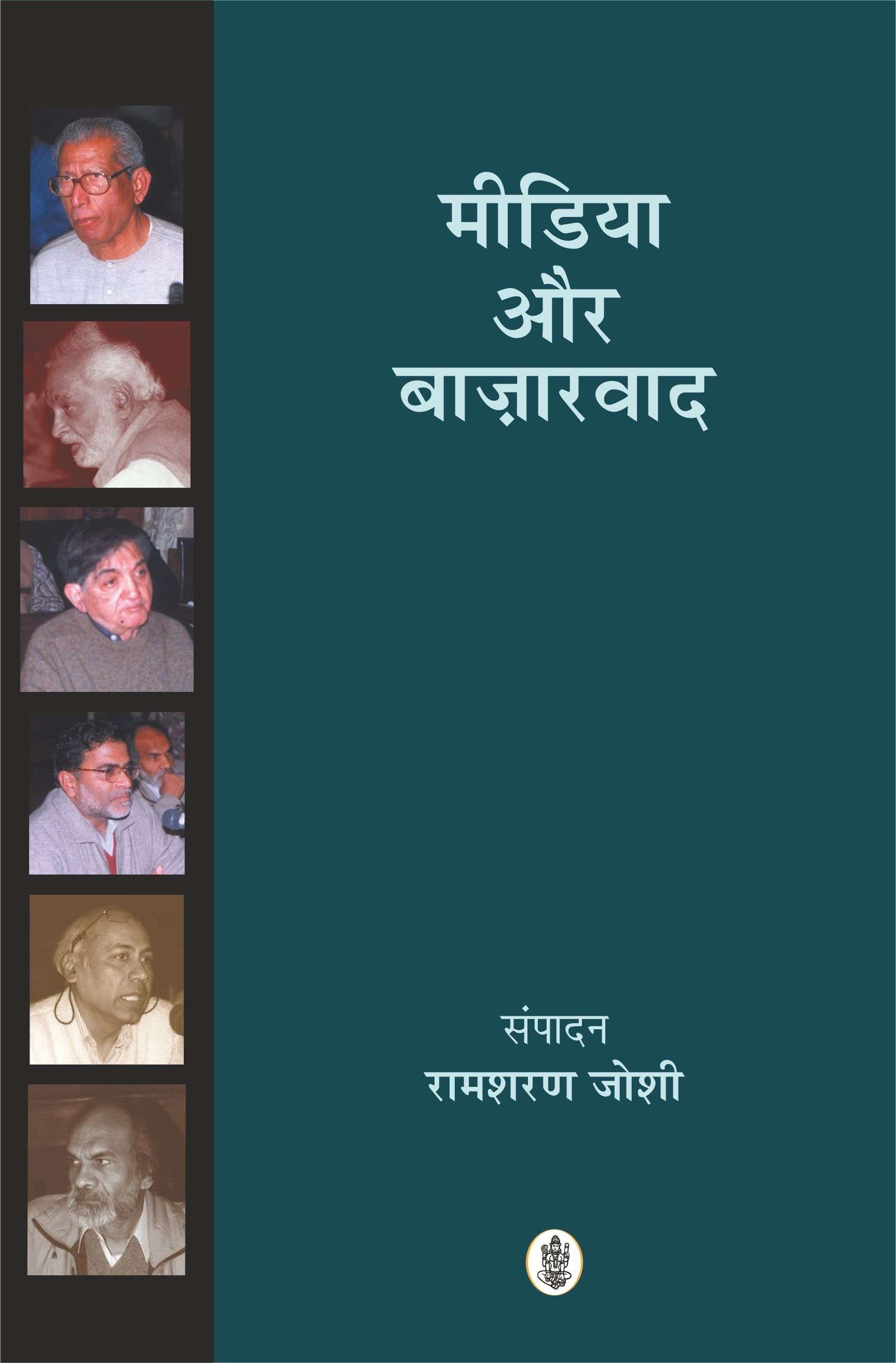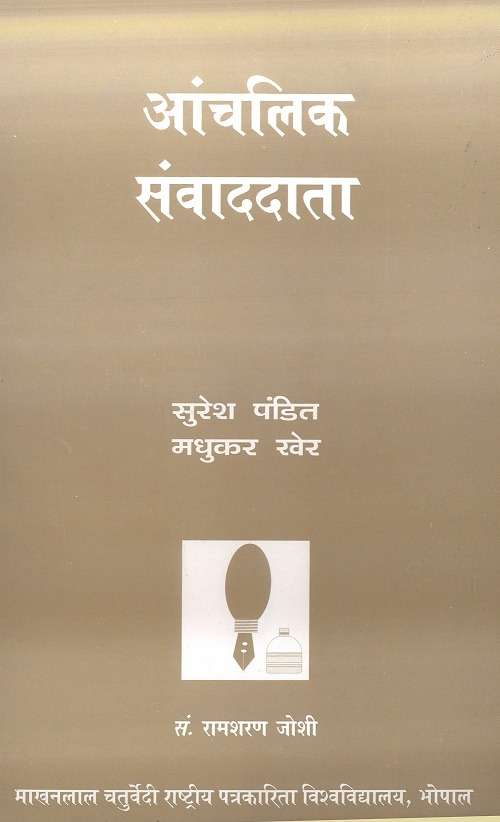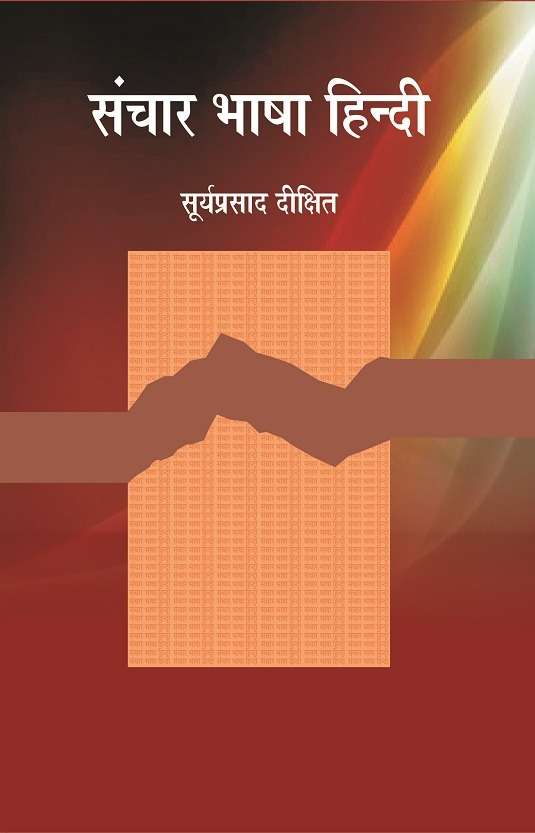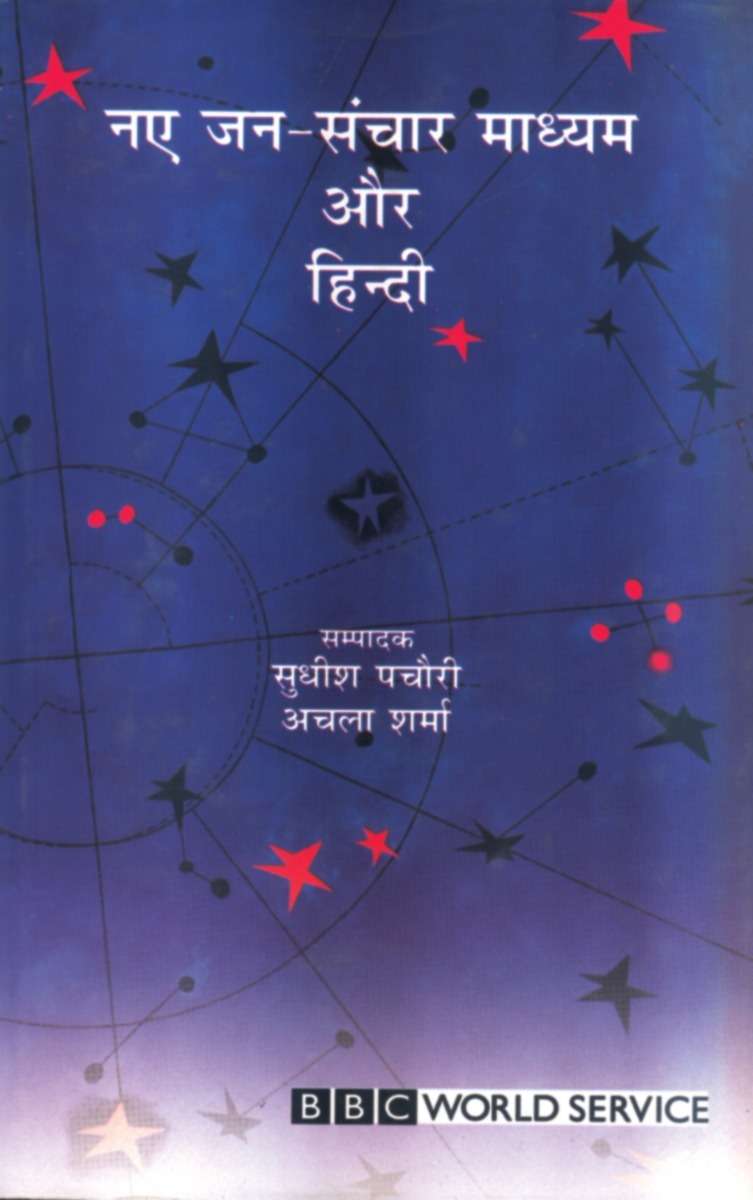
Naye Jan-Sanchar Madhyam Aur Hindi
Author:
Sudhish PachauriPublisher:
Rajkamal Prakashan SamuhLanguage:
HindiCategory:
Media0 Ratings
Price: ₹ 396
₹
495
Available
नए जन-संचार माध्यमों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है। हर प्रक्रिया में माध्यम बदल रहे हैं, हिन्दी भी बदल रही है। नए रूप बन रहे हैं। माध्यमों में भाषा ने स्वयं एक संचार किया है।</p>
<p>बदलती भाषा संचार की अनन्त अन्तर्क्रियाओं को जन्म दे रही है। हिन्दी के सामने नई चुनौतियाँ उपस्थित हैं और उतनी ही चुनौतियाँ माध्यमकर्मियों के सामने हैं।</p>
<p>बी.बी.सी. ने नए जन-संचार माध्यमों में हिन्दी के स्वरूप को लेकर इसीलिए एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार की सामग्री इस किताब में पाठकों के लिए उपलब्ध है।</p>
<p>यहाँ पाठकों को पहली बार बी.बी.सी. वेबसाइट की ‘स्टाइल बुक’ का परिचय मिलेगा। मीडिया का हिन्दी शब्दकोश होना चाहिए; एक पदावली कोश भी—इस तरफ़ कुछ इशारे यहाँ दिए गए हैं।</p>
<p>उम्मीद है कि यह किताब नए जन-संचार माध्यमों के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।
ISBN: 9788126704514
Pages: 124
Avg Reading Time: 4 hrs
Age: 18+
Country of Origin: India
Recommended For You
Jab Top Mukabil Ho
- Author Name:
Prabhash Joshi
- Book Type:

-
Description:
‘जब तोप मुकाबिल हो’ पुस्तक में प्रभाष जोशी के पत्रकारिता और मीडिया के दूसरे माध्यमों से सम्बन्धित लेखों के अलावा भाषा, अर्थ, जगत और महिलाओं से जुड़े लेख संकलित हैं। पुस्तक की भूमिका में प्रभाष जोशी लिखते हैं :
“ जब तोप मुकाबिल हो’ तो अख़बार निकालो’—ऐसा अकबर इलाहाबादी ने कहा है। आज लोग तोप का मुक़ाबला करने को अख़बार नहीं निकालते। वे पैसा और थोड़ा-बहुत पव्वा कमाने के लिए अख़बार निकालते हैं। इसलिए छापने के पैसे माँगने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं होती। अपन ऐसी पत्रकारिता करने नहीं आए थे। आज़ादी के बाद के दूसरे दशक में लगता था कि पत्रकारिता समाज बदलने और नया समतावादी और न्याय आधारित समाज बनाने का एक माध्यम है। आज आप ऐसी बातें करें तो लोग हँसने लगते हैं। फिर भी नरसिंह राव के कहने पर मनमोहन सिंह जब सन् इक्यानबे में नवउदार आर्थिक व्यवस्था लाए तब तक भारतीय पत्रकारिता में समाज परिवर्तन की वाहक बनने की इच्छा थी। आज जो प्रवृत्तियाँ आप देख रहे और दुखी हो रहे हैं, वे सब इसके बाद की हैं।
लेकिन यहाँ जो लेख संकलित हैं, वे आज की पत्रकारिता की आलोचना में नहीं हैं। ये पत्रकारिता करने या उसे कॉलेजों में पढ़ानेवालों के लिए भी नहीं हैं। मुझे हमेशा लगता रहा कि पत्रकारिता करने और करके दिखाने की चीज़ है, उपदेश देने या सिखाने की नहीं। यह अपने काम की आत्मालोचन है और जो कर न पाए, उसका अफ़सोस भी। लेकिन यह पत्रकारिता को जनसम्पर्क अभियान या प्रकाशन उद्योग बना देने के विरुद्ध तो है ही। मुझे अब कोई पचास साल हो जाएँगे लेकिन कभी मुझे नहीं लगा कि पत्रकारिता बेकार का काम है। ऐसा होता तो अपने अख़बार में मैं लगातार लिखता नहीं रह सकता था—न दैन्यम् न पलायनम्!”
Chainalon Ke Chehre
- Author Name:
Shyam Kashyap +1
- Book Type:

- Description: न्यूज़ चैनलों की जब भी बात होती है तो उनके एंकर की चर्चा ज़रूर की जाती है। और कैसे न हो। एंकर किसी भी चैनल की पहचान होते हैं। वे चैनलों के चेहरे होते हैं। किसी भी चैनल के एंकर जिस तरह के होते हैं, उसके आधार पर ही यह राय बनाई जाती है कि वह चैनल कैसा है। अगर एंकर ख़ूबसूरत, समझदार, चौकन्ने हैं तो उस चैनल को भी लोग उसी नज़र से देखेंगे। इसलिए कोई भी चैनल एंकर के चयन को सबसे ज़्यादा महत्त्व देता है। वह ऐसे चेहरों की तलाश में रहता है जो दर्शकों को बाँध सकें। ज़ाहिर है कि टेलीविज़न एंकरिंग एक आकर्षक एवं प्रभावशाली विधा है, पेशा है और यह बहुत स्वाभाविक है कि छात्र ही नहीं, टेलीविज़न में वर्षों से काम कर रहे पत्रकार भी यह सपना पाले रहते हैं कि उन्हें भी स्क्रीन पर आने का मौक़ा मिले। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा भी एंकरिंग के लिए होती है। चैनल चलानेवाले भी एंकर के चयन के मामले में बेहद कठोर होते हैं। कोई भी चैनल एंकर को लेकर समझौता नहीं करना चाहता। इसलिए एंकर बनने के इच्छुक लोगों को यह ज़रूर पता होना चाहिए कि उनकी राह बहुत आसान नहीं है और यह सपना कैसे पूरा हो सकता है या उसे पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, इस पर सोचना ज़रूरी है। आजकल सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि एंकरिंग के बारे में विस्तार से जानने और फिर उसे सीखने का कोई इन्तज़ाम नहीं है। दिल्ली, मुम्बई जैसे कुछ बड़े शहरों को छोड़ दें तो कहीं ढंग के प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं। जहाँ हैं, वहाँ सिखानेवाले ख़ुद ही प्रशिक्षित नहीं हैं। बड़े शहरों में भी अधिकांश प्रशिक्षण संस्थान मोटी रक़म वसूलने के लिए ज़्यादा कुख्यात हैं। ऐसे में कमज़ोर हैसियत और छोटे तथा मझोले शहरों में रहनेवाले लोग क्या करें, कहाँ जाएँ? उन्हें तो किताबों की ही मदद से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। लेकिन मुश्किल यह है कि टेलीविज़न एंकरिंग पर ढंग की किताबें भी नहीं हैं। जो हैं वे दशकों पुरानी एंकरिंग को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं जबकि अब उसमें आमूलचूल परिवर्तन आ चुका है। टेलीविज़न पत्रकरिता माला के तहत ‘चैनलों के चेहरे’ शीर्षक से एंकरिंग पर किताब लिखने का मक़सद इस कमी को पूरा करना ही है। कोशिश रही है कि यह किताब एंकरिंग की एक परिपक्व गाइड की भूमिका अदा करे। इसलिए टेलीविज़न के मौजूदा दौर को ध्यान में रखकर और एंकरिंग के बारे में विस्तार से जानकारी जुटाकर इसे तैयार किया गया है। यह पुस्तक एंकरिंग के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है, जिससे वे ख़ुद अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें।
Mitata Bharat Banta India
- Author Name:
Shashi Shekhar Tiwari
- Book Type:

-
Description:
20वीं सदी के अन्तिम दशक में भारत की राजसत्ता द्वारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उदारीकरण की नीति अपनाई गई। धीरे-धीरे बाज़ार मुक्त किया जाने लगा तथा अनेक महत्त्वपूर्ण सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण होने लगे। इस पहल का भारतीय समाज की संरचना पर गहरा असर हुआ। उसके आधार पर ऊपरी ढाँचे में अनेक निर्णायक परिवर्तन घटित होने लगे। उसका प्रभाव राजनीति, समाज, शिक्षा, जीवन-शैली तथा अन्तरराष्ट्रीय मामलों पर सीधे दिखाई देने लगा। 21वीं सदी के पहले दशक में इस परिवर्तन को जिन लोगों ने सबसे पहले पहचानने की कोशिश की, उनमें शशि शेखर पहली क़तार में हैं।
उदारीकरण की आँधी में मिटते भारत और बनते इंडिया की गूँज अगर सुननी हो तो शशि शेखर की इस पुस्तक के इन लेखों को पढ़ जाइए। 2001 से 2010 के बीच उन्होंने लगभग हर हफ़्ते अपने कॉलम ‘आजकल’ में अपने समय का साप्ताहिक इतिहास दर्ज किया है। यह पुस्तक इस कॉलम के उन्हीं लेखों का संकलन है। इन लेखों के द्वारा आप शशि शेखर के नज़रिए से 21वीं सदी के पहले दशक की धड़कनों की समग्रता में महसूस कर सकेंगे। इन लेखों में समय पर बहस है। समय से शिकायत है। समय की प्रशंसा है। समय की कठोरता को जीत लेने का दम-खम है। समय के वास्तविक स्वरूप को पहचानने का तीक्ष्ण विवेक भी है।
Hindi Patrakarita : Ek Yatra
- Author Name:
Mrinal Pande
- Book Type:

- Description: अरसे तक ‘राष्ट्रीय मीडिया’ मानी जानेवाली अंग्रेजी मीडिया के वर्चस्व को, अपने व्यापक जमीनी जुड़ाव की बदौलत किनारे कर, देश के कोने-कोने तक पहुँच बना चुकी हिन्दी मीडिया का यह ऐतिहासिक सफर अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहा है, जिसका ब्योरा मृणाल पाण्डे ने इस किताब में दर्ज किया है। इसमें औपनिवेशिक काल में बढ़ती राष्ट्रीय भावना से उपजे अखबार और अंग्रेजी की अधीनता से लेकर, आजादी के बाद के दौर में विज्ञापन और निजी कॉरपोरेटों की बढ़ती मौजूदगी से आए उन बदलावों का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है जिन्होंने पत्रकारिता का परिदृश्य आमूल बदल दिया। आगे डिजीटलीकरण, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के बढ़ते प्रभावों और विज्ञापनों पर भारी निर्भरता ने बदलावों को और तेज किया। और अब, राजनीति, कारपोरेट और मीडिया के बीच स्पष्ट किन्तु जटिल रिश्तों की छाया में यह सवाल सामने है कि एक समय भारतीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का जरिया बनी हिन्दी मीडिया आज हमारे संविधान प्रदत्त सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हक को आगे बढ़ा पाने में किस हद तक सक्षम है? जरूरी जानकारियों से भरी यह किताब पत्रकारिता के छात्रों, प्रोफेसरों और मीडियाकर्मियों के साथ-साथ उन सबके लिए एक विचारोत्तेजक पाठ है जो मीडिया और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास, वर्तमान और भविष्य में दिलचस्पी रखते हैं।
Un Social Network
- Author Name:
Geeta Yadav +1
- Book Type:

- Description: ‘अनसोशल नेटवर्क’ किताब भारत के विशिष्ट सन्दर्भों में सोशल मीडिया का सम्यक् आकलन प्रस्तुत करती है। जनसंचार का नया माध्यम होने के बावजूद, सोशल मीडिया ने इस क्षेत्र के अन्य माध्यमों को पहुँच और प्रभाव के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है और यह दुनिया को अप्रत्याशित ढंग से बदल रहा है। इसने जितनी सम्भावनाएँ दिखाई हैं, उससे कहीं अधिक आशंकाओं को जन्म दिया है। वास्तव में राजनीति और लोकतंत्र से लेकर पारिवारिक और व्यक्तिगत सम्बन्धों तथा उत्पादों और सेवाओं की खरीद-बिक्री तक शायद ही कोई क्षेत्र होगा, जो सोशल मीडिया के असर से अछूता हो। यह एक ओर जनसंचार के क्षेत्र को अधिक लोकतांत्रिक बनानेवाला नजर आया तो दूसरी ओर इस क्षेत्र को प्रभुत्वशाली शक्तियों के हित में नियंत्रित करने का साधन भी बना है। ऐसे ही अनेक पहलुओं का विश्लेषण करते हुए यह किताब सोशल मीडिया की बनावट के उन अहम बिन्दुओं की शिनाख्त करती है जो इसे ‘अनसोशल’ बनाती हैं। यह किताब सोशल मीडिया के अध्येताओं के साथ-साथ इसके यूजरों के लिए भी खासी उपयोगी है।
Photo Patrakarita
- Author Name:
Dhananjai Chopra
- Book Type:

- Description: हमारा समय विजुअल कम्युनिकेशन यानी दृश्य संचार का समय है। वास्तविक दुनिया हो या आभासी दुनिया, हर तरफ छवियां ही छवियां हैं। कास्टिंग के लगभग सारे उपक्रम यानी प्रिंटकास्ट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, वेबकास्ट और ह्यूमनकास्ट अनायास ही छवियों के अधिकाधिक प्रयोग की होड़ में शामिल हो गए हैं। संचार के क्षेत्र में छवियों यानी दृश्यों के इस तरह प्रयोग से जन-संप्रेषण की दुनिया में बड़ा बदलाव आया है। इस बदलाव का कारण बना, हमारे मोबाइल फोन में कैमरे का आ जाना। इक्वींसवीं सदी के प्रारंभ से ही लोगों ने अपने आसपास के दृश्यों को सहेजना शुरू कर दिया था। दृश्यों के माध्यम से जन इतिहास का लिखा जाना यह बता रहा था कि आने वाले समय में शब्दों से कहीं अधिक दृश्य पढ़े जाएंगे। हुआ भी यही, हमने एक ऐसे समाज की रचना कर ली है, जिसमें दृश्य संचार के बिना रह पाना मुश्किल हो रहा है। टेक्नोलॉजी के बलबूते बदलती दुनिया और बदलते समय में दृश्य संस्कृति विकसित हो रही है। दृश्य गढ़े जा रहे हैं, रचे जा रहे हैं, प्रस्तुत किए जा रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं। अब से पहले इतने अधिक दृश्यों का आदान-प्रदान कभी नहीं हुआ था। दरअसल यह दृश्य विस्फोट यानी विजुअल एक्सप्लोजन का समय है। यह फोटोग्राफी और फोटो पत्रकारिता को सीखने, समझने, सहेजने और संचरित करने का अप्रतिम समय है।
Kavi Shailendra : Zindagi Ki Jeet Mein Yakeen
- Author Name:
Prahlad Agarwal
- Book Type:

- Description: कुछ अकेले नहीं हैं और पहले भी नहीं हैं—शैलेन्द्र, विद्वज्जनों ने जिनकी ओर नज़र नहीं डाली—ऐसे अनेकानेक लोककवि हैं। यूँ हर ज़माने ने अपने ज़माने की लोकरचना की सादगी की संश्लिष्टता को स्वीकार करने में कोताही की—और होकर यूँ रहा कि समय के साथ वह रंग और गहरा होता चला गया। पीढ़ियाँ-दर-पीढ़ियाँ उनके शब्दों में ज़िन्दगी के नए मायने तलाशती रहीं। शैलेन्द्र के गीत हमारे बचपन की गुनगुनाहटों में शामिल होकर आज तक हमसफ़र हैं। दुनिया-भर की पुरकशिश कविता की तरह उन्होंने ज़िन्दगी की पुरपेच गलियों में आलोकित राजपथ प्रशस्त किया। इतने सरल और लुभावने कि आवारामिज़ाजी से ज़ुबाँ पर चढ़ जाएँ, क़दम-ब-क़दम ज़िन्दगी के फ़लसफ़े में तब्दील होते हुए। अपनी मासूम गुनगुनाहटों के शब्द के फ़नकार का नाम हमें सालों बाद पता चला और इस परिचय के ऊषाकाल में ही वह सितारा टूट गया। जब शैलेन्द्र ने आत्मघात किया, हम उन्नीस साल के थे। इसके चंद महीने पहले ही शैलेन्द्र निर्मित एकमात्र फ़िल्म ‘तीसरी क़सम’ प्रदर्शित हुई थी। नहीं मालूम सच है या झूठ, लेकिन कहा जाता है कि शैलेन्द्र को यक़ीन था, इसे ‘राष्ट्रपति स्वर्णपदक’ मिलेगा—और मिला, लेकिन वह दिन देखने के लिए शैलेन्द्र नहीं थे। जनकवि शैलेन्द्र के बहुआयामी रचनात्मक अवदान का आकलन करने की विनम्र कोशिश है यह पुस्तक।
Patrakarita Mein Anuwad
- Author Name:
Priyadarshan
- Book Type:

- Description: अनुवाद की बात आते ही हमें दो भाषाओं का परिदृश्य ध्यान में आता है। अनुवाद की ज़रूरत केवल दो भाषाओं के सन्दर्भ में ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अनुवाद के कई ऐसे आयाम होते हैं जिन पर हम आम तौर पर ग़ौर नहीं करते। दो विरोधी दर्शन और विचार रखनेवालों के बीच संवाद के लिए भी अनुवाद की ज़रूरत होती है। अनुवाद के ऐसे ग़ैर-पारम्परिक अर्थ और प्रसंग को छोड़ भी दें तो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुवाद का अहम स्थान है।हिन्दी के प्रति प्रेम राष्ट्र-गौरव की भावना आत्म-सम्मान जैसे सराहनीय और वांछनीय आदर्शों के सशक्त हिमायती होने के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अख़बारों द्वारा अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य के निरन्तर अद्यतन और सही ढंग से अंकन के लिए अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद की ज़रूरत अभी भी बरकरार है। अनुवाद की कला कठिन है क्योंकि दो भिन्न भाषाओं की अभिव्यक्ति शैली भी भिन्न होती है। हर भाषा का एक अपना चरित्र होता है और उस चरित्र के कारण भाषा की शैली की विशिष्टता होती है। विद्वान लेखकों द्वारा तैयार इस पुस्तक के ज़रिए इस कला को विस्तार देने और सँवारने की कोशिश की गई है। पत्रकारिता से जुड़े हर व्यक्ति के लिए यह उपयोगी पुस्तक है।
Chand : Phansi Ank
- Author Name:
Nareshchandra Chaturvedi
- Book Type:

- Description: Awating description for this book
Dakhinn Bharat Ki Hindi Patrakarita
- Author Name:
Ravindra Katyayan
- Book Type:

- Description: Dakhinn Bharat Ki Hindi Patrakarita
Anchor Reporter
- Author Name:
Punya Prasoon Vajpayee
- Book Type:

- Description: जब कोई व्यक्ति टेलीविज़न के परदे पर समाचार देख रहा होता है तो उसके ज़ेहन में दो व्यक्ति अहम हो जाते हैं—एंकर और रिपोर्टर। एंकर जो टेलीविज़न के परदे पर पहले-पहल किसी ख़बर की सूचना देता है, उसके बारे में बताता है, तो रिपोर्टर वह होता है जो घटनास्थल से यह बता रहा होता है कि घटनाक्रम किस प्रकार घटित हुआ। वास्तव में किसी महत्त्वपूर्ण ख़बर के दौरान दर्शकों के लिए यह भी महत्त्वपूर्ण नहीं होता है कि वे चैनल कौन-सा देख रहे हैं, वह महत्त्वपूर्ण ख़बर जिस भी चैनल पर आ रही होती है, दर्शकों का रिमोट उसी चैनल पर ठहर जाता है। ऐसे में किसी समाचार चैनल के लिए एंकर और रिपोर्टर बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि दर्शकों को चैनल से जोड़ने का काम वही करते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि एंकर और रिपोर्टर को हर परिस्थिति को सँभालने में माहिर होना चाहिए। पुण्य प्रसून वाजपेयी ‘आजतक’ के प्रमुख एंकर थे। पेशे के रूप में एंकर-रिपोर्टर का काम क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है, उसका काम कितना चुनौतीपूर्ण होता है—पुण्य प्रसून जी ने इन्हीं पहलुओं को विभिन्न कोणों से इस पुस्तक में रखा है। यह पुस्तक टी.वी. पत्रकारिता सीखनेवालों के लिए तो उपयोगी है ही, उनके लिए भी बड़े काम की साबित हो सकती है जो इन पेशों की चुनौतियों को जानना-समझना चाहते हैं। यह एक ‘इनसाइडर’ की ‘इनसाइड स्टोरी’ की तरह है।
Khel Sirf Khel Nahin Hai
- Author Name:
Prabhash Joshi
- Book Type:

-
Description:
‘खेल सिर्फ़ खेल नहीं है’ पुस्तक में प्रभाष जोशी द्वारा खेल पर लिखे गए लेख संकलित हैं। इन लेखों से हिन्दी में खेल विश्लेषण का पूरा परिदृश्य ही बदल गया था।
प्रभाष जोशी ने अपनी भूमिका में लिखा है :
“इस पुस्तक में वे लेख दिए गए हैं जो मैंने खेल पर लिखे। अब जिस तरह राजनीति पर सम्पादकीय पेज पर सम्पादकीय या मुख्य लेख या जब ज़रूरी हुआ, पहले पेज पर लिखता रहा। उसी तरह खेल जैसे खेले जाते रहे—पहले पेज, आख़िरी पेज और सम्पादकीय पेज पर कवर करता रहा। ऐसा करते हुए जो बच जाता था या जिसके मानवीय पहलू के लिए ख़बर में गुंजाइश नहीं होती थी, वही कागद कारे में आया।
खेल को महज़ एक मनोरंजन या शारीरिक व्यायाम मैं नहीं मानता। खेल मनुष्य का चरित्र बनाता है लेकिन उससे भी ज़्यादा खेल में मनुष्य का चरित्र व्यक्त और प्रकट होता है। अंग्रेज़ माँ के कैनेडियन बेटे ग्रेग रूज़ेस्की ने अमेरिकी माइकल चांग से एक मैच में एक सेट जीता, एक हारा और तीसरे सेट में चार-चार गेम पर थे। रूज़ेस्की सर्व कर रहा था तीस-तीस पर। गेम जीतने के लिए दो पाइंट और चाहिए थे। किसी तरह वह ड्यूस पर आया और फिर एडवांटेज पर। एक पाइंट के बाद गेम उसका होना था। सर्व करने के पहले रूज़ेस्की ने अपने पर क्रॉस बनाया और गेंद चूमी। तभी मुझे लगा कि गेम यह हार जाएगा। रूज़ेस्की ने सर्विस की और नेट में मार दी और फिर मार के डबन फॉल्ट कर दिया। चांग को मौक़ा मिला और वह गेम और सेट दोनों ले गया। तब रूज़ेस्की की सर्विस गोले जैसे होती थी और उसका कैरियर बन रहा था। मैंने लिखा कि वह कभी कोई ग्रैंड स्लेम जीत नहीं पाएगा। जीता भी नहीं और अब तो खेलता भी नहीं। उस मैच के सबसे नाजुक और निर्णायक मौक़े पर रूज़ेस्की का अपने पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने क्रॉस बनाया और गेंद चूमी। सबसे कठिन घड़ी में जिसका अपने पर विश्वास नहीं होता, उससे कुछ भी जीता नहीं जाएगा।
मैं क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेल इन्हीं नाजुक और कठिन घड़ियों में खिलाड़ियों और टीमों के चरित्र समझने के लिए देखता हूँ। महज़ मन बहलाने के लिए नहीं। खेल सचमुच एक अनुशासन है जो मनुष्य को पूरा बनाता और प्रकट करता है।”
Bhojpuri Sanskar geet Aur Prasar Madhyam
- Author Name:
Shailesh Shrivastva
- Book Type:

-
Description:
लोकगीत माटी की महक हैं, संस्कारों के स्वर हैं, अन्तर की आवाज़ हैं। इनकी पूरी व्यापक धरोहर श्रव्य परम्परा में सिमटी हुई है। शैलेश जी ने लुप्त होते लोकगीतों को सुरक्षित रखने और इनके संरक्षण हेतु स्तुतनीय प्रयास किया है। वह स्वयं एक जानी-मानी गायिका हैं। कुछ लोकगीतों की स्वरलिपि व सी.डी. देने से पुस्तक का महत्त्व और बढ़ गया है।
—गोपाल चतुर्वेदी
इस पुस्तक में संस्कार सम्बन्धी उत्सवों के अवसरों पर गाए जानेवाले भोजपुरी लोकगीतों का सामाजिक मूल्यांकन तथा उनके संरक्षण और प्रचार-प्रसार में संचार माध्यमों विशेषकर दूरदर्शन, आकाशवाणी की भूमिका पर एक संक्षिप्त अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। कुछ लोकगीतों की स्वरलिपियाँ व धुनों की सी.डी. संलग्न हैं, जो संरक्षण की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।
—डॉ. विद्याविन्दु सिंह
शैलेश इन लोकगीतों को गाती नहीं, जीती हैं। इसलिए आधुनिकता के नाम पर लोकगीतों के विकृत स्वरूप उन्हें पीड़ा देते हैं। उनकी यह पुस्तक इस विकृति को समझने की उनकी एक सार्थक कोशिश है।
—विश्वनाथ सचदेव
शैलेश श्रीवास्तव पिछले अनेक वर्षों से बिना अपनी दुंदुभी बजाए हुए हिन्दी के लोकसंगीत प्रेमियों के बीच पाश्चात्य संस्कृति के अन्धानुकरण के चलते अपनी जड़ों से उखड़ लगभग विलुप्ति के कगार पर आ खड़े हुए संस्कार गीतों की जन-मानस में पुनर्प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्नशील हैं। बच्चे के जन्म पर गाए जानेवाले सोहर से लेकर मुंडन, छेदन, घुड़चढ़ी, लगुन भाँवरे; झूला (सावन), होली (फाग), टोना, नजर, सगुन, चैती, ठुमरी आदि सभी को उन्होंने अपना कंठ ही नहीं दिया है, बल्कि सुदूर गाँव-जवार के ओने-कोने की यात्राएँ कर उन्हें बड़ी-बूढ़ियों की कंठस्थ संचित पूँजी से बीन-चुन अपनी संगीत मंजूषा को निरन्तर समृद्ध भी किया है। प्रस्तुत शोध पुस्तक ‘भोजपुरी संस्कार गीत और प्रसार माध्यम’ उनकी श्रम-साध्य मेहनत का ही नतीजा है।
—चित्रा मुद्गल
21vin Sadi : Pahala Dasak
- Author Name:
Prabhash Joshi
- Book Type:

-
Description:
‘21वीं सदी : पहला दशक’ पुस्तक में विख्यात पत्रकार प्रभाष जोशी के वे लेख संकलित हैं जो उन्होंने ‘जनसत्ता’ दैनिक में सन् 2000 के बाद लिखे। 2001 से 2009 के बीच प्रकाशित इन लेखों में देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन की धड़कनें सुनी जा सकती हैं।
21वीं सदी के आगमन को सत्ताधारी वर्ग ने सम्पन्नता के स्वप्न के रूप में प्रचारित किया था। लेकिन सचाई यह थी कि 21वीं सदी देश के बहुजन जीवन के लिए अभिशाप की तरह प्रकट हुई। आर्थिक उदारीकरण की नीति के दुष्परिणाम सामने आने लगे। आम लोगों का जीवन पहले की तुलना में ज़्यादा मुश्किलों के घेरे में आ गया। इस पुस्तक में प्रभाष जोशी ने आर्थिक और सामाजिक स्तर पर पैदा होनेवाली इन मुश्किलों की व्याख्या विस्तार से की है। उसकी आत्महन्ता राजनीतिक परिणति को प्रभावी तरीक़े से समझाया गया है।
प्रभाष जोशी की पत्रकारिता महज़ चिन्तन और विश्लेषण की पत्रकारिता नहीं है, वह सामाजिक सक्रियता और विसंगतियों के विरुद्ध हस्तक्षेप की पत्रकारिता है। इन लेखों में एक शोषणमुक्त भारतीय समाज का स्वप्न भी देखा गया है, जिसमें एक नए विकल्प का संकेत भी दिखाई देता है। यह पुस्तक नई सदी की वास्तविक पहचान का रेखाचित्र है।
Jansanchar Madhyam Aur Vishesh Lekhan (Swaroop Aur Prakar)
- Author Name:
Niranjan Sahay
- Book Type:

-
Description:
आज हम ऐसे दौर में हैं जब पलक झपकते हम हजारों मील दूर बैठे परिचित से चेहरा देखते हुए बात कर सकते हैं, जिसे सम्भव किया है इंटरनेट और सूचना क्रान्ति के नूतन आविष्कार 'वीडियो कॉल' ने, जिसमें डाटा एक सेकेंड से भी कम समय में वह दूरी तय कर लेता है।
संचार के इतिहास में कई महत्त्वपूर्ण पड़ाव आए हैं। हमने बोलने के साथ-साथ गाना सीखा, विभिन्न वाद्य यंत्र बनाए एवं संगीत की रचना की। पहले पत्तों पर लिखना सीखा और फिर काग़ज़ का निर्माण हुआ, जिससे लिखे गए को संरक्षित रखना सम्भव हुआ। पन्द्रहवीं सदी में छापेखाने के आविष्कार ने वह रास्ता दिखाया, जिससे अखबार और किताब लाखों-करोड़ों लोगों तक पहुँच सकें। टेलीग्राफ की तारों से कोई भी लिखित सन्देश चन्द मिनटों में अपनी मंजिल तक पहुँचने लगा। टेलीफोन से हम एक-दूसरे से एक ही समय पर दूर बैठकर बात करने में सक्षम हुए।
हजारों वर्षों के इस तकनीकी कालक्रम में जो एक चीज समान रही है वह है—अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने की आवश्यकता। आदि मानव इशारों से एक-दूजे को खतरे की चेतावनी देते थे, तो हम आज विभिन्न प्रयोजनों के लिए लिखित से लेकर वीडियो सन्देश और कॉन्फ्रेंसिंग तक कर लेते हैं। संचार अपने विचारों और जरूरतों को इसी तरह दूसरों तक पहुँचाने का काम है।
संचारशास्त्र के जाने-माने प्रणेता हैरॉल्ड लैसवेल के अनुसार, संचार प्रक्रिया का सार है कि किसने किससे किस माध्यम द्वारा क्या कहा और उसका (यानी कहे गए का) क्या प्रभाव पड़ा? यह पुस्तक संचार, जनसंचार और उनके विभिन्न पहलुओं की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करती है।
Patrakarita : Naya Daur, Naye Pratiman
- Author Name:
Santosh Bhartiya
- Book Type:

-
Description:
संतोष भारतीय ने महत्त्वपूर्ण पत्रकारिता की है। वे कुशल संवाददाता रहे हैं और ‘चौथी दुनिया’ से सम्पादन की निपुणता भी दिखा चुके हैं। मगर फ़ैज़ के भाव में ‘कुछ इश्क़ किया कुछ काम किया’ की उधेड़बुन के चलते शायद वे कहीं ठहर-से गए। राजनीति की तरफ़ वे ज़्यादा न झुकते तो और सार्थक काम करते। बहरहाल, उनकी किताब ‘पत्रकारिता : नया दौर, नए प्रतिमान’ सिरे से पढ़ने के क़ाबिल है। इसमें उनके ‘रविवार’ और ‘चौथी दुनिया’ के दिनों के संस्मरण हैं, अपने रपट-रिपोर्ताज हैं और साथ में सम्पादक-उपसम्पादक और संवाददाता आदि की ज़िम्मेवारियों का विवेचन है। इस तरह एक मायने में किताब पत्रकारिता की पाठ्य-पुस्तक बन गई है। साफ़गोई और बेबाक टिप्पणियों के लिए यह किताब अलग से जानी जाएगी। हालाँकि उनके कुछ निष्कर्ष भावुकता-भरे हैं, कुछ से आप शायद सहमत न हों। पर वे बहुत दिलचस्प हैं और हमें हिन्दी पत्रकारिता के एक अहम दौर की घटनाओं पर फिर से सोचने को उकसाते हैं।
—ओम थानवी
Apne Gireban Mein
- Author Name:
Yashwant Vyas
- Book Type:

-
Description:
कोई जमाना था जब दिल्ली से निकलने वाले अखबार राष्ट्रीय और लखनऊ-लुधियाना से निकलने वाले अखबार क्षेत्रीय कहे जाते थे। हिंदी अखबारों की दुनिया इस बीच बहुत बदल चुकी है। सैटेलाइट संस्करणों ने जो महादृश्य उपस्थित किया है उसने हिंदी अखबारों की बाजार शक्ति की नए सिरे से पहचान कराई है। पारंपरिक अर्थ में गढ़ कहे जाने वाले, ध्वस्त हो रहे हैं। संपादक और स्वामी के पारस्परिक रिश्तों ने नई शक्ल ले ली है। जबर्दस्त पूँजी निवेश, आक्रामक बाजार नीति तथा पत्रकारिक फैशन परेड का नया पैकेज सामने आ रहा है। प्रसार की उछाल में पाठक के लिए नए विकल्प खुले हैं। लेकिन क्या यह नई दुनिया सचमुच एक अद्भुत दुनिया है?
एक रचनाकार होने के साथ-साथ, पत्रकारिता की उसी बदलती हुई दुनिया के अनुभव का हिस्सा होते हुए यशवंत व्यास जब क्षेत्रीय पत्रकारिता में बदलाव को आँकते हैं तो उनकी दृष्टि गहरी संवेदना से युक्त होती है। वे निरंतर हो रहे परिवर्तनों को गहन अनुभूतियों तथा स्पष्ट तथ्यों के बीच दर्ज करते हैं। इसके लिए वे न सिर्फ भाषा के स्तर पर बल्कि प्रस्तुति पर भी शोध को नया, ताज़गी-भरा आकार देते हैं। अंतर्विरोधों की पहचान के प्रति पैनी दृष्टि तथा क्षेत्रीय पत्रकारिता में सफलता असफलता की गंभीर पड़ताल करने की कोशिशों जैसी खूबियों के चलते ‘अपने गिरेबान’ में समकालीन क्षेत्रीय हिंदी पत्रकारिता पर एक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है।
Media Aur Bazarvad
- Author Name:
Ramsharan Joshi
- Book Type:

- Description: बाज़ार नाम की संस्था आदिम समाज के लिए भी रही है, और आज के समाज के लिए भी है। इसलिए बाज़ार से बैर करके आप अपना समाज और अपना जीवन चला सकें, इसकी सम्भावना नहीं है। लेकिन जब बाज़ार मनुष्य की नियति तय करे तो इसका मतलब यह है कि अब तक जो मनुष्य का सेवक रहा है, वह मनुष्य का मालिक होना चाहिए। बाज़ार मनुष्य का बहुत अच्छा सेवक है। कोई पाँच हज़ार साल से उसकी सेवा कर रहा है। शायद उससे भी ज़्यादा वर्षों से कर रहा हो। अगर वो मनुष्य की नियति तय करेगा तो उसमें एक मूल खोट आनेवाला है, क्योंकि बाज़ार भाव से चलता है, बाज़ार मूल्य से नहीं चलता और मूल्यों के बिना किसी भी मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव समाज भाव से नहीं चल सकता, मूल्य से ही चल सकता है। मानव समाज को मूल्य से चलना है। अब जो बाज़ार की शक्तियाँ दुनिया में इकट्ठा हुई हैं उनसे आप कैसे निपटेंगे? मुझे कई लोगों ने कहा कि यह तो हिन्दुस्तान है जो जाजम की तरह बिछने के लिए तैयार है, नहीं तो जहाँ-जहाँ बाज़ार गया है, वह उस देश के समाज की शर्तों पर गया है। पर हमने एक कमज़ोर देश की तरह से अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार को स्वीकारा है। इसलिए अब हमारे यहाँ जाजम की तरह बिछ जाने का लगभग कुचक्र चल रहा है!
Anchalik Samwaddata
- Author Name:
Suresh Pandit
- Book Type:

- Description: लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के बावजूद संचार के विकेन्द्रीकरण का मुद्दा अभी विमर्श का विषय नहीं बन सका है। इसके बिना लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सफलता भी आंशिक ही रहेगी। जब ज्ञान और सूचना को शक्ति माना जाता है तो भला केन्द्रीकृत सूचना-व्यवस्था से विकेन्द्रीकृत शासन-व्यवस्था की आशा कैसे की जा सकती है! जनता के क़रीब के शासकीय पायदानों अर्थात् पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर निकायों और गाँवों तथा क़स्बों के समाचारों की महत्ता अख़बारों में बढ़े, तो ही विकेन्द्रित सत्ता का सही आभास हो पाएगा। राजधानी और बड़े शहरों की चमक-दमक-भरे समाचारों को उनका सही स्थान दिखा देने की ज़रूरत है। यह तभी सम्भव है जब कुशल आंचलिक संवाददाता ग्रामीण समाज और नवीन विकेन्द्रीकृत व्यवस्था पर केन्द्रित अच्छे समाचारों को प्रकाशन के लिए भेज सकें जिनमें लोगों के दिल की धड़कन सुनाई पड़े। इसके सामने राज्य और केन्द्र की सत्ता तथा शहर की चमकीली छवि भी फीकी पड़ जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में आंचलिक संवाददाता की मदद के लिए तैयार की गई यह पुस्तक बहुत प्रासंगिक है। निश्चय ही यह पुस्तक कुशल आंचलिक संवाददाता तैयार करने और उनके निरन्तर विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेगी।
Sanchar Bhasha Hindi
- Author Name:
Dr. Surya Prasad Dixit
- Book Type:

-
Description:
जनसंचार माध्यमों की सबसे बड़ी शक्ति है, संचार भाषा। मीडिया द्वारा प्रसारित भाषा में लक्ष्यीभूत श्रोता, दर्शक, पाठक विभिन्न बौद्धिक स्तरों के होते हैं। जन-माध्यमों का यह प्रयास होता है कि वे भाषिक सम्प्रेषण को सर्व सुलभ बनाएँ। इसके लिए एक-एक शब्द को बड़ी सावधानी के साथ प्रयुक्त करना होता है। यह ध्यान रखना होता है कि उच्चरित भाषा में कितना अन्तराल, कितना आयतन, कितना आरोहावरोह और कितना यति-गति-विधान रखा जाए। इन जन-माध्यमों की अपनी अलग-अलग भाषिक प्रोक्तियाँ होती हैं। अख़बार भरसक जन-भाषा का प्रयोग करता है, रेडियो उसे ‘विजुअल’ बनाने का प्रयास करता है और टेलीविज़न दृश्य भाषा का पूरी क्षमता के साथ निर्वाह करता है।
इधर कम्प्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि ने भाषा के नए-नए रूप निकाले हैं। इन्हें समझने के लिए भाषा प्रौद्योगिकी का संज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए अपेक्षित है—अनुवाद कला का अभ्यास, डबिंग, दुभाषिया प्रविधि और वाचिक कलाओं की जानकारी, कमेंट्री, उद्घोषणा तथा संचालन की सफलता पूर्णत: भाषिक उच्चारण और लहज़े पर निर्भर होती है। समाचार, फ़ीचर, ध्वनि नाटक, संवाद, वार्त्ता, वृत्तचित्र, रिपोर्ताज़ आदि विधाएँ मूलत: भाषिक प्रयोगों पर निर्भर होती हैं।
संचार भाषा में सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है शब्द संवेदना पर। उसी के सहारे विज्ञापन के नारे इतने हृदयस्पर्शी सिद्ध होते हैं।
इस कृति में प्रथम बार संचार भाषा रूप में हिन्दी का अनुप्रयोग स्पष्ट किया गया है। कहना न होगा कि यह कृति प्रत्येक संचारकर्मी के लिए मात्र उपादेय ही नहीं, बल्कि अपरिहार्य है।
Customer Reviews
Be the first to write a review...
0 out of 5
Book