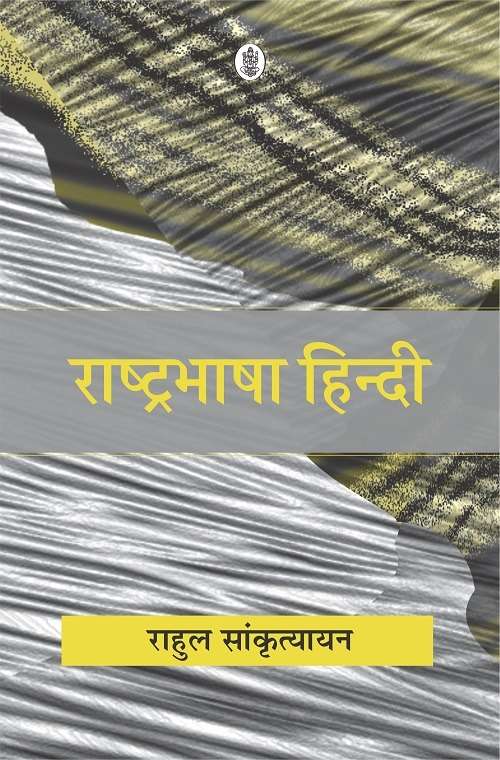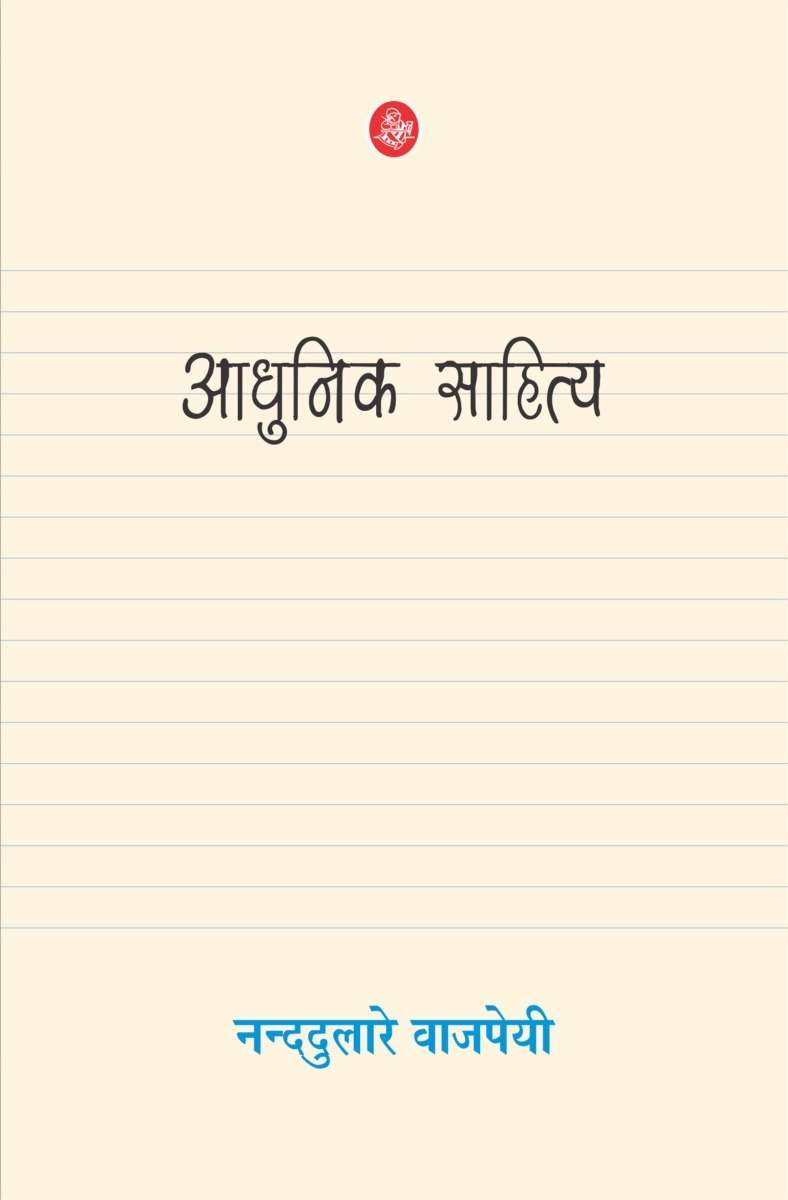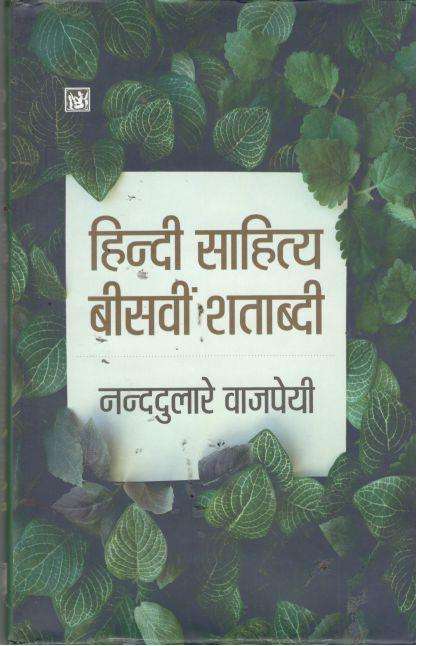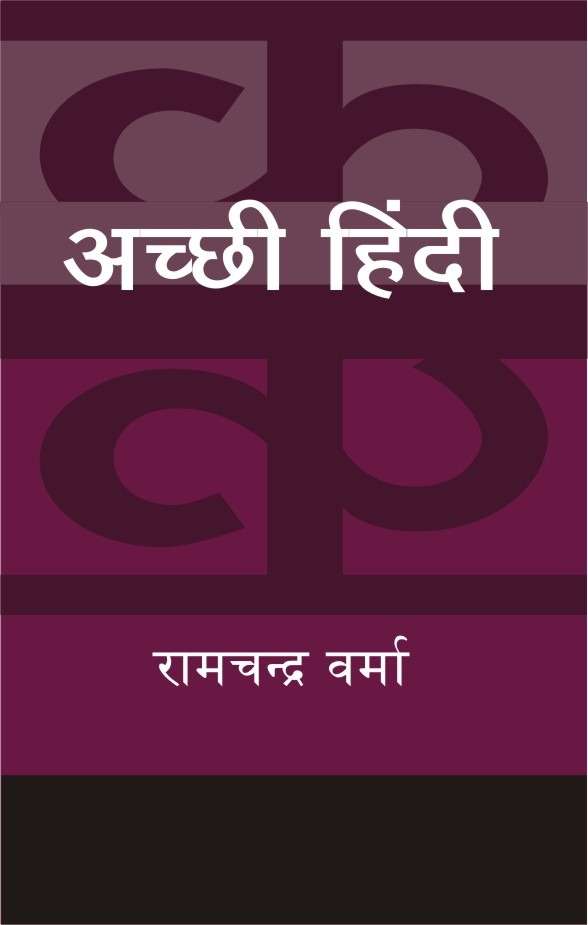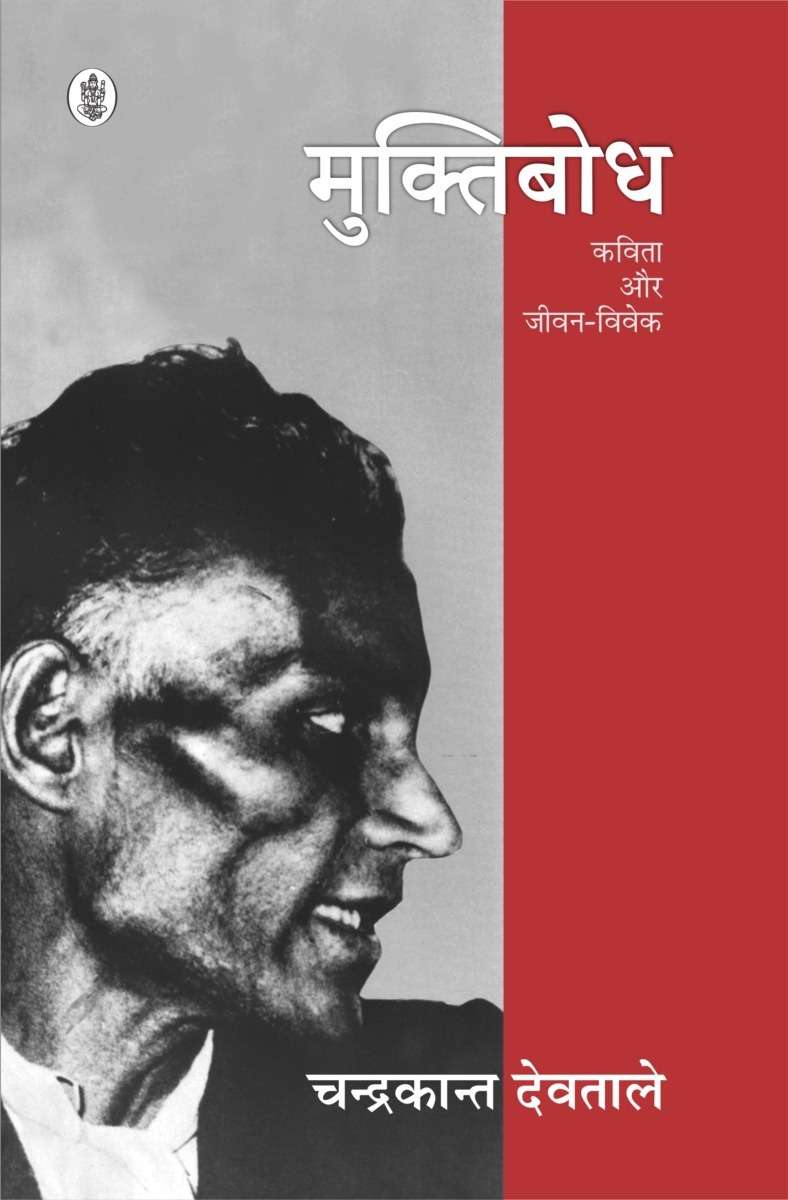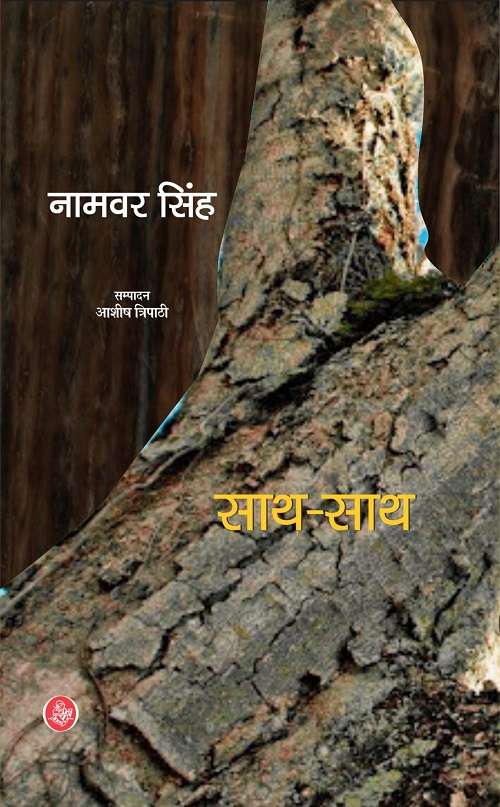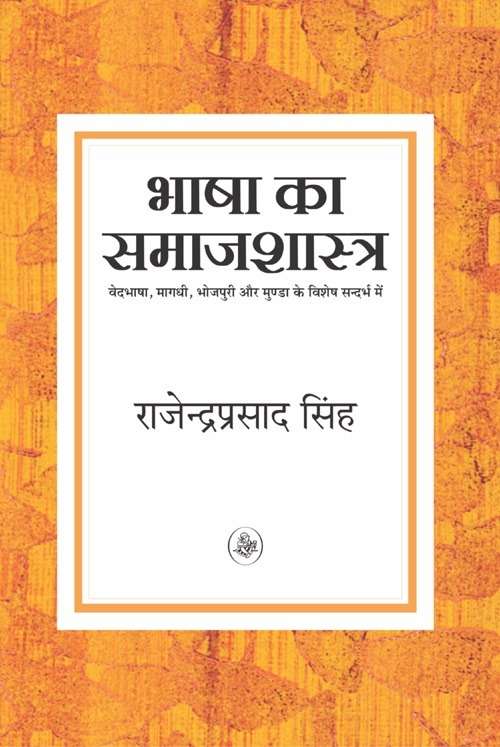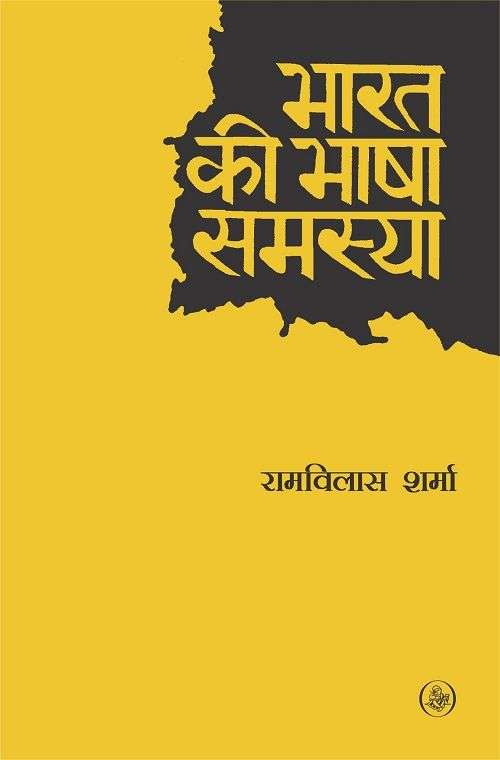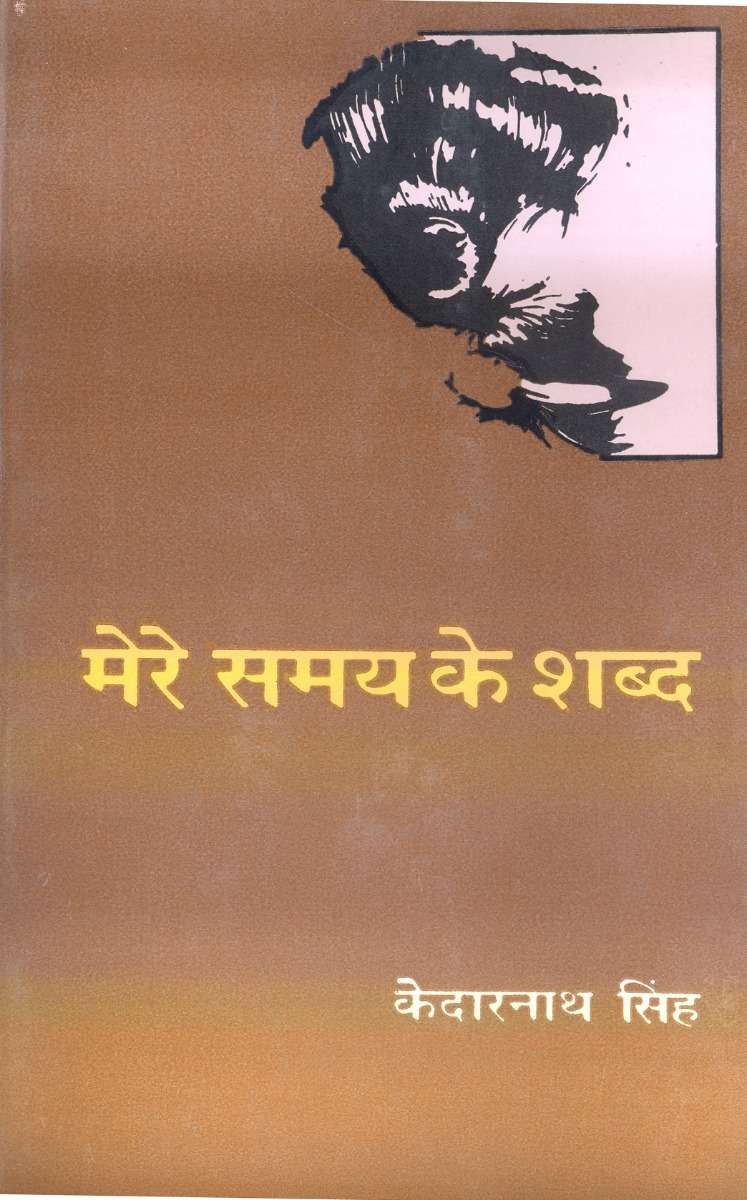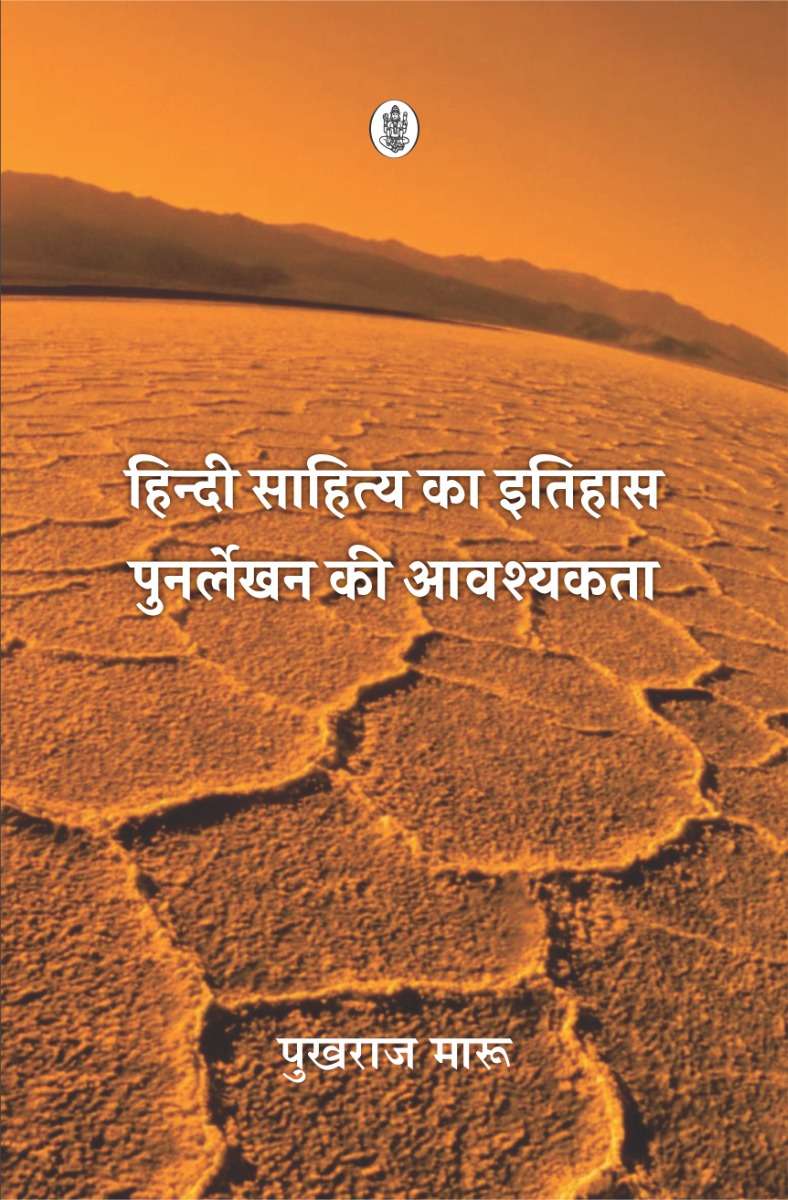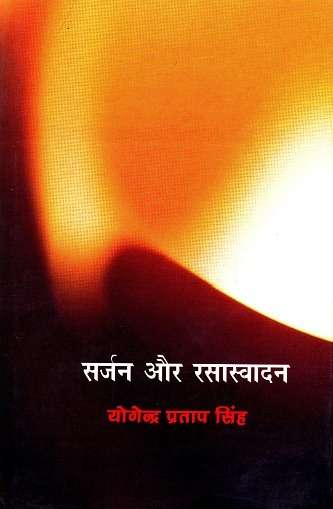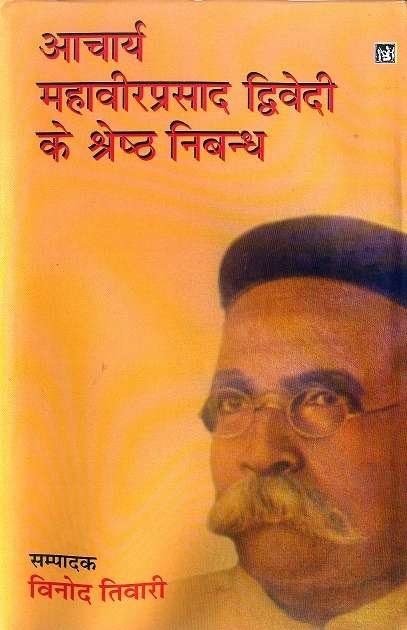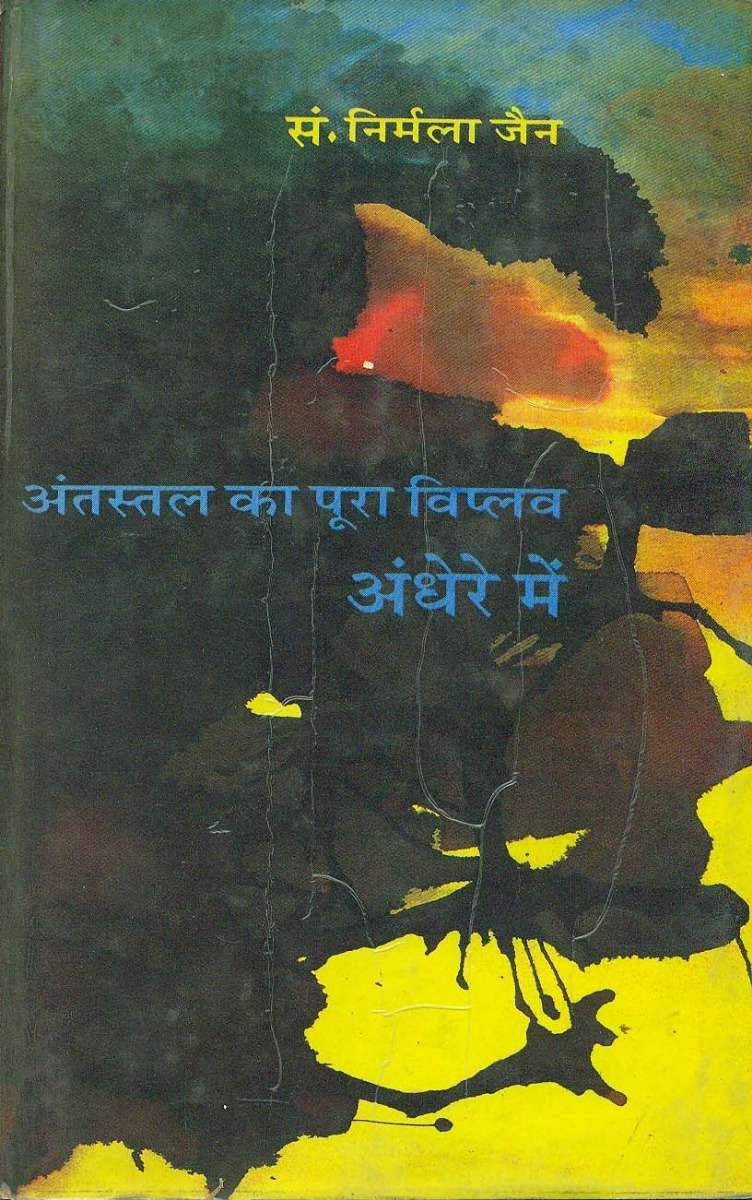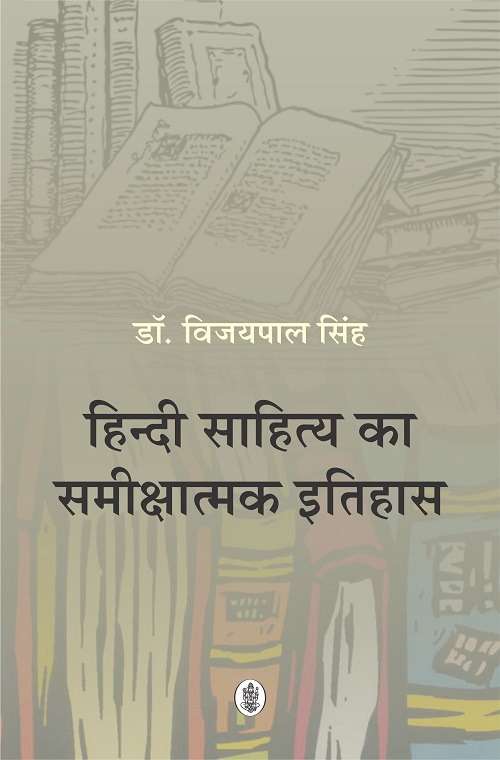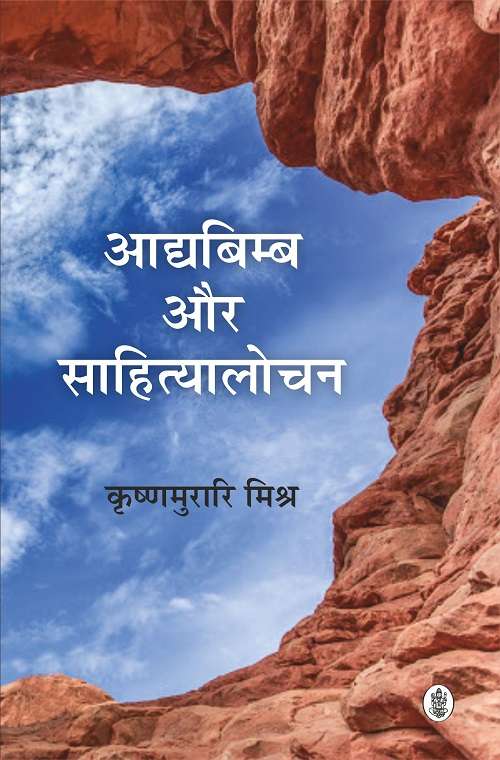
Aadyabimb Aur Sahityalochan
Author:
Krishna Murari MishraPublisher:
Rajkamal Prakashan SamuhLanguage:
HindiCategory:
Language-linguistics0 Ratings
Price: ₹ 636
₹
795
Available
प्रोफ़ेसर कृष्णमुरारि मिश्र आधुनिक हिन्दी आलोचना के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। हिन्दी में आद्यबिम्बात्मक आलोचना के प्रवर्तन का श्रेय उन्हें प्राप्त है। साहित्यिक कृतियों की संरचनात्मक गहनताओं की व्याख्या और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए उन्हें विशेष ख्याति मिली है। ‘आद्यबिम्ब और साहित्यालोचन’ शीर्षक उनका प्रस्तुत ग्रन्थ इस आलोचना के सिद्धान्त और सम्प्रयोग से सम्बद्ध है। ग्रन्थ में तीन शीर्षक ग्रंथित हैं—'आद्यबिम्ब', 'आद्यबिम्ब और साहित्यालोचन : आधार' तथा ' आद्यबिम्ब और साहित्यालोचन : स्वरूप'।</p>
<p>'आद्यबिम्ब' शीर्षक के अन्तर्गत आद्यबिम्ब की युगीय धारणा का सैद्धान्तिक विवेचन है। इसमें फ़्रायड और युग की धारणाओं के मूलभूत अन्तर का हिन्दी में पहली बार उद्घाटन है। साथ ही आद्यबिम्ब की युगीय धारणा का सारभूत आख्यान है जिसमें यौगपत्य के अल्पज्ञात वैज्ञानिक सिद्धान्त की भी चर्चा है। 'आद्यबिम्ब और साहित्यालोचन : आधार' शीर्षक से मुख्यतया युग के कला-चिन्तन का विवेचन है। आद्यबिम्बात्मक आलोचना की सैद्धान्तिकी के इस विवेचन से सिद्ध है कि युग का कला-चिन्तन हमारे भारतीय साहित्य-चिन्तन के लिए विजातीय नहीं है। वह भारतीय साहित्यशास्त्र के कालसिद्ध निकषों का पोषक है। युग की कलाविषयक धारणाएँ रससिद्धान्त और ध्वनिसिद्धान्त के बहुत निकट हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य-हेतु के रूप में प्रतिभा के जिस स्वरूप की स्थापना की गई है, वह सामूहिक अचेतन की युगीय धारणा के निकट है। सर्जक के व्यक्तित्व की असाधारणता को भारतीय आचार्यों के समान युग ने भी मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। भारतीय आचार्यों के समान युग ने भी काव्य की लोकमंगलकारिणी शक्ति पर बल दिया है। उन्होंने सर्जक, भावक और समाज के सन्दर्भ में काव्य के माध्यम से जिस आत्मोपलब्धि का उल्लेख किया है, उसमें आनन्द और लोकमंगल दोनों का समावेश है। 'आद्यबिम्ब और साहित्यालोचन : स्वरूप' शीर्षक के अन्तर्गत हिन्दी की आद्यबिम्बात्मक आलोचना के स्वरूप की सम्यक् विवृत्ति है।</p>
<p>आशा है, यह ग्रन्थ भी उनके पूर्व प्रकाशित ग्रन्थों की तरह हिन्दी में समादृत होगा।
ISBN: 9788183615846
Pages: 219
Avg Reading Time: 7 hrs
Age: 18+
Country of Origin: India
Recommended For You
Rashtrabhasha Hindi
- Author Name:
Rahul Sankrityayan
- Book Type:

-
Description:
इस पुस्तक में राहुल जी के भाषा-सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण लेखों और भाषणों को संकलित किया गया है, जिनमें उन्होंने सामान्यत: भारत की भाषा-समस्या और विशेषत: हिन्दी पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।
कहने की ज़रूरत नहीं कि भाषा-सम्बन्धी जो सवाल पचास साल पहले हमारे सामने थे, वे कमोबेश आज भी जस के तस हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही उग्र हुए हैं। मसलन अंग्रेज़ी का मसला, जिसने व्यवहार में राष्ट्रभाषा हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को दूसरे-तीसरे दर्जे पर पहुँचा दिया है। इसके अलावा वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली की समस्या है, जिस पर अभी भी काफ़ी काम किए जाने की ज़रूरत है। राहुल जी इन निबन्धों में इन सभी बिन्दुओं पर गहराई और अधिकार के साथ विचार करते हैं। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर स्थापित करने की पैरवी करते हुए वे अन्य भारतीय भाषाओं को भी उनका उचित और सम्मानित स्थान दिए जाने की ज़रूरत महसूस करते हैं। उनका सुझाव है कि हरेक बालक-बालिका को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, और सारे देश में जहाँ भी निर्धारित अल्पमत संख्या में विद्यार्थी मिलें, वहाँ उनके लिए अपनी भाषा के स्कूल खोलने चाहिए।
इसके अलावा हिन्दी की संरचना, विकास, साहित्य और इतिहास आदि अनेक पहलुओं पर राहुल जी के स्पष्ट विचार इन निबन्धों में संकलित हैं।
Aadhunik Sahitya
- Author Name:
Nandulare Vajpeyi
- Book Type:

-
Description:
‘आधुनिक साहित्य’ आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी के निबन्धों का संग्रह है। इसमें सम्मिलित निबन्धों में सन् 1930 से 1942 तक की कालावधि के हिन्दी साहित्य की मुख्य कृतियों और प्रवृत्तियों का विवेचन किया गया है। कुछ अन्य प्रासंगिक निबन्ध भी इसमें जोड़ दिए गए हैं, जो विषय पर भिन्न दिशा और भूमि से प्रकाश डालते हैं। लेकिन जैसाकि स्वयं वाजपेयी जी अपनी भूमिका में कहते हैं : “पुस्तक में इस सामग्री के रहते हुए भी इसे उस समय का साहित्यिक इतिहास नहीं कहा जा सकता। इसका निर्माण इतिहास से भिन्न प्रणाली और प्रेरणा से किया गया है।”
वाजपेयी जी आगे कहते हैं : “मेरी ये समीक्षाएँ और निबन्ध निर्माण की पगडंडियाँ हैं; इतिहास वह ‘रोलर’ है, जो इन अथवा इन जैसी अन्य पगडंडियों को समतल कर प्रशस्त पथ बनाता है। जब तक विविध दृष्टियों और उपादानों को लेकर अच्छे परिमाण में साहित्यिक समीक्षाएँ नहीं प्रस्तुत की जातीं, तब तक इतिहास-लेखन का कार्य वस्तुतः सम्भव नहीं है। ‘हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी’ के साथ ‘आधुनिक साहित्य’ के ये पूरक निबन्ध यदि नई साहित्यिक रुचि और दृष्टि के निर्माण में कुछ भी योग दे सकें, तो यह इनकी सफलता होगी।”
इस पुस्तक में शामिल निबन्ध अपने विषय-काल के साहित्य की एक विहंगम तस्वीर पाठक के सामने प्रस्तुत करते हैं और साहित्येतिहास की दिशा में उन्मुख होनेवाले विद्वज्जनों को एक आधार मुहैया कराते हैं।
Hindi Sahitya Beesvin Shatabdi
- Author Name:
Nandulare Vajpeyi
- Book Type:

-
Description:
यह पुस्तक निबन्धों का संग्रह है। प्रस्तुत पुस्तक में प्रारम्भिक चालीस वर्षों के ही कुछ प्रमुख साहित्यिक व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। यद्यपि इस समय के सभी प्रमुख साहित्यकार पुस्तक में नहीं आ सके हैं, परन्तु जितने आए हैं, उतने ही इस काल के साहित्य के स्वरूप, उसकी समृद्धि-सीमा और उसकी विकास-दिशा को दिखा देने के लिए पर्याप्त है।
बीसवीं शताब्दी के साहित्य की जिस सामान्य रूपरेखा का उल्लेख किया गया, उससे इस साहित्य का विस्तार और इसकी अनेकरूपता तो प्रकट हुई ही, उसके आलोचन-कार्य को पेचीदगी का भी कुछ-न-कुछ आभास मिला। इन निबन्धों में इस युग के साहित्य की समीक्षा का प्राथमिक प्रयास किया गया है। इसके पहले इस विषय की कोई व्यवस्थित सामग्री उपलब्ध न थी।
ये निबन्ध किसी नियमित क्रम या शैली पर नहीं लिखे गए हैं। लेखकों की सम्पूर्ण रचनाओं को सब समय सामने नहीं रखा गया है। कहीं-कहीं तो किसी एक ही रचना पर पूरा निबन्ध आधारित है (यद्यपि ऐसे निबन्धों में लेखक की अन्य रचनाएँ भी अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान में रही हैं) किसी निबन्ध में किसी लेखक पर प्रशंसात्मक चर्चा की गई है और किसी अन्य पर विरोधी ढंग से लिखा गया है। जिनकी आवश्यकता से अधिक प्रशंसा हो रही थी, उनके सम्बन्ध में दूसरे पक्ष को सामने रखा गया है। इसमें लक्ष्य लेखकों की स्थिति में सामंजस्य स्थापित करने का रहा है। किन्तु प्रशंसा या अप्रशंसा द्वारा भी रचयिता के व्यक्तित्व को सीमित और साकार करने की चेष्टा ही मुख्य रही है। इस प्रकार अनुकूल या प्रतिकूल विवेचन से लेखकों की वास्तविक रचना-क्षमता ही स्पष्ट हुई है।
Achhi Hindi
- Author Name:
Ramchandra Verma
- Book Type:

- Description: आज-कल देश में हिन्दी का जितना अधिक मान है और उसके प्रति जन-साधारण का जितना अधिक अनुराग है, उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारी भाषा सचमुच राष्ट्र-भाषा के पद पर आसीन होती जा रही है। लोग गला फाड़कर चिल्लाते हैं कि राज-काज में, रेडियो में, देशी रियासतों में सब जगह हिन्दी का प्रचार करना चाहिए, पर वे कभी आँख उठाकर यह नहीं देखते कि हम स्वयं कैसी हिन्दी लिखते हैं। मैं ऐसे लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि, हमारी भाषा में उच्छृंखलता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। किसी को हमारी भाषा का कलेवर विकृत करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। देह के अनेक ऐसे प्रान्तों में हिन्दी का ज़ोरों से प्रचार हो रहा है, जहाँ की मात्र-भाषा हिन्दी नहीं है। अतः हिन्दी का स्वरूप निश्चित और स्थिर करने का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व उत्तर भारत के हिन्दी लेखकों पर ही है। उन्हें यह सोचना चाहिए कि हमारी लिखी हुई भद्दी, अशुद्ध और बे-मुहावरे भाषा का अन्य प्रान्तवालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और भाषा के क्षेत्र में हमारा यह पतन उन लोगों को कहाँ ले जाकर पटकेगा। इसी बात का ध्यान रखते हुए पूज्य अम्बिका प्रसाद जी वाजपेयी ने कुछ दिन पहले हिन्दी के एक प्रसिद्ध लेखक और प्रचारक से कहा था, "आप अन्य प्रान्तों के निवासियों को हिन्दी पढ़ा रहे हैं और उन्हें अपना व्याकरण भी दे रहे हैं, पर जल्दी ही वह समय आएगा, जबकि वही लोग आपके ही व्यकारण से आपकी भूल दिखाएँगे!" यह मानो भाषा की अशुद्धियों वाले व्यापक तत्त्व की और गूढ़ संकेत था। जब हमारी समझ में यह तत्त्व अच्छी तरह आ जाएगा, तब हम भाषा लिखने में बहुत सचेत होने लगेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारी भाषा की वास्तविक उन्नति का आरम्भ भी उसी दिन से होगा। भाषा वह साधन है, जिससे हम अपने मन के भाव दूसरों पर प्रकट करते हैं। वस्तुतः यह मन के भाव प्रकट करने का ढंग या प्रकार मात्र है। अपने परम प्रचलित और सीमित अर्थ में भाषा के अन्तर्गत वे सार्थक शब्द भी आते हैं, जो हम बोलते हैं और उन शब्दों के वे क्रम भी आते हैं, जो हम लगाते हैं। हमारे मन में समय-समय पर विचार, भाव, इच्छाएँ, अनुभूतियाँ आदि उत्पन्न होती हैं, वही हम अपनी भाषा के द्वारा, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, चाहे किसी संकेत से दूसरों पर प्रकट करते हैं, कभी-कभी हम अपने मुख की कुछ विशेष प्रकार की आकृति बनाकर या भावभंगी आदि से भी अपने विचार और भाव एक सीमा तक प्रकट करते हैं, पर भाव प्रकट करने के ये सब प्रकार हमारे विचार प्रकट करने में उतने अधिक सहायक नहीं होते, जितनी बोली जानेवाली भाषा होती है। यह ठीक है कि कुछ चरम अवस्थाओं में मन का कोई विशेष भाव किसी अवसर पर मूक रहकर या फिर कुछ विशिष्ट मुद्राओं से प्रकट किया जाता है और इसीलिए 'मूक अभिनय' भी 'अभिनय' का एक उत्कृष्ट प्रकार माना जाता है। पर साधारणतः मन के भाव प्रकट करने का सबसे अच्छा, सुगम और सब लोगों के लिए सुलभ उपाय भाषा ही है।
Kutaz
- Author Name:
Hazariprasad Dwivedi
- Book Type:

- Description: आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी भारतीय मनीषा के प्रतीक और साहित्य एवं संस्कृति के अप्रतिम व्याख्याकार माने जाते हैं और उनकी मूल निष्ठा भारत की पुरानी संस्कृति में है लेकिन उनकी रचनाओं में आधुनिकता के साथ भी आश्चर्यजनक सामंजस्य पाया जाता है। ‘हिन्दी साहित्य की भूमिका’ और ‘बाणभट्ट की आत्मकथा’ जैसी यशस्वी कृतियों के प्रणेता आचार्य द्विवेदी को उनके निबन्धों के लिए भी विशेष ख्याति मिली। निबन्धों में विषयानुसार शैली का प्रयोग करने में इन्हें अद्भुत क्षमता प्राप्त है। तत्सम शब्दों के साथ ठेठ ग्रामीण जीवन के शब्दों का सार्थक प्रयोग इनकी शैली का विशेष गुण है। भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष और विभिन्न धर्मों का उन्होंने गम्भीर अध्ययन किया है जिसकी झलक पुस्तक में संकलित इन निबन्धों में मिलती है। छोटी-छोटी चीज़ों, विषयों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन और विश्लेषण-विवेचन उनकी निबन्ध-कला का विशिष्ट व मौलिक गुण है। निश्चय ही उनके निबन्धों का यह संग्रह पाठकों के लिए न केवल पठनीय है बल्कि उनकी सोच को एक रचनात्मक आयाम भी प्रदान करता है।
Muktibodh : Kavita Aur Jeevan Vivek
- Author Name:
Chandrakant Devtale
- Book Type:

-
Description:
मुक्तिबोध प्रथमत: और अन्तत: कवि थे। जिस तरह उन्होंने अपने विचार को कविता में लाने के लिए आन्तरिक संघर्ष किया, उसी तरह अपने जीवनानुभूतियों को भी अपनी कला में रूपान्तरित किया। उनका व्यक्तित्व जिन तत्त्वों से निर्मित हुआ है, उनके सरलीकृत, वर्गीकृत और सुविधावादी विश्लेषण से हम सही निष्कर्षों तक नहीं पहुँच सकते हैं।
इस पुस्तक का उद्देश्य मुक्तिबोध के लगभग मिथक बन चुके जीवन और व्यक्तित्व को खोलना नहीं, बल्कि समझना है। उनका काव्य और चिन्तन उनके व्यक्तित्व और जीवन से दूर-दूर तक प्रभावित है, लेकिन इस प्रभाव को किसी यांत्रिक रिश्ते के आधार पर रेखांकित करना न तो सम्भव है, और न उचित ही। उन्होंने अपने दु:ख को निजी मर्सिया की शक्ल में कहीं भी नहीं लिखा है, उनके जीवन में झाँककर उनकी कष्टपूर्ण स्थितियों को मानवीय पीड़ा के व्यापक रूप में कविताओं में देखना एक रोमांचक अनुभव है। यह पुस्तक मुक्तिबोध के जीवन और व्यक्तित्व की रेखाओं को उनके अन्तर्विरोधों सहित पहचानने का प्रयत्न करती है।
कवि चन्द्रकान्त देवताले मुक्तिबोध के जीवन और उनकी कविता में लम्बे समय से दिलचस्पी लेते रहे हैं; यह पुस्तक इसी का नतीजा है। अपनी भूमिका में वे कहते हैं : “मैं समझता हूँ मुक्तिबोध जैसे कवि और बेहद सचेत मनुष्य की कविताओं और उनके विचारों का आकलन एक और अन्तिम बार का कार्य नहीं है। कवि के प्रति अपने आत्मीय लगाव के साथ ही मैंने उन्हें समझने की कोशिश की। पर यह आत्मीय लगाव इस अर्थ में कहीं बन्धनकारी नहीं रहा कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ, उसे कहने में संकोच करूँ।”
Sath-Sath
- Author Name:
Namvar Singh
- Book Type:

-
Description:
‘साथ-साथ’ मुख्यतः परिसंवादों का संकलन है। इन परिसंवादों में नामवर सिंह एक पक्ष के रूप में शामिल हुए हैं। परिसंवाद उपनिषदों और संगीतियों की परम्परा का ही आधुनिक रूप है। संवाद का सर्वाधिक लोकतांत्रिक रूप। इसमें वक्ता को वार्ताकारों के अन्य पक्षों के साथ अपनी बात कहनी होती है। यह एक तरह की बहुपक्षी जुगलबन्दी है।
पुस्तक में चार परिचर्चाएँ हैं। इनसे गुज़रते हुए हम सहज ही देख पाते हैं कि आलोचक के रूप में नामवर सिंह ‘संवाद’ को कितना महत्त्व देते थे। साथी वार्ताकारों के व्यक्तित्व और विचारों को पूरी विनम्रता के साथ सुनना, उनकी उपस्थिति को स्वीकारना और उनके विचारों को ‘लोकतांत्रिक’ जगह के भीतर ही तर्क-वितर्क की परिधि में लाना—उनके संवादी व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा था। सभी संवादों को एक साथ देखने पर हम पाते हैं, ये किसी एक विषय से बँधे नहीं हैं। बातचीत का समय भी दूर तक फैला हुआ है। इस अर्थ में यह पुस्तक एक राग-माला की तरह है। हिन्दी आलोचना के अनेक पक्षों के बीच नामवर जी की पक्षधरताएँ यहाँ स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई हैं।
पुस्तक में विशेष महत्त्व के दो साक्षात्कार सम्मिलित हैं। पहला साक्षात्कार रामविलास शर्मा से लिया गया है। रामविलास शर्मा से दूसरी बातचीत एक परिचर्चा है। पहली बातचीत के क्रम में इसे पढ़ने पर अनेक ऐतिहासिक बहसों के सन्दर्भ में रामविलास शर्मा और नामवर सिंह की वैचारिक स्थिति स्पष्ट होती है। इस बातचीत से वामपंथी बुद्धिजीवियों के बीच मौजूद स्वस्थ लोकतांत्रिकता और ईमानदार बहस-धर्मिता सामने आती है। स्पष्ट होता है कि हमारे समय में क्षीण हो रहे इस निर्भय आलोचनात्मक विवेक के बग़ैर वामपंथी विचार परम्परा का विकास नहीं हो सकता है।
Bhasha Ka Samajshastra
- Author Name:
Rajendra Prasad Singh
- Book Type:

- Description: वेदों में ‘मनुष्य’ और ‘मानुष’ एक साथ कैसे चलते हैं? कौन किसका अपभ्रंश है? अगर मनुष्य में षष्ठी विभक्ति है तो मानुष में कौन-सी विभक्ति है जिसके बलबूते पहले की व्युत्पत्ति मनु की सन्तति की जाती है? वैदिक ‘मान’ का अर्थ है घर, जो घर में रहता है, वह ‘मानुष’ है और जो वन में रहता है, वह ‘वनमानुष’ है; इसीलिए ‘वनमनुष्य’ पद नहीं चलता है। हिन्दी भाषी क्षेत्र की लोकबोलियों में मानुस शब्द चलता है, मनुष्य नहीं। इसलिए यह दावा करना कि लोकबोलियों के सभी शब्द संस्कृत के अपभ्रंश हैं, ग़लत होगा। भोजपुरी में जानवरों की माँद को आज भी मान/मनान कहा जाता है। लोकबोलियों में मनुष्य को ‘मनई’ भी कहा जाता है यानी मान (घर) में रहनेवाला जैसे कि मान (घर) में रहनेवाले को खड़ी बोली में ‘मानव’ कहा जाता है। ‘मान’ का क्रियामूल ‘मा’ है जिसका अर्थ होता है—निर्माण करना। यह क्रियामूल मठ, मण्डप, मन्दिर, माँद, मान, मनान, माड़ो—सभी में मौजूद है। ‘मानुष’ तत्सम है, ‘मनुष्य’ तद्भव है। संस्कृत में बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो लोकबोलियों के आधार पर गढ़े गए हैं परन्तु ग़लती से उसे तत्सम मान लिया जाता है। कारण कि हमारी भाषावैज्ञानिक स्थापना रही है कि संस्कृत पुरानी भाषा है, इसलिए लोकबोलियों के शब्द तद्भव हैं जबकि संस्कृत का पहला लम्बा अभिलेख 150 ई. में पश्चिमी भारत के जूनागढ़ से मिलता है। प्राकृत के अभिलेख भारत में सबसे पुराने हैं। वैदिक भाषा पुरानी है, वैदिक संस्कृति भी पुरानी है तब इस तथ्य की भी पड़ताल की जानी चाहिए कि वैदिक युग के तथाकथित सोने के सिक्के ‘निष्क’ कहाँ गए जबकि धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मिलते हैं। भाषा का समाजशास्त्र इस बात का जवाब देगा कि मागधी प्राकृत के साथ संस्कृत के आचार्यों ने दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों किया है।
Bharat Ki Bhasha Samasya
- Author Name:
Ramvilas Sharma
- Book Type:

- Description: भारत की भाषा-समस्या एक ज्वलन्त राष्ट्रीय समस्या है। सुप्रसिद्धप्रगतिशील आलोचक और विचारक डॉ. रामविलास शर्मा के अनुसार यह ‘विशुद्ध भाषा-विज्ञान कीसमस्या’ नहीं बल्कि ‘बहुजातीय राष्ट्र के गठन और विकास की ऐतिहासिक-राजनीतिक समस्या’ है। स्वाधीनता के तीन दशक बाद भी अगर यह समस्या ज्यों-की-त्यों बनी है तो सम्भवतः इसलिए कि उनकी तरह औरों ने भी इस समस्या को इसके वास्तविक और व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने का प्रयास नहीं किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में रामविलास जी ने भाषा-समस्या के विभिन्न पक्षों की विस्तार से चर्चा की है तथा इस बात पर बल दिया है कि सबसे पहले अंग्रेज़ी के प्रभुत्व को समाप्त करना आवश्यक है, क्योंकि वह भारत की सभी भाषाओं पर साम्राज्यवादियों द्वारा लादी हुई भाषा है। भारत की भाषा-समस्या के हल के लिए वह ‘अनिवार्य राष्ट्र-भाषा’ नहीं, बल्कि सम्पर्क भाषा की बात करते हैं जो हिन्दी ही हो सकती है। हिन्दी के जातीय स्वरूप की चर्चा के सन्दर्भ में वह यह स्पष्ट करते हैं कि हिन्दी और उर्दू में ‘बुनियादी एकता’ तथा हिन्दी की जनपदीय बोलियाँ परस्पर-सम्बद्ध हैं। भाषा-समस्या पर भारतीय जनता का सामाजिक और सांस्कृतिक भविष्य निर्भर करता है, इसलिए वह इसे आवश्यक मानते हैं कि ‘हम अपने बहुजातीय राष्ट्र की विशेषताएँ पहचानें, इस राष्ट्र में हिन्दी-भाषी जाति की भूमिका पहचानें।’इस पुस्तक में दिए गए उनके अकाट्य तर्क समस्या को समझने की सही दृष्टि ही नहीं देते, समस्या-समाधान की दिशा में मन को आन्दोलित भी करते हैं।
Garo Literature
- Author Name:
Caroline Marak
- Rating:
- Book Type:

- Description: Indian Literature in Tribal Languages documented and translated into english By Caroline Marak
Mere Samay Ke Shabda
- Author Name:
Kedarnath Singh
- Book Type:

-
Description:
केदारनाथ सिंह हमारे समय के सुप्रतिष्ठित कवि हैं। उन्होंने समय-समय पर विभिन्न साहित्यिक विषयों पर विश्लेषणपूर्ण लेख लिखे हैं। कई बार तर्कपूर्ण विचारप्रवण टिप्पणियाँ की हैं। एक शीर्षस्थ कवि का यह गद्य-लेखन संवेदना व संरचना की दृष्टि से अनूठा है। ‘मेरे समय के शब्द’ में केदारनाथ सिंह की रचनाशीलता का यह सुखद आयाम उद्घाटित हुआ है।
प्रस्तुत पुस्तक में कविता की केन्द्रीय उपस्थिति है। हिन्दी आधुनिकता का अर्थ तलाशते हुए सुमित्रानन्दन पंत ज्ञेय, नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा और श्रीकान्त वर्मा आदि के कविता-जगत की थाह लगाई गई है। इस सन्दर्भ में ‘आचार्य शुक्ल की काव्य-दृष्टि और आधुनिक कविता’ लेख अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
इसके अनन्तर पाँच खंड हैं—‘पाश्चात्य आधुनिकता के कुछ रंग’, ‘कुछ टिप्पणियाँ’, ‘व्यक्ति-प्रसंग’, ‘स्मृतियाँ’ और ‘परिशिष्ट’। पहले खंड में एजरा पाउंड, रिल्के और रेने शा की कविता पर विचार करने के साथ समकालीन अंग्रेज़ी कविता का मर्मान्वेषण किया गया है। दूसरे खंड में विभिन्न विषयों पर की गई टिप्पणियाँ लघु लेख सरीखी हैं।
‘व्यक्ति-प्रसंग’ के दो लेख त्रिलोचन और नामवर सिंह का आत्मीय आकलन हैं। अज्ञेय, श्रीकान्त वर्मा
और सोमदत्त की ‘स्मृतियाँ’ समानधर्मिता की ऊष्मा से भरी हैं। ‘परिशिष्ट’ में तीन साक्षात्कार हैं। एक उत्तर में केदारनाथ सिंह कहते हैं, ‘...नई पीढ़ी को एक नई मुक्ति के एहसास के साथ लिखना चाहिए और अपने रचनाकर्म में सबसे अधिक भरोसा करना चाहिए अपनी संवेदना और अपने विवेक पर।’
यह पुस्तक शब्द की समकालीन सक्रियता में निहित संवेदना और विवेक को भलीभाँति प्रकाशित करती है।
A History of Kashmiri Literature
- Author Name:
Trilokinath Raina
- Rating:
- Book Type:

- Description: Kashmiri literature, with poetry as its chief mode of expression, is said to have started with Lal Ded and Sheikh-ul-Alam. Over the last sixty years, it has expanded into various genres such as essays, criticism, history, drama, and fiction. Kashmiri literature now holds a significant place in Indian Letters. This book chronicles the history of Kashmiri literature from its beginnings to the present.
Hindi Sahitya Ka Itihas Punarlekhan Ki Avashyakta
- Author Name:
Pukhraj Maroo
- Book Type:

-
Description:
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य-लेखन की रामकथा के वाल्मीकि हैं, कोई भी साहित्येतिहासकार उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। यह कहना अनुचित न होगा कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की जैसी रंगारंग और जीवित पारदर्शियाँ हमें उनके इतिहास में मिलती हैं, वैसी आधुनिक साहित्य के बारे में नहीं मिलती हैं। इस दृष्टि से हिन्दी साहित्येतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता महसूस की जाती है।
इसके अलावा शुक्ल जी के बाद कई दशकों में फैला तकनीक क्रान्ति, और संचार तथा सूचनाओं का विस्फोटक दौर हमारे सामने है। इन वर्षों का हिन्दी साहित्य भाषा की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त विविध और सम्पन्न साहित्य है। सभ्यता, संस्कृति और विश्व-साहित्य के संगम-काल के इस साहित्य का विवेचन और दस्तावेज़ीकरण भी अब एक बड़ी आवश्यकता है।
यह पुस्तक ऐसे ही अन्य घटकों पर भी नज़र डालती है जो साहित्येतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। साथ ही इसमें इतिहास-लेखन के अब तक के इतिहास के हर चरण को विस्तार से विवेचित किया गया है जो अध्येताओं और विद्यार्थियों के लिए विशेष पठनीय है। आचार्य शुक्ल लिखित इतिहास के बाद हिन्दी में साहित्येतिहास-लेखन के जो अन्य प्रयास हुए उनका विशद विश्लेषण और तथ्यगत जानकारी भी दी गई है। आधुनिक हिन्दी साहित्य की विविध विधाओं, और इतिहास-लेखन की दृष्टि से उनका मूल्यांकन भी लेखक ने किया है।
Sarjan Aur Rasasvadan : Bhartiya Paksh
- Author Name:
Yogendra Pratap Singh
- Book Type:

-
Description:
हिन्दी साहित्य में आधुनिक काल के अन्तर्गत सन् 1942 तक एक ओर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने ‘रस मीमांसा लिखकर समसामयिकता के सन्दर्भ में इसके प्रासंगिक कपाटों को खोलने की चेष्टा की है तो दूसरी ओर नई कविता के आन्दोलन ने रस चिन्तन को रूढ़, प्राचीन, अप्रासंगिक, ऐतिहासिक, मृत आदि घोषित करने की चेष्टा की है और अज्ञेय, लक्ष्मीकान्त वर्मा, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी आदि ने इसे उसकी मूल सत्ता से च्युत किया। आधुनिक हिन्दी साहित्य में रस चिन्तन का यह द्वन्द्व, निश्चित ही एक जटिल बनकर हमारे सामने आता है।
मानव जाति के कलात्मक स्वभाव की यह रागात्मक चेतना भारतीय चिन्तन में रस के रूप में व्याख्यायित हुई है और आज उसे आकस्मिक रूप से नई कविता के कवियों तथा समीक्षकों द्वारा मृत घोषित कर दिया जाना, उनकी तथाकथित आधुनिकता के मोह का प्रतिफल है, जो सर्वथा असंगत है।
यही नहीं, आधुनिक युग के सृजनात्मक विस्तार के बीच रस चिन्तन की व्याप्ति की सम्भावनाओं का पुनर्विश्लेषण आवश्यक है। सृजन का सम्बन्ध केवल साहित्य से ही नहीं है, चित्र, वाद्य, नृत्य, संगीत, स्थापत्य आदि कलाएँ आज जो विस्तार प्राप्त कर रही हैं, उनकी सृजनात्मक अभिव्यक्तियाँ आस्वादन की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। सम्पूर्ण कलाओं के आस्वादन फल का ही नाम रस है। मानव मन की रागात्मक चेतना एवं अनुभूति जगत् के विस्तार से रस व्याप्ति की सम्भावनाओं का भी विस्तार हो रहा है और ऐसी स्थिति में, आज उसके बार-बार विश्लेषण की आवश्यकता है, नकारने या पलायन की नहीं।
इस प्रकार, इस कृति का मूल मन्तव्य है, आज की निषेधवादी विचारधाराओं का खंडन करते हुए इसकी सामयिक प्रासंगिकता का विश्लेषण।
Acharya Mahaveerprasad Dwivedi Ke Shreshth Nibandh
- Author Name:
Acharya Mahaveerprasad Dwivedi
- Book Type:

-
Description:
आज हम जो कुछ भी हैं, उन्हीं के बनाए हुए है। यदि पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी न होते तो बेचारी हिन्दी कोसों पीछे होती, समुन्नति की इस सीमा तक आने का अवसर ही नहीं मिलता। उन्होंने हमारे लिए पथ भी बनाया और पथ-प्रदर्शक का भी काम किया। हमारे लिए उन्होंने वह तपस्या की है जो हिन्दी-साहित्य की दुनिया में बेजोड़ ही कही जाएगी। किसी ने हमारे लिए इतना नहीं किया, जितना उन्होंने। वे हिन्दी के सरल सुन्दर रूप के उन्नायक बने, हिन्दी-साहित्य में विश्व-साहित्य के उत्तमोत्तम उपकरणों का उन्होंने समावेश किया; दर्जनों कवि, लेखक और सम्पादक बनाए। जिसमें कुछ प्रतिभा देखी उसी को अपना लिया और उसके द्वारा मातृभाषा की सेवा कराई। हिन्दी के लिए उन्होंने अपना तन, मन, धन सब कुछ अर्पित कर दिया। हमारी उपस्थित उपलब्धि उन्हीं के त्याग का परिणाम है।
—प्रेमचन्द
अंग्रेज़ी भाषा में जो स्थान डॉ. जॉनसन का है वर्तमान में वही स्थान द्विवेदी जी का है। जिस प्रकार अंग्रेज़ी भाषा का वर्तमान स्वरूप बहुत दूर तक डॉ. जॉनसन का दिया हुआ है, उसी प्रकार हिन्दी का वर्तमान स्वरूप द्विवेदी जी का।
—सेठ गोविन्द दास
द्विवेदी जी ने समाजशास्त्र और इतिहास के बारे में जो कुछ लिखा है, उससे समाज-विज्ञान और इतिहास लेखन के विज्ञान की नवीन रूप-रेखाएँ निश्चित होती हैं। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का नवीन मूल्यांकन किया। एक ओर उन्होंने इस देश के प्राचीन दर्शन, विज्ञान, साहित्य तथा संस्कृति के अन्य अंगों पर हमें गर्व करना सिखाया, एशिया के सांस्कृतिक मानचित्र में भारत के गौरवपूर्ण स्थान पर ध्यान केन्द्रित किया, दूसरी ओर उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक रूढ़ियों का तीव्र खंडन किया और उस विवेक परम्परा का उल्लेख सहानुभूतिपूर्वक किया जिसका सम्बन्ध चार्वाक और बृहस्पति से जोड़ा जाता है। अध्यात्मवादी मान्यताओं, धर्मशास्त्र की स्थापनाओं को उन्होंने नई विवेक दृष्टि से परखना सिखाया।
—रामविलास शर्मा
उल्लेखनीय है कि महावीरप्रसाद द्विवेदी की 'सरस्वती' ज्ञान की पत्रिका कही गई है और उनका गद्य हिन्दी साहित्य का ज्ञानकांड। इस प्रकार, भारत का उन्नीसवीं शताब्दी का नवजागरण यूरोप के 'एनलाइटेनमेंट' अथवा 'ज्ञानोदय' की चेतना के अधिक निटक प्रतीत होता है और पन्द्रहवीं शताब्दी का नवजागरण 'रेनेसां' के तुल्य।
—नामवर सिंह
Celebrating The City Kolkata in Indian Literature
- Author Name:
Sayantan Dasgupta
- Book Type:

- Description: This anthology has its roots in a Sahitya Akademi symposium in which the Centre for Translation of Indian Literatue, Jadhapur University collaborated under the aegis of its UGC RUSA 2.0 project on Redefining Indian Literature.
Antastal Ka Poora Viplav : Andhere Mein
- Author Name:
Nirmala Jain
- Book Type:

-
Description:
‘अँधेरे में’ उत्तरशती की सबसे महत्त्वपूर्ण और शायद सबसे विवादास्पद कविता है। विवाद भिन्न रुचि और विचारधारा वालों के बीच ही नहीं, समानधर्मा आलोचकों के बीच भी है। यह तथ्य कविता की सम्भावनाशीलता का प्रमाण है। यह भी सही है कि मुक्तिबोध के जीवन-काल में इस कविता को ख़ुद उनसे सुना तो कइयों ने होगा, लेकिन इसे सराहा उनकी मृत्यु के बाद ही गया। इस विलम्ब का कारण उपेक्षा या उदासीनता नहीं, बल्कि ऐतिहासिकता है।
अपने समय का अतिक्रमण हर कालजयी रचना में होता है। लेकिन आनेवाले समय के इस कदर साथ चलनेवाली रचनाओं की संख्या बहुत नहीं होती। इस दृष्टि से देखने पर यह बात हैरत में डालनेवाली है कि अपने सारे जटिल अर्थ-विन्यास और अपारदर्शी शिल्प के बावजूद इस कविता के पाठकों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई है।
कविता के पाठक-आलोचकों ने तरह-तरह से इस बात को दोहराया है कि मध्यवर्ग के सुविधाजीवी, समझौतावादी और आदर्शजीवी मन का संघर्ष ही ‘अँधेरे में’ की काव्य-वस्तु है।
इस पुस्तक में ख्यात हिन्दी आलोचक निर्मला जैन ने ‘अँधेरे में’ पर आधारित आलोचनात्मक आलेखों को संकलित किया है। ये आलेख इस कालजयी कविता की विभिन्न पक्षों से व्याख्या करते हैं।
Hindi Bhasha : Vikas Aur Swaroop
- Author Name:
Dr. Kailash Chandra Bhatia
- Book Type:

- Description: हिंदी के ऐतिहासिक संदर्भ में जहाँ अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी महत्त्व है वहीं उसके स्वरूप-निर्धारण में उसकी उपभाषाओं-बोलियों का, विशेष रूप से ब्रजभाषा और अवधी का, अप्रतिम महत्त्व है। हिंदी की प्रमुख बोलियों और उनके पारस्परिक संबंध पर भी विवेचन प्रस्तुत किया गया है। हिंदी भाषा के मानकीकरण की समस्या भी है। प्रयोग क्षेत्र में हिंदी की कोई समानता नहीं है, जिसको हिंदी क्रियाओं के विविध प्रयोगों को लेकर प्रस्तुत किया गया है। इससे दो प्रयोगों में सूक्ष्म अंतर स्पष्ट हो सकेगा। शुद्ध हिंदी लिखने के लिए हिंदी व्याकरण के प्रमुख नियमों का ज्ञान भी आवश्यक है। अपनी अभिव्यक्ति का रंग-रूप निखारने के लिए व्याकरणसम्मत भाषा का प्रयोग अच्छा रहता है। पुस्तक की विषय-वस्तु बहुत सरल तथा सहज भाषा में प्रस्तुत की गई है, जिससे हिंदी भाषा के जिज्ञासु उससे अधिकाधिक लाभान्वित हो सकें।
Latin America, Caribbeyayi Kshetra Aur Bharat
- Author Name:
Deepak Bhojwani
- Book Type:

- Description: लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र के बारे में आम तौर पर भारत में कम जानकारी है। इस क्षेत्र में भारतीयों का अपेक्षाकृत प्रवास और संपर्क कम ही रहा है। यह पुस्तक इस क्षेत्र और यहाँ के देशों की विशिष्टताओं से पाठकों को परिचित कराती है। प्रारंभिक अध्यायों में इस क्षेत्र के राजनीतिक विकास-क्रम तथा आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों की जानकारी दी गई है। बाद के अध्यायों में भारत के साथ इन देशों के राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों का विवेचन किया गया है। तैंतीस देशों वाले इस क्षेत्र के देशों से मैत्री में भारत के लिए अनेक संभावनाएँ निहित हैं । ये देश विविध संसाधनों से समृद्ध हैं; इन देशों ने आकर्षक विकास-दर हासिल की है और इनकी सामाजिक नीतियों ने स्थिर सरकारों को आधार दिया है। इस पुस्तक से पाठकों को अनेक महत्त्वपूर्ण अंतर्निहित पक्षों की भी जानकारी मिलती है। लेखक ने इस क्षेत्र के देशों से संबंधों की चुनौतियों और संभावनाओं का आकलन करते हुए, अधिक प्रभावी तथा सार्थक संबंधों की दिशा दिखाई है।
Hindi Sahitya Ka Samikshatmak Itihas
- Author Name:
Vijaypal Singh
- Book Type:

-
Description:
हिन्दी साहित्य में रीति काव्य, ख़ासतौर से केशव पर डॉ. विजयपाल सिंह की पुस्तकें अत्यन्त लोकप्रिय रही हैं। इस पुस्तक में उन्होंने असाधारण प्रवाह के साथ हिन्दी साहित्य के विभिन्न चरणों और प्रवृत्तियों का समीक्षात्मक अध्ययन किया है।
अभी तक उपलब्ध विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखे गए इतिहासों को ध्यान में रखते हुए तथा नए तथ्यों को समाहित करते हुए इस पुस्तक में उन्होंने प्रयास किया है कि आरम्भिक काल से लेकर आधुनिक साहित्य तक का विस्तारपूर्वक विवेचन प्रस्तुत किया जा सके।
लेखक ने इस कृति को ग्यारह खंडों में विभाजित किया है। खंडों का विभाजन साहित्येतिहास के आलोचकों, समीक्षकों तथा साहित्येतिहासकारों, अनुसन्धानों तथा टिप्पणियों के विश्लेषण और पुनर्मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।
लेखक ने डॉ. ग्रियर्सन, हजारीप्रसाद द्विवेदी, मिश्र-बन्धुओं, रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, इडविन ग्रिब्ज जैसे विद्वानों द्वारा किए काल खंडों का भी पुनर्मूल्यांकन और विश्लेषण किया है।
पुस्तक के लेखन में विद्वान आलोचक ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि विद्वज्जनों के साथ-साथ यह पुस्तक छात्रों, शोधार्थियों और सामान्य पाठकों के लिए भी सहज ग्राह्य हो।
Customer Reviews
Be the first to write a review...
0 out of 5
Book